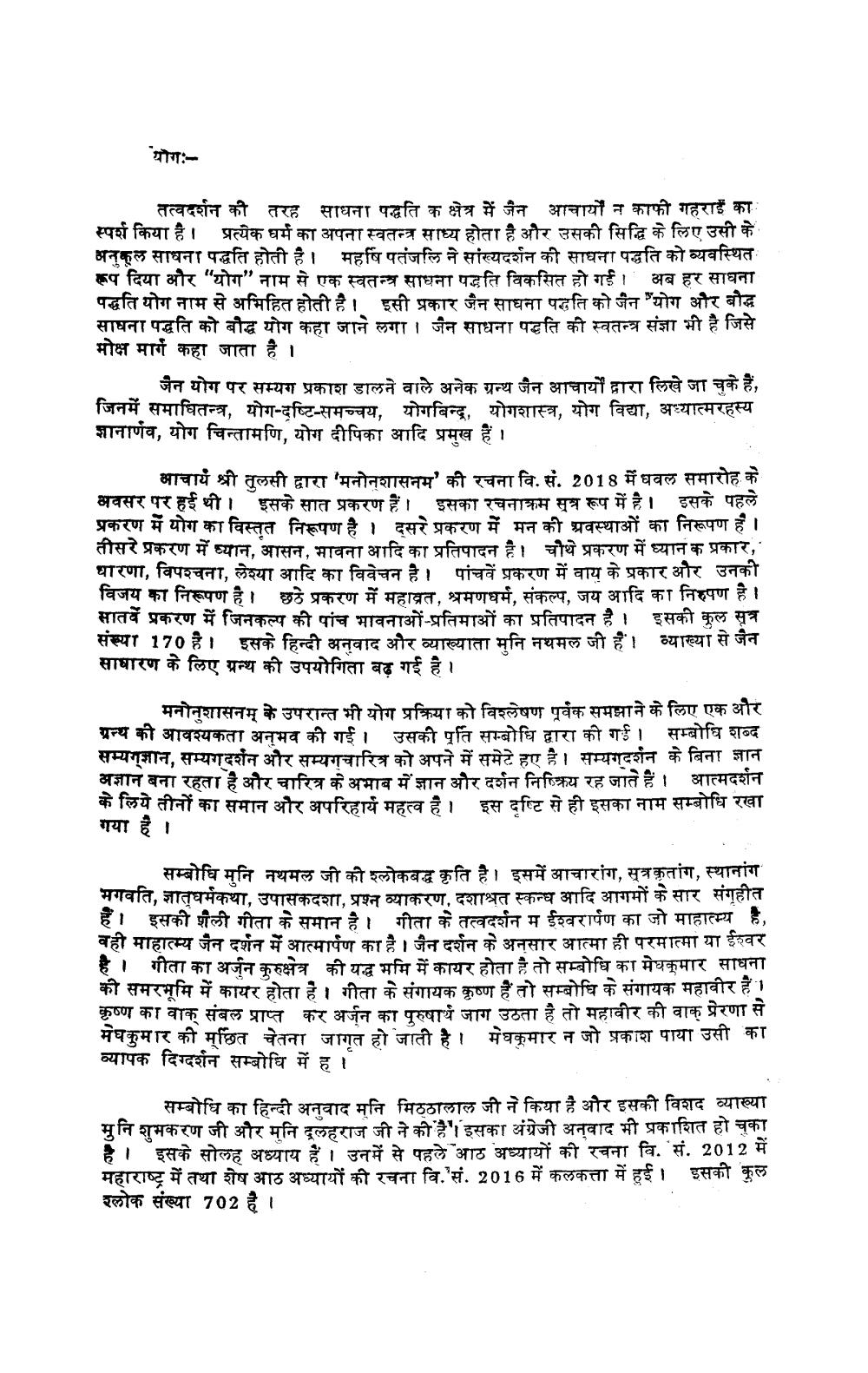________________
योग:
तत्वदर्शन की तरह साधना पद्धति क क्षेत्र में जैन आचार्यों न काफी गहराई का स्पर्श किया है। प्रत्येक धर्म का अपना स्वतन्त्र साध्य होता है और उसकी सिद्धि के लिए उसी के अनकल साधना पद्धति होती है। महर्षि पतंजलि ने सांख्यदर्शन की साधना पद्धति को व्यवस्थित रूप दिया और “योग" नाम से एक स्वतन्त्र साधना पद्धति विकसित हो गई। अब हर साधना पद्धति योग नाम से अभिहित होती है। इसी प्रकार जैन साधना पद्धति को जैन "योग और बौद्ध साधना पद्धति को बौद्ध योग कहा जाने लगा। जैन साधना पद्धति की स्वतन्त्र संज्ञा भी है जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है ।
जैन योग पर सम्यग प्रकाश डालने वाले अनेक ग्रन्थ जैन आचार्यों द्वारा लिखे जा चुके हैं, जिनमें समाधितन्त्र, योग-दष्टि-समच्चय, योगबिन्द्र, योगशास्त्र, योग विद्या, अध्यात्मरहस्य ज्ञानार्णव, योग चिन्तामणि. योग दीपिका आदि प्रमख हैं।
आचार्य श्री तुलसी द्वारा 'मनोनशासनम' की रचना वि.सं. 2018 में धवल समारोह के अवसर पर हई थी। इसके सात प्रकरण हैं। इसका रचनाक्रम सुत्र रूप में है। इसके पहले प्रकरण में योग का विस्तृत निरूपण है। दसरे प्रकरण में मन की अवस्थाओं का निरूपण है। तीसरे प्रकरण में ध्यान, आसन, भावना आदि का प्रतिपादन है। चौथे प्रकरण में ध्यान क प्रकार, धारणा, विपश्चना, लेश्या आदि का विवेचन है। पांचवें प्रकरण में वाय के प्रकार और उनकी विजय का निरूपण है। छठे प्रकरण में महाव्रत, श्रमणधर्म, संकल्प, जय आदि का निरूपण है। सातवें प्रकरण में जिनकल्प की पांच भावनाओं-प्रतिमाओं का प्रतिपादन है। इसकी कुल सूत्र संख्या 170 है। इसके हिन्दी अनुवाद और व्याख्याता मुनि नथमल जी हैं। व्याख्या से जैन साधारण के लिए ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है।
मनोनुशासनम के उपरान्त भी योग प्रक्रिया को विश्लेषण पूर्वक समझाने के लिए एक और ग्रन्थ की आवश्यकता अनमव की गई। उसकी पति सम्बोधि द्वारा की गई। सम्बोधि शब्द सम्यग्ज्ञान, सम्यगदर्शन और सम्यगचारित्र को अपने में समेटे हए है। सम्यगदर्शन के बिना ज्ञान अज्ञान बना रहता है और चारित्र के अभाव में ज्ञान और दर्शन निष्क्रिय रह जाते हैं। आत्मदर्शन कालय तीनों का समान और अपरिहार्य महत्व है। इस दष्टि से ही इसका नाम सम्बोधि रखा गया है।
सम्बोधि मुनि नथमल जी को श्लोकबद्ध कृति है। इसमें आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग भगवति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकदशा. प्रश्न व्याकरण. दशाश्रत स्कन्ध आदि आगमों के सार संग्रहीत है। इसकी शैली गीता के समान है। गीता के तत्वदर्शन म ईश्वरार्पण का जो माहात्म्य है, वही माहात्म्य जैन दर्शन में आत्मार्पण का है। जैन दर्शन के अनसार आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर है। गीता का अर्जुन कुरुक्षेत्र की यद्ध ममि में कायर होता है तो सम्बोधि का मेषकुमार साधना का समरभूमि में कायर होता है। गीता के संगायक कृष्ण हैं तो सम्बोधि के संगायक महावीर हैं। कृष्ण का वाक संबल प्राप्त कर अर्जन का पुरुषार्थ जाग उठता है तो महावीर की वाक् प्रेरणा से मघकुमार की मछित चेतना जागत हो जाती है। मेघकूमार न जो प्रकाश पाया उसी का व्यापक दिग्दर्शन सम्बोधि में ह।
सम्बोधि का हिन्दी अनुवाद मनि मिठठालाल जी ने किया है और इसकी विशद व्याख्या मुनि शुभकरण जी और मनि दूलहराज जी ने की है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। इसके सोलह अध्याय हैं। उनमें से पहले आठ अध्यायों की रचना वि.सं. 2012 में महाराष्ट्र में तथा शेष आठ अध्यायों की रचना वि.सं. 2016 में कलकत्ता में हई। इसकी कूल श्लोक संख्या 702 है ।