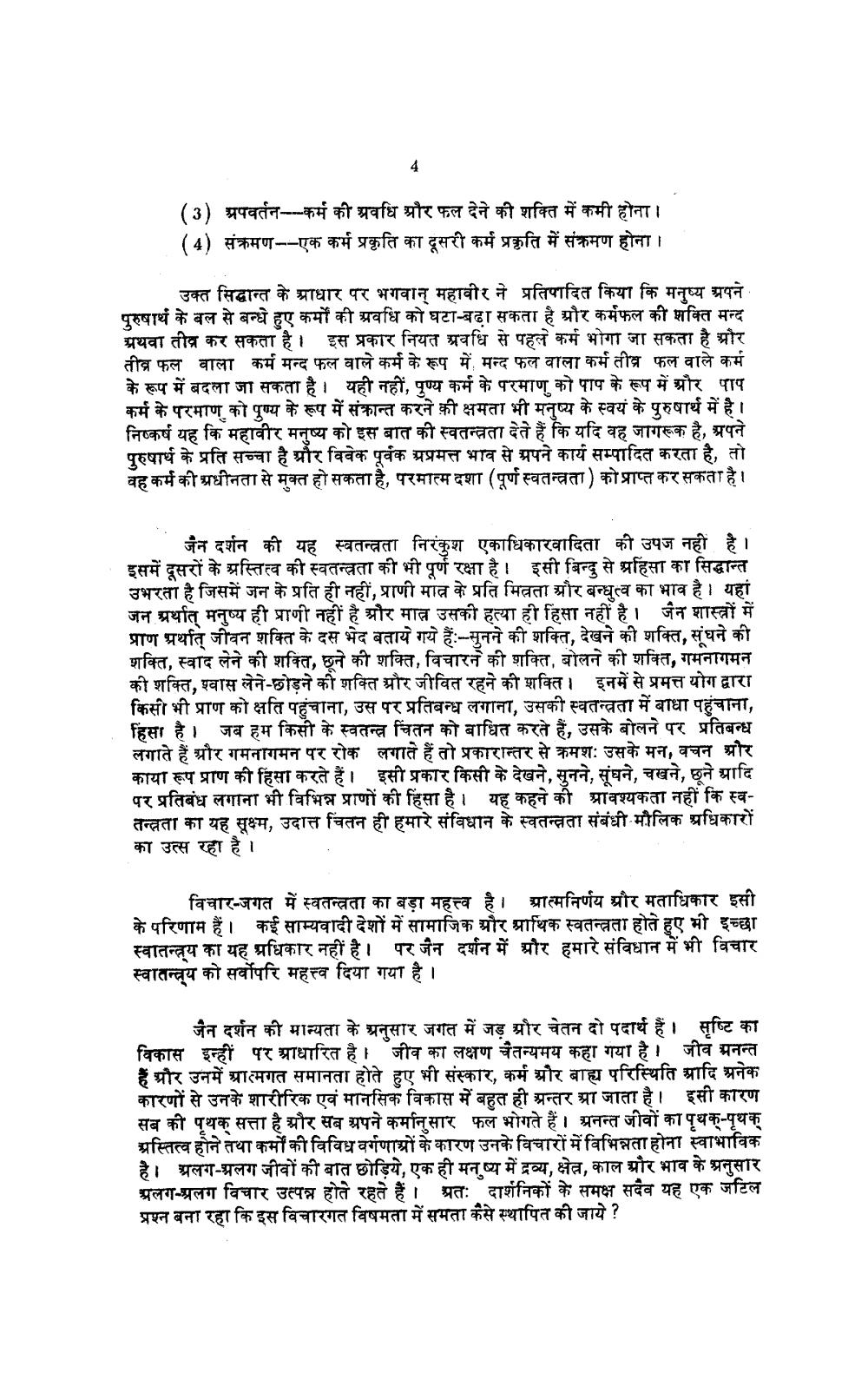________________
(3) अपवर्तन--कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में कमी होना। (4) संक्रमण--एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में संक्रमण होना।
उक्त सिद्धान्त के आधार पर भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल से बन्धे हए कर्मों की अवधि को घटा-बढ़ा सकता है और कर्मफल की शक्ति मन्द अथवा तीव्र कर सकता है। इस प्रकार नियत अवधि से पहले कर्म भोगा जा सकता है और तीव्र फल वाला कर्म मन्द फल वाले कर्म के रूप में मन्द फल वाला कर्म तीव्र फल वाले कर्म के रूप में बदला जा सकता है। यही नहीं, पुण्य कर्म के परमाणु को पाप के रूप में और पाप कर्म के परमाण को पुण्य के रूप में संक्रान्त करने की क्षमता भी मनुष्य के स्वयं के पुरुषार्थ में है। निष्कर्ष यह कि महावीर मनुष्य को इस बात की स्वतन्त्रता देते हैं कि यदि वह जागरूक है, अपने पुरुषार्थ के प्रति सच्चा है और विवेक पूर्वक अप्रमत्त भाव से अपने कार्य सम्पादित करता है, तो वह कर्म की अधीनता से मुक्त हो सकता है, परमात्म दशा (पूर्ण स्वतन्त्रता) कोप्राप्त कर सकता है।
जैन दर्शन की यह स्वतन्त्रता निरंकुश एकाधिकारवादिता की उपज नहीं है। इसमें दूसरों के अस्तित्व की स्वतन्त्रता की भी पूर्ण रक्षा है। इसी बिन्दु से अहिंसा का सिद्धान्त उभरता है जिसमें जन के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता और बन्धुत्व का भाव है। यहां जन पर ष्य ही प्राणी नहीं है और मात्र उसकी हत्या ही हिंसा नहीं है। जैन शास्त्रों में प्राण प्रर्थात् जीवन शक्ति के दस भेद बताये गये हैं:-सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, छूने की शक्ति, विचारने की शक्ति, बोलने की शक्ति, गमनागमन की शक्ति, श्वास लेने-छोड़ने की शक्ति और जीवित रहने की शक्ति। इनमें से प्रमत्त योग द्वारा किसी भी प्राण को क्षति पहुंचाना, उस पर प्रतिबन्ध लगाना, उसकी स्वतन्त्रता में बाधा पहुंचाना, हिंसा है। जब हम किसी के स्वतन्त्र चिंतन को बाधित करते हैं, उसके बोलने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं और गमनागमन पर रोक लगाते हैं तो प्रकारान्तर से क्रमशः उसके मन, वचन और काया रूप प्राण की हिंसा करते हैं। इसी प्रकार किसी के देखने, सुनने, सुंघने, चखने, छूने आदि पर प्रतिबंध लगाना भी विभिन्न प्राणों की हिंसा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतन्त्रता का यह सूक्ष्म, उदात्त चितन ही हमारे संविधान के स्वतन्त्रता संबंधी मौलिक अधिकारों का उत्स रहा है।
विचार-जगत में स्वतन्त्रता का बड़ा महत्त्व है। प्रात्मनिर्णय और मताधिकार इसी के परिणाम हैं। कई साम्यवादी देशों में सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता होते हुए भी इच्छा स्वातन्त्रय का यह अधिकार नहीं है। पर जैन दर्शन में और हमारे संविधान में भी विचार स्वातन्त्र्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है ।
जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जगत में जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। सृष्टि का विकास इन्हीं पर आधारित है। जीव का लक्षण चैतन्यमय कहा गया है। जीव अनन्त हैं और उनमें प्रात्मगत समानता होते हए भी संस्कार, कर्म और बाह्य परिस्थिति आदि अनेक कारणों से उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बहत ही अन्तर आ जाता है। इसी कारण सब की पृथक सत्ता है और सब अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। अनन्त जीवों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व होने
प्रा के कारण उनके विचारों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। अलग-अलग जीवों की बात छोड़िये, एक ही मनुष्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार अलग-अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अतः दार्शनिकों के समक्ष सदैव यह एक जटिल प्रश्न बना रहा कि इस विचारगत विषमता में समता कैसे स्थापित की जाये ?