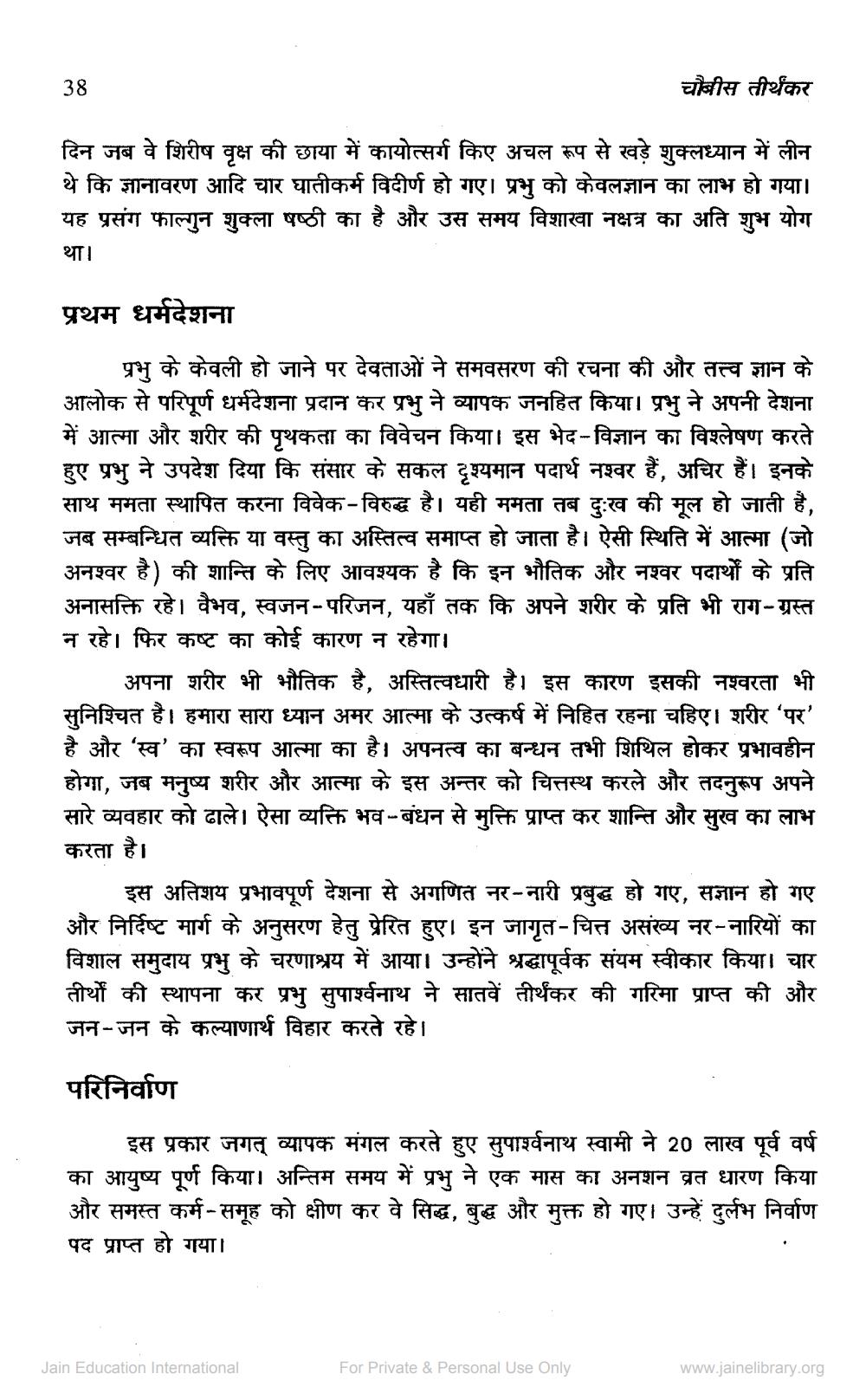________________
38
चौबीस तीर्थंकर
दिन जब वे शिरीष वृक्ष की छाया में कायोत्सर्ग किए अचल रूप से खड़े शुक्लध्यान में लीन थे कि ज्ञानावरण आदि चार घातीकर्म विदीर्ण हो गए। प्रभु को केवलज्ञान का लाभ हो गया। यह प्रसंग फाल्गुन शुक्ला षष्ठी का है और उस समय विशाखा नक्षत्र का अति शुभ योग था।
प्रथम धर्मदेशना
__ प्रभु के केवली हो जाने पर देवताओं ने समवसरण की रचना की और तत्त्व ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण धर्मदेशना प्रदान कर प्रभु ने व्यापक जनहित किया। प्रभु ने अपनी देशना में आत्मा और शरीर की पृथकता का विवेचन किया। इस भेद-विज्ञान का विश्लेषण करते हुए प्रभु ने उपदेश दिया कि संसार के सकल दृश्यमान पदार्थ नश्वर हैं, अचिर हैं। इनके साथ ममता स्थापित करना विवेक-विरुद्ध है। यही ममता तब दुःख की मूल हो जाती है, जब सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा (जो अनश्वर है) की शान्ति के लिए आवश्यक है कि इन भौतिक और नश्वर पदार्थों के प्रति अनासक्ति रहे। वैभव, स्वजन-परिजन, यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी राग-ग्रस्त न रहे। फिर कष्ट का कोई कारण न रहेगा।
अपना शरीर भी भौतिक है, अस्तित्वधारी है। इस कारण इसकी नश्वरता भी सुनिश्चित है। हमारा सारा ध्यान अमर आत्मा के उत्कर्ष में निहित रहना चहिए। शरीर 'पर' है और 'स्व' का स्वरूप आत्मा का है। अपनत्व का बन्धन तभी शिथिल होकर प्रभावहीन होगा, जब मनुष्य शरीर और आत्मा के इस अन्तर को चित्तस्थ करले और तदनुरूप अपने सारे व्यवहार को ढाले। ऐसा व्यक्ति भव-बंधन से मुक्ति प्राप्त कर शान्ति और सुख का लाभ करता है।
- इस अतिशय प्रभावपूर्ण देशना से अगणित नर-नारी प्रबुद्ध हो गए, सज्ञान हो गए और निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण हेतु प्रेरित हुए। इन जागृत-चित्त असंख्य नर-नारियों का विशाल समुदाय प्रभु के चरणाश्रय में आया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक संयम स्वीकार किया। चार तीर्थों की स्थापना कर प्रभु सुपार्श्वनाथ ने सातवें तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की और जन-जन के कल्याणार्थ विहार करते रहे।
परिनिर्वाण
इस प्रकार जगत् व्यापक मंगल करते हुए सुपार्श्वनाथ स्वामी ने 20 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया। अन्तिम समय में प्रभु ने एक मास का अनशन व्रत धारण किया और समस्त कर्म-समूह को क्षीण कर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। उन्हें दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त हो गया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org