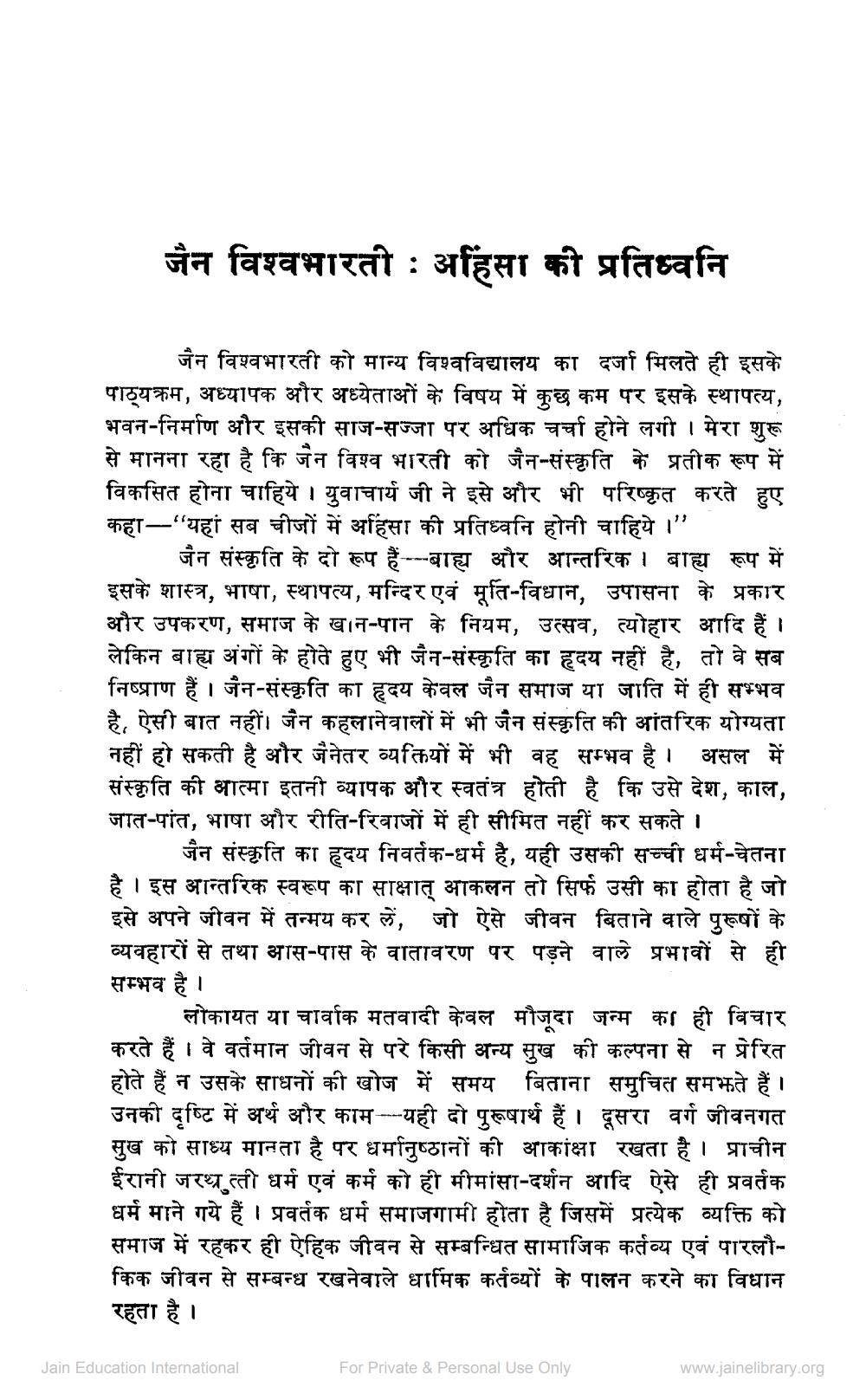________________
जैन विश्वभारती : अहिंसा की प्रतिध्वनि
जैन विश्वभारती को मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलते ही इसके पाठ्यक्रम, अध्यापक और अध्येताओं के विषय में कुछ कम पर इसके स्थापत्य, भवन-निर्माण और इसकी साज-सज्जा पर अधिक चर्चा होने लगी । मेरा शुरू से मानना रहा है कि जैन विश्व भारती को जैन-संस्कृति के प्रतीक रूप में विकसित होना चाहिये । युवाचार्य जी ने इसे और भी परिष्कृत करते हुए कहा- “यहां सब चीजों में अहिंसा की प्रतिध्वनि होनी चाहिये ।"
जैन संस्कृति के दो रूप हैं---बाह्य और आन्तरिक । बाह्य रूप में इसके शास्त्र, भाषा, स्थापत्य, मन्दिर एवं मूर्ति-विधान, उपासना के प्रकार
और उपकरण, समाज के खान-पान के नियम, उत्सव, त्योहार आदि हैं। लेकिन बाह्य अंगों के होते हुए भी जैन-संस्कृति का हृदय नहीं है, तो वे सब निष्प्राण हैं । जैन-संस्कृति का हृदय केवल जैन समाज या जाति में ही सभ्भव है, ऐसी बात नहीं। जैन कहलानेवालों में भी जैन संस्कृति की आंतरिक योग्यता नहीं हो सकती है और जैनेतर व्यक्तियों में भी वह सम्भव है। असल में संस्कृति की आत्मा इतनी व्यापक और स्वतंत्र होती है कि उसे देश, काल, जात-पांत, भाषा और रीति-रिवाजों में ही सीमित नहीं कर सकते ।
जैन संस्कृति का हृदय निवर्तक-धर्म है, यही उसकी सच्ची धर्म-चेतना है । इस आन्तरिक स्वरूप का साक्षात् आकलन तो सिर्फ उसी का होता है जो इसे अपने जीवन में तन्मय कर लें, जो ऐसे जीवन बिताने वाले पुरूषों के व्यवहारों से तथा आस-पास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से ही सम्भव है।
लोकायत या चार्वाक मतवादी केवल मौजूदा जन्म का ही विचार करते हैं । वे वर्तमान जीवन से परे किसी अन्य सुख की कल्पना से न प्रेरित होते हैं न उसके साधनों की खोज में समय बिताना समुचित समझते हैं। उनकी दृष्टि में अर्थ और काम-यही दो पुरूषार्थ हैं। दूसरा वर्ग जीवनगत सुख को साध्य मानता है पर धर्मानुष्ठानों की आकांक्षा रखता है। प्राचीन ईरानी जरथ त्ती धर्म एवं कर्म को ही मीमांसा-दर्शन आदि ऐसे ही प्रवर्तक धर्म माने गये हैं । प्रवर्तक धर्म समाजगामी होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर ही ऐहिक जीवन से सम्बन्धित सामाजिक कर्तव्य एवं पारलौकिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले धार्मिक कर्तव्यों के पालन करने का विधान रहता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org