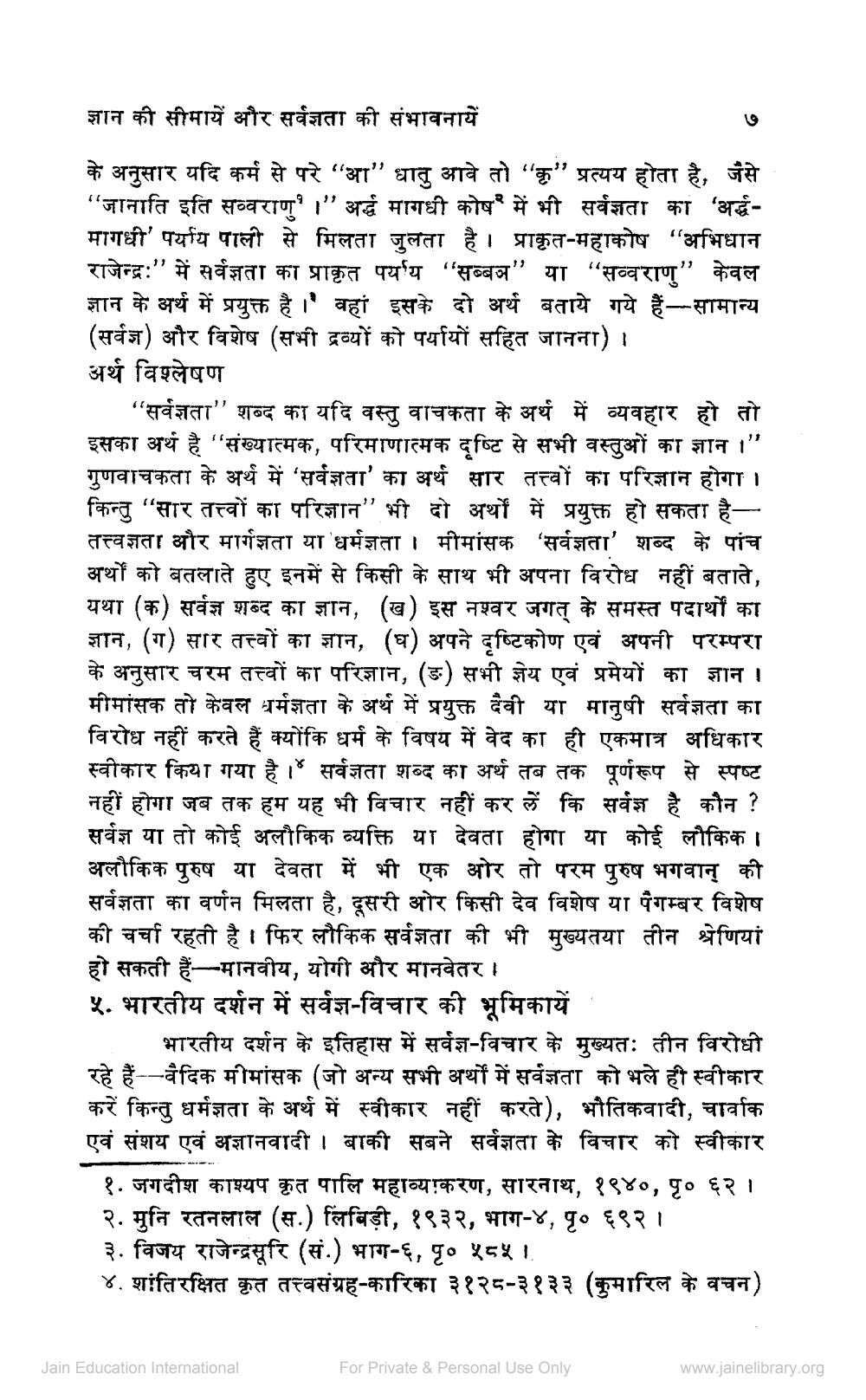________________
ज्ञान की सीमायें और सर्वज्ञता की संभावनायें
के अनुसार यदि कर्म से परे "आ" धातु आवे तो "कृ" प्रत्यय होता है, जैसे "जानाति इति सव्वराणु' ।" अर्द्ध मागधी कोषमें भी सर्वज्ञता का 'अर्द्धमागधी' पर्याय पाली से मिलता जुलता है। प्राकृत-महाकोष “अभिधान राजेन्द्रः" में सर्वज्ञता का प्राकृत पर्याय “सब्बञ" या "सव्वराणु" केवल ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है।' वहां इसके दो अर्थ बताये गये हैं-सामान्य (सर्वज्ञ) और विशेष (सभी द्रव्यों को पर्यायों सहित जानना)। अर्थ विश्लेषण
"सर्वज्ञता' शब्द का यदि वस्तु वाचकता के अर्थ में व्यवहार हो तो इसका अर्थ है "संख्यात्मक, परिमाणात्मक दृष्टि से सभी वस्तुओं का ज्ञान ।" गुणवाचकता के अर्थ में 'सर्वज्ञता' का अर्थ सार तत्त्वों का परिज्ञान होगा। किन्तु “सार तत्त्वों का परिज्ञान' भी दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता हैतत्त्वज्ञता और मार्गज्ञता या धर्मज्ञता। मीमांसक 'सर्वज्ञता' शब्द के पांच अर्थों को बतलाते हुए इनमें से किसी के साथ भी अपना विरोध नहीं बताते, यथा (क) सर्वज्ञ शब्द का ज्ञान, (ख) इस नश्वर जगत् के समस्त पदार्थों का ज्ञान, (ग) सार तत्त्वों का ज्ञान, (घ) अपने दृष्टिकोण एवं अपनी परम्परा के अनुसार चरम तत्त्वों का परिज्ञान, (ङ) सभी ज्ञेय एवं प्रमेयों का ज्ञान । मीमांसक तो केवल धर्मज्ञता के अर्थ में प्रयुक्त दैवी या मानुषी सर्वज्ञता का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि धर्म के विषय में वेद का ही एकमात्र अधिकार स्वीकार किया गया है। सर्वज्ञता शब्द का अर्थ तब तक पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होगा जब तक हम यह भी विचार नहीं कर लें कि सर्वज्ञ है कौन ? सर्वज्ञ या तो कोई अलौकिक व्यक्ति या देवता होगा या कोई लौकिक । अलौकिक पुरुष या देवता में भी एक ओर तो परम पुरुष भगवान की सर्वज्ञता का वर्णन मिलता है, दूसरी ओर किसी देव विशेष या पैगम्बर विशेष की चर्चा रहती है। फिर लौकिक सर्वज्ञता की भी मुख्यतया तीन श्रेणियां हो सकती हैं-मानवीय, योगी और मानवेतर । ५. भारतीय दर्शन में सर्वज्ञ-विचार की भूमिकायें
भारतीय दर्शन के इतिहास में सर्वज्ञ-विचार के मुख्यतः तीन विरोधी रहे हैं--वैदिक मीमांसक (जो अन्य सभी अर्थों में सर्वज्ञता को भले ही स्वीकार करें किन्तु धर्मज्ञता के अर्थ में स्वीकार नहीं करते), भौतिकवादी, चार्वाक एवं संशय एवं अज्ञानवादी। बाकी सबने सर्वज्ञता के विचार को स्वीकार १. जगदीश काश्यप कृत पालि महाव्याकरण, सारनाथ, १९४०, पृ० ६२ । २. मुनि रतनलाल (स.) लिविड़ी, १९३२, भाग-४, पृ० ६९२ ।। ३. विजय राजेन्द्रसूरि (सं.) भाग-६, पृ० ५८५। ४. शांतिरक्षित कृत तत्त्वसंग्रह-कारिका ३१२८-३१३३ (कुमारिल के वचन)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org