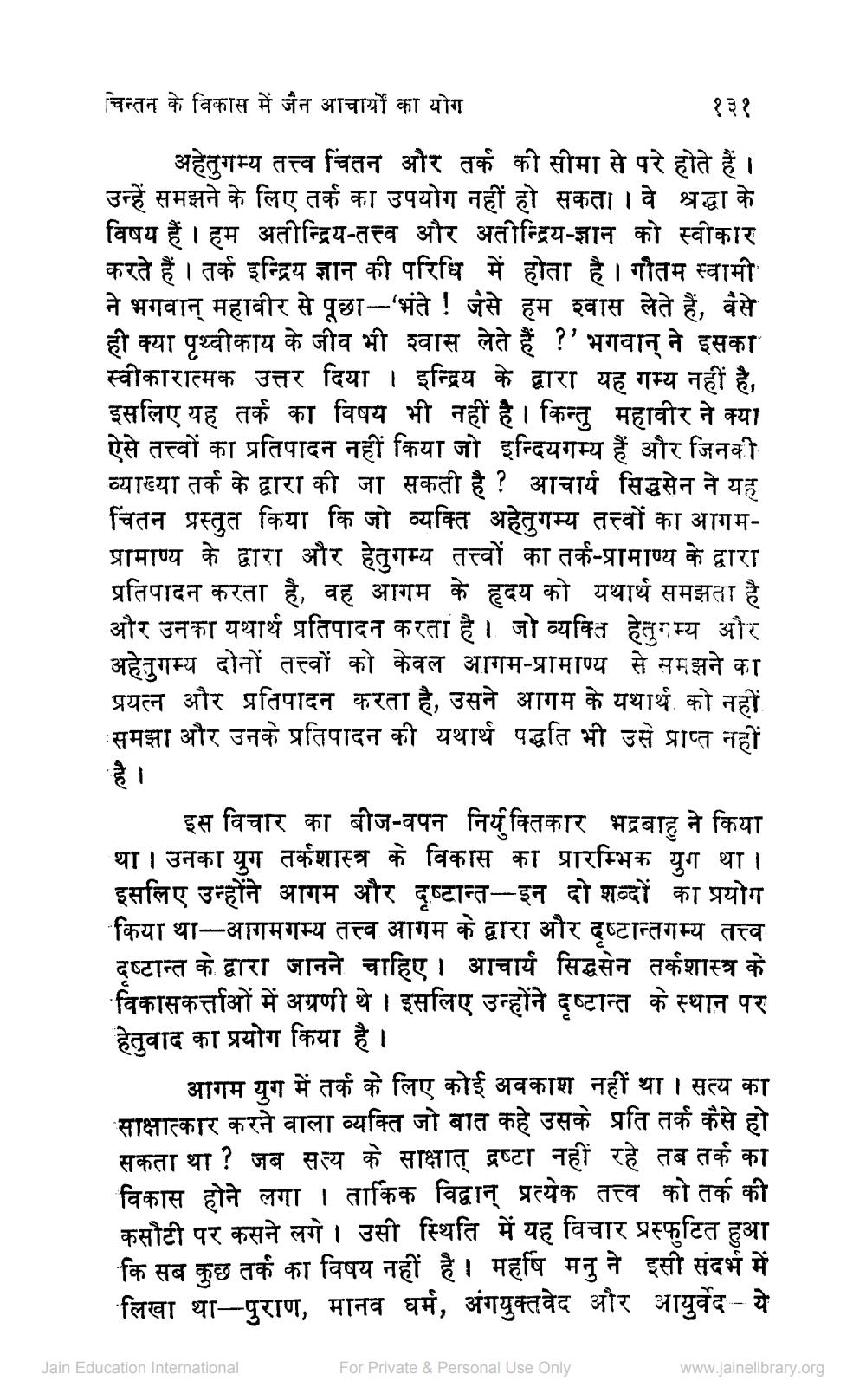________________
चिन्तन के विकास में जैन आचार्यों का योग
१३१
अहेतुगम्य तत्त्व चिंतन और तर्क की सीमा से परे होते हैं । उन्हें समझने के लिए तर्क का उपयोग नहीं हो सकता । वे श्रद्धा के विषय हैं । हम अतीन्द्रिय-तत्त्व और अतीन्द्रिय ज्ञान को स्वीकार करते हैं । तर्क इन्द्रिय ज्ञान की परिधि में होता है । गौतम स्वामी' ने भगवान् महावीर से पूछा - 'भंते ! जैसे हम श्वास लेते हैं, वैसे ही क्या पृथ्वीका के जीव भी श्वास लेते हैं ?' भगवान् ने इसका स्वीकारात्मक उत्तर दिया । इन्द्रिय के द्वारा यह गम्य नहीं है, इसलिए यह तर्क का विषय भी नहीं है । किन्तु महावीर ने क्या ऐसे तत्त्वों का प्रतिपादन नहीं किया जो इन्दियगम्य हैं और जिनकी व्याख्या तर्क के द्वारा की जा सकती है ? आचार्य सिद्धसेन ने यह चितन प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति अहेतुगम्य तत्त्वों का आगमप्रामाण्य के द्वारा और हेतुगम्य तत्त्वों का तर्क - प्रामाण्य के द्वारा प्रतिपादन करता है, वह आगम के हृदय को यथार्थ समझता है और उनका यथार्थ प्रतिपादन करता है । जो व्यक्ति हेतुगम्य और अहेतुगम्य दोनों तत्त्वों को केवल आगम-प्रामाण्य से समझने का प्रयत्न और प्रतिपादन करता है, उसने आगम के यथार्थ को नहीं समझा और उनके प्रतिपादन की यथार्थ पद्धति भी उसे प्राप्त नहीं है ।
इस विचार का बीज - वपन निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने किया था । उनका युग तर्कशास्त्र के विकास का प्रारम्भिक युग था । इसलिए उन्होंने आगम और दृष्टान्त- इन दो शब्दों का प्रयोग किया था - आगमगम्य तत्त्व आगम के द्वारा और दृष्टान्तगम्य तत्त्व दृष्टान्त के द्वारा जानने चाहिए । आचार्य सिद्धसेन तर्कशास्त्र के विकासकर्त्ताओं में अग्रणी थे । इसलिए उन्होंने दृष्टान्त के स्थान पर हेतुवाद का प्रयोग किया है।
आगम युग में तर्क के लिए कोई अवकाश नहीं था । सत्य का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति जो बात कहे उसके प्रति तर्क कैसे हो सकता था ? जब सत्य के साक्षात् द्रष्टा नहीं रहे तब तर्क का विकास होने लगा । तार्किक विद्वान् प्रत्येक तत्त्व को तर्क की कसौटी पर कसने लगे । उसी स्थिति में यह विचार प्रस्फुटित हुआ कि सब कुछ तर्क का विषय नहीं है । महर्षि मनु ने इसी संदर्भ में लिखा था - पुराण, मानव धर्म, अंगयुक्तवेद और आयुर्वेद - ये
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org