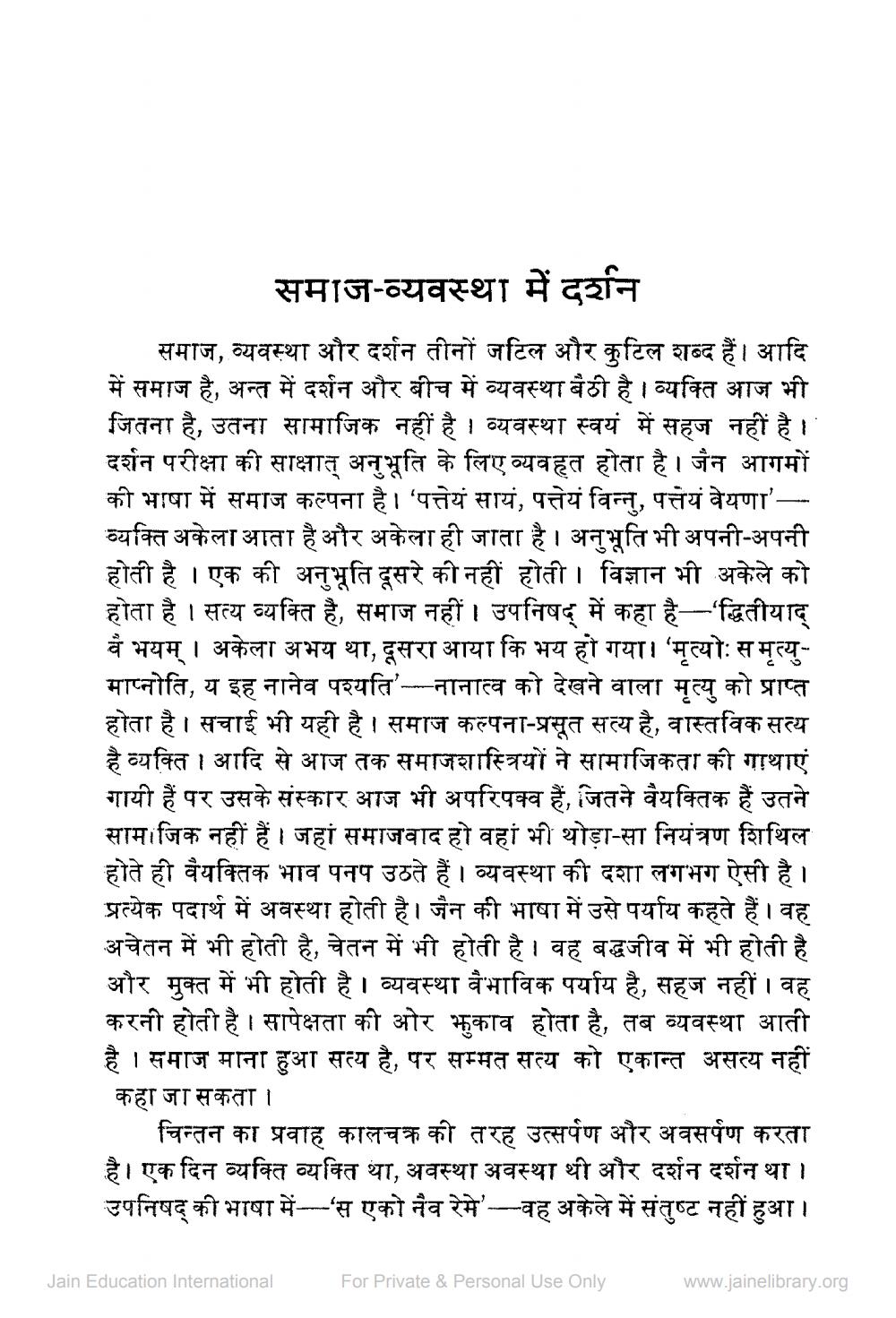________________
समाज-व्यवस्था में दर्शन
समाज, व्यवस्था और दर्शन तीनों जटिल और कुटिल शब्द हैं। आदि में समाज है, अन्त में दर्शन और बीच में व्यवस्था बैठी है। व्यक्ति आज भी जितना है, उतना सामाजिक नहीं है । व्यवस्था स्वयं में सहज नहीं है। दर्शन परीक्षा की साक्षात् अनुभूति के लिए व्यवहृत होता है। जैन आगमों की भाषा में समाज कल्पना है। ‘पत्तेयं सायं, पत्तेयं विन्नु, पत्तेयं वेयणा'व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अनुभूति भी अपनी-अपनी होती है । एक की अनुभूति दूसरे की नहीं होती। विज्ञान भी अकेले को होता है । सत्य व्यक्ति है, समाज नहीं। उपनिषद् में कहा है-'द्धितीयाद् वै भयम् । अकेला अभय था, दूसरा आया कि भय हो गया। 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति'----नानात्व को देखने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है। सचाई भी यही है। समाज कल्पना-प्रसूत सत्य है, वास्तविक सत्य है व्यक्ति । आदि से आज तक समाजशास्त्रियों ने सामाजिकता की गाथाएं गायी हैं पर उसके संस्कार आज भी अपरिपक्व हैं, जितने वैयक्तिक हैं उतने सामाजिक नहीं हैं। जहां समाजवाद हो वहां भी थोड़ा-सा नियंत्रण शिथिल होते ही वैयक्तिक भाव पनप उठते हैं। व्यवस्था की दशा लगभग ऐसी है। प्रत्येक पदार्थ में अवस्था होती है। जैन की भाषा में उसे पर्याय कहते हैं। वह अचेतन में भी होती है, चेतन में भी होती है। वह बद्धजीव में भी होती है और मुक्त में भी होती है। व्यवस्था वैभाविक पर्याय है, सहज नहीं । वह करनी होती है। सापेक्षता की ओर झुकाव होता है, तब व्यवस्था आती है । समाज' माना हुआ सत्य है, पर सम्मत सत्य को एकान्त असत्य नहीं कहा जा सकता।
चिन्तन का प्रवाह कालचक्र की तरह उत्सर्पण और अवसर्पण करता है। एक दिन व्यक्ति व्यक्ति था, अवस्था अवस्था थी और दर्शन दर्शन था। उपनिषद् की भाषा में-'स एको नैव रेमे'--वह अकेले में संतुष्ट नहीं हुआ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org