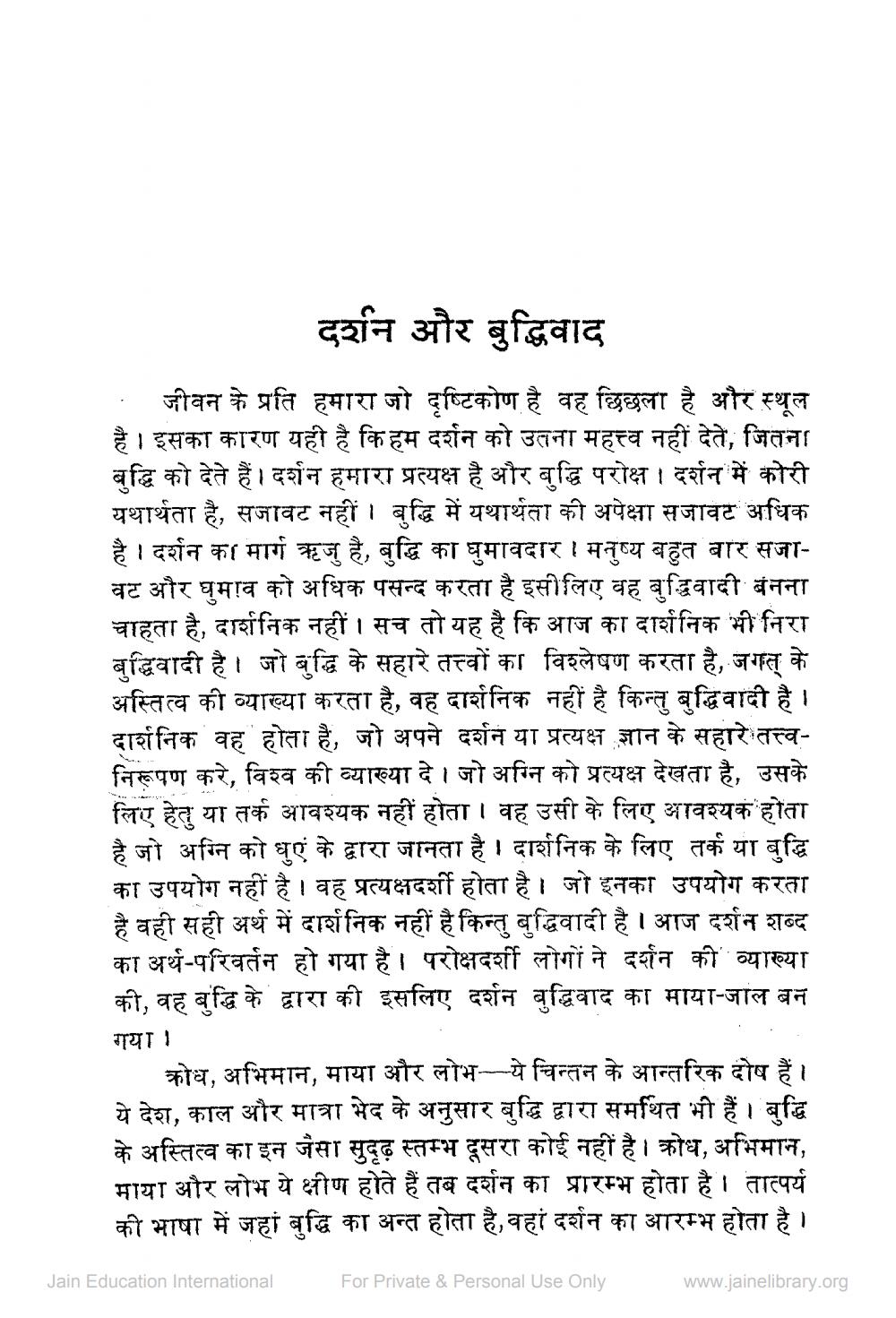________________
दर्शन और बुद्धिवाद . जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वह छिछला है और स्थूल है। इसका कारण यही है कि हम दर्शन को उतना महत्त्व नहीं देते, जितना बुद्धि को देते हैं। दर्शन हमारा प्रत्यक्ष है और बुद्धि परोक्ष । दर्शन में कोरी यथार्थता है, सजावट नहीं। बुद्धि में यथार्थता की अपेक्षा सजावट अधिक है । दर्शन का मार्ग ऋजु है, बुद्धि का घुमावदार । मनुष्य बहुत बार सजावट और घुमाव को अधिक पसन्द करता है इसीलिए वह बुद्धिवादी बनना चाहता है, दार्शनिक नहीं। सच तो यह है कि आज का दार्शनिक भी निरा बद्धिवादी है। जो बुद्धि के सहारे तत्त्वों का विश्लेषण करता है, जगत के अस्तित्व की व्याख्या करता है, वह दार्शनिक नहीं है किन्तु बुद्धिवादी है । दार्शनिक वह होता है, जो अपने दर्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान के सहारे तत्त्वनिरूपण करे, विश्व की व्याख्या दे। जो अग्नि को प्रत्यक्ष देखता है, उसके लिए हेतु या तर्क आवश्यक नहीं होता। वह उसी के लिए आवश्यक होता है जो अग्नि को धुएं के द्वारा जानता है। दार्शनिक के लिए तर्क या बुद्धि का उपयोग नहीं है। वह प्रत्यक्षदर्शी होता है। जो इनका उपयोग करता है वही सही अर्थ में दार्शनिक नहीं है किन्तु बुद्धिवादी है । आज दर्शन शब्द का अर्थ-परिवर्तन हो गया है। परोक्षदर्शी लोगों ने दर्शन की व्याख्या की, वह बुद्धि के द्वारा की इसलिए दर्शन बुद्धिवाद का माया-जाल बन गया। ___ क्रोध, अभिमान, माया और लोभ-ये चिन्तन के आन्तरिक दोष हैं। ये देश, काल और मात्रा भेद के अनुसार बुद्धि द्वारा समर्थित भी हैं। बद्धि के अस्तित्व का इन जैसा सुदृढ़ स्तम्भ दूसरा कोई नहीं है। क्रोध, अभिमान, माया और लोभ ये क्षीण होते हैं तब दर्शन का प्रारम्भ होता है। तात्पर्य की भाषा में जहां बुद्धि का अन्त होता है, वहां दर्शन का आरम्भ होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org