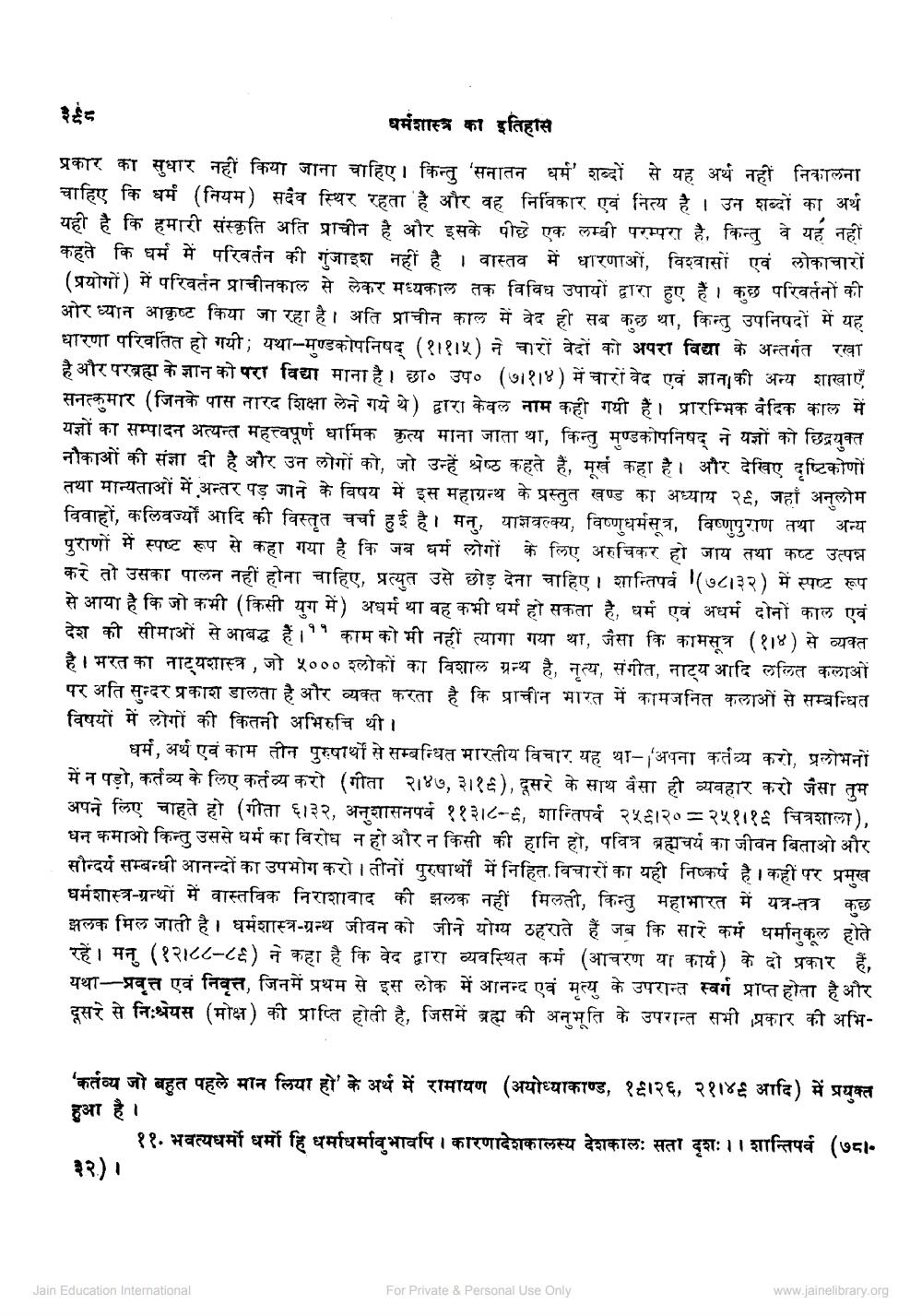________________
છુંદ
धर्मशास्त्र का इतिहास
प्रकार का सुधार नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु 'सनातन धर्म' शब्दों से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि धर्मं (नियम) सदैव स्थिर रहता है और वह निर्विकार एवं नित्य है । उन शब्दों का अर्थ यही है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और इसके पीछे एक लम्बी परम्परा है, किन्तु वे यह नहीं कहते कि धर्म में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है । वास्तव में धारणाओं, विश्वासों एवं लोकाचारों (प्रयोगों) में परिवर्तन प्राचीनकाल से लेकर मध्यकाल तक विविध उपायों द्वारा हुए हैं। कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अति प्राचीन काल में वेद ही सब कुछ था, किन्तु उपनिषदों में यह धारणा परिवर्तित हो गयी; यथा-मुण्डकोपनिषद् (१।१।५ ) ने चारों वेदों को अपरा विद्या के अन्तर्गत रखा है और परब्रह्म के ज्ञान को परा विद्या माना है । छा० उप० (७११।४ ) में चारों वेद एवं ज्ञान की अन्य शाखाएँ सनत्कुमार (जिनके पास नारद शिक्षा लेने गये थे ) द्वारा केवल नाम कही गयी हैं। प्रारम्भिक वैदिक काल में यज्ञों का सम्पादन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक कृत्य माना जाता था, किन्तु मुण्डकोपनिषद् ने यज्ञों को छिद्रयुक्त नौकाओं की संज्ञा दी है और उन लोगों को, जो उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं, मूर्ख कहा है। और देखिए दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं में अन्तर पड़ जाने के विषय में इस महाग्रन्थ के प्रस्तुत खण्ड का अध्याय २६, जहाँ अनुलोम विवाहों, कलिवर्ज्यो आदि की विस्तृत चर्चा हुई है । मनु याज्ञवल्क्य, विष्णुधर्मसूत्र, विष्णुपुराण तथा अन्य पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब धर्म लोगों के लिए अरुचिकर हो जाय तथा कष्ट उत्पन्न करे तो उसका पालन नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे छोड़ देना चाहिए । शान्तिपर्व | ( ७८०३२ ) में स्पष्ट रूप से आया है कि जो कभी ( किसी युग में) अधर्म था वह कभी धर्म हो सकता है, धर्म एवं अधर्म दोनों काल एवं देश की सीमाओं से आबद्ध हैं । " " काम को भी नहीं त्यागा गया था, जैसा कि कामसूत्र ( १।४ ) से व्यक्त है । भरत का नाट्यशास्त्र, जो ५००० श्लोकों का विशाल ग्रन्थ है, नृत्य, संगीत, नाट्य आदि ललित कलाओं पर अति सुन्दर प्रकाश डालता है और व्यक्त करता है कि प्राचीन भारत में कामजनित कलाओं से सम्बन्धित विषयों में लोगों की कितनी अभिरुचि थी ।
धर्म, अर्थ एवं काम तीन पुरुषार्थों से सम्बन्धित भारतीय विचार यह था - अपना कर्तव्य करो, प्रलोभनों में न पड़ो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो ( गीता २/४७, ३।१६ ), दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो ( गीता ६।३२, अनुशासनपर्व ११३८ - ६, शान्तिपर्व २५६/२० = २५१।१६ चित्रशाला ), धन कमाओ किन्तु उससे धर्म का विरोध न हो और न किसी की हानि हो, पवित्र ब्रह्मचर्य का जीवन बिताओ और सौन्दर्य सम्बन्धी आनन्दों का उपभोग करो । तीनों पुरुषार्थों में निहित विचारों का यही निष्कर्ष है । कहीं पर प्रमुख धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में वास्तविक निराशावाद की झलक नहीं मिलती, किन्तु महाभारत में यत्र-तत्र झलक मिल जाती है। धर्मशास्त्र-ग्रन्थ जीवन को जीने योग्य ठहराते हैं जब कि सारे कर्म धर्मानुकूल होते रहें । मनु ( १२१८८ - ८६ ) ने कहा है कि वेद द्वारा व्यवस्थित कर्म ( आचरण या कार्य) के दो प्रकार हैं, यथा- प्रवृत्त एवं निवृत्त, जिनमें प्रथम से इस लोक में आनन्द एवं मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग प्राप्त होता है और दूसरे से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, जिसमें ब्रह्म की अनुभूति के उपरान्त सभी प्रकार की अभि
कछ
'कर्तव्य जो बहुत पहले मान लिया हो' के अर्थ में रामायण ( अयोध्याकाण्ड, १६ २६, २१०४६ आदि) में प्रयुक्त हुआ है।
११. भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्मावुभावपि । कारणादेशकालस्य देशकालः सता दृशः । । शान्तिपर्व ( ७८/०
३२) ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org