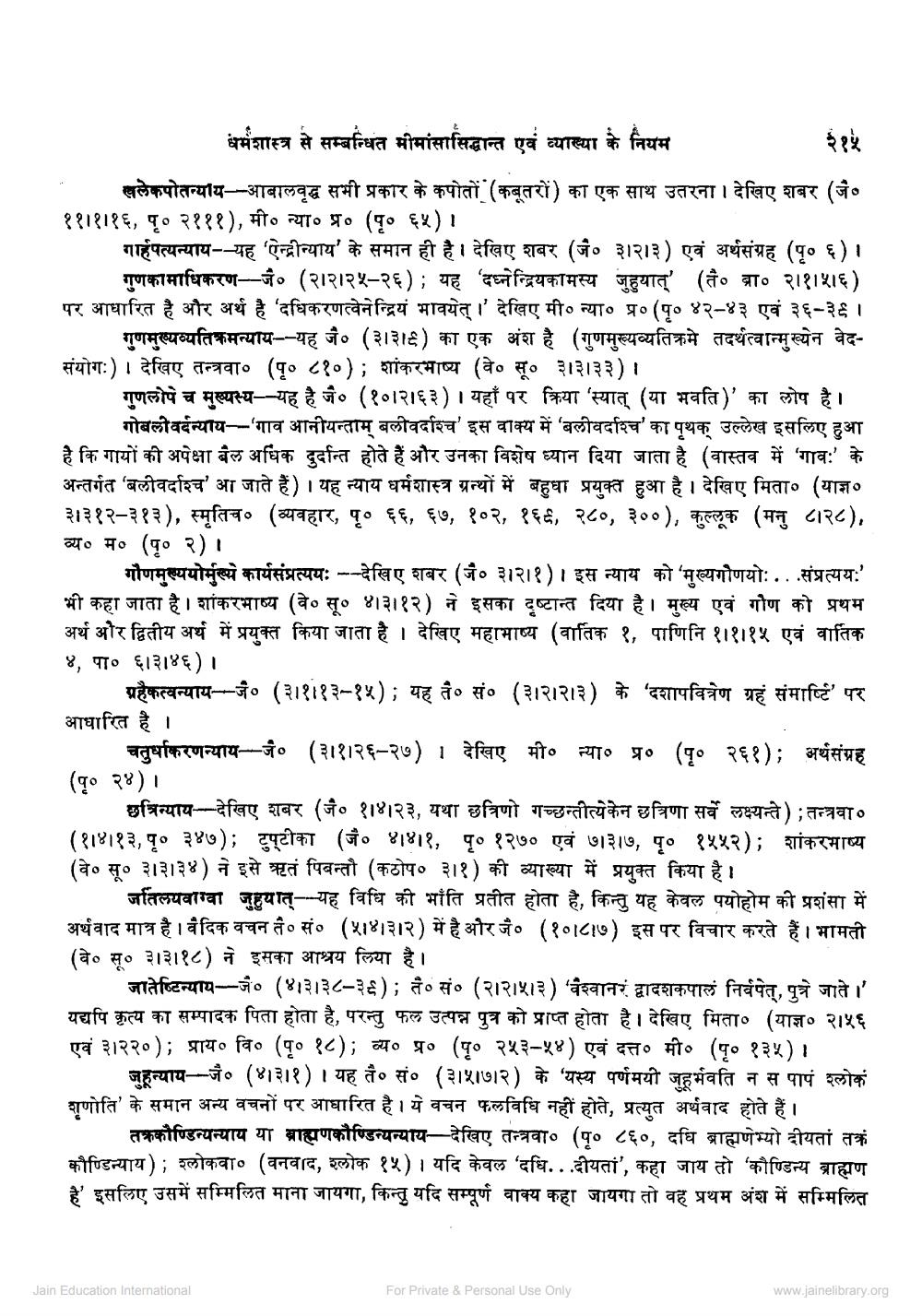________________
२१५
धर्मशास्त्र से सम्बन्धित मीमांसासिद्धान्त एवं व्याख्या के नियम खलेकपोतन्याय--आबालवृद्ध सभी प्रकार के कपोतों (कबूतरों) का एक साथ उतरना। देखिए शबर (ज० ११।१।१६, पृ० २१११), मी० न्या० प्र० (पृ. ६५)।
गार्हपत्यन्याय--यह 'ऐन्द्रीन्याय' के समान ही है । देखिए शबर (जे० ३।२।३) एवं अर्थसंग्रह (पृ० ६) ।
गुणकामाधिकरण-जै० (२।२।२५-२६); यह 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' (तै० ब्रा० २।१।२६) पर आधारित है और अर्थ है 'दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेत् ।' देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० ४२-४३ एवं ३६-३६ ।
गुणमुख्यव्यतिक्रमन्याय--यह जै० (३।३।६) का एक अंश है (गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः) । देखिए तन्त्रवा० (पृ० ८१०); शांकरभाष्य (वे० सू० ३।३।३३)।
गुणलोपे च मुख्यस्य--यह है जै० (१०।२।६३) । यहाँ पर क्रिया 'स्यात् (या भवति)' का लोप है।
गोबलोवर्दन्याय-'गाव आनीयन्ताम् बलीवर्दाश्च' इस वाक्य में 'बलीवाश्च' का पृथक् उल्लेख इसलिए हुआ है कि गायों की अपेक्षा बैल अधिक दुर्दान्त होते हैं और उनका विशेष ध्यान दिया जाता है (वास्तव में 'गावः' के अन्तर्गत 'बलीवर्दाश्च' आ जाते हैं)। यह न्याय धर्मशास्त्र ग्रन्थों में बहुधा प्रयुक्त हुआ है । देखिए मिता० (याज्ञ० ३६३१२-३१३), स्मृतिच० (व्यवहार, पृ० ६६, ६७, १०२, १६६, २८०, ३००), कुल्लूक (मनु ८१२८), व्य० म० (पृ० २)।
गौणमुख्ययोर्मुख्य कार्यसंप्रत्ययः --देखिए शबर (ज० ३।२।१)। इस न्याय को 'मुख्यगौणयोः . . .संप्रत्ययः' भी कहा जाता है। शांकरभाष्य (वे० सू० ४।३।१२) ने इसका दृष्टान्त दिया है। मुख्य एवं गौण को प्रथम अर्थ और द्वितीय अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है । देखिए महाभाष्य (वार्तिक १, पाणिनि १।१।१५ एवं वार्तिक ४, पा० ६।३।४६)।
ग्रहैकत्वन्याय-ज० (३।१।१३-१५); यह तै० सं० (३।२।२।३) के 'दशापवित्रेण ग्रहं समाष्टि' पर आधारित है ।
चतुर्धाकरणन्याय-० (३।१।२६-२७) 1 देखिए मी० न्या० प्र० (पृ० २६१); अर्थसंग्रह (पृ० २४)।
- छत्रिन्याय-देखिए शबर (जै० १।४।२३, यथा छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्ते) ; तन्त्रवा० (१।४।१३, पृ० ३४७); टुप्टीका (जै० ४।४।१, पृ० १२७० एवं ७।३।७, पृ० १५५२); शांकरभाष्य (वे० सू० ३।३।३४) ने इसे ऋतं पिबन्तौ (कठोप० ३।१) की व्याख्या में प्रयुक्त किया है।
जतिलयवाग्वा जुहुयात्--यह विधि की भाँति प्रतीत होता है, किन्तु यह केवल पयोहोम की प्रशंसा में अर्थवाद मात्र है । वैदिक वचन तै० सं० (५।४।३।२) में है और जै० (१०८१७) इस पर विचार करते हैं। भामती (वे० सू० ३।३।१८) ने इसका आश्रय लिया है।
जातेष्टिन्याय-जै० (४।३।३८-३६); तै० सं० (२।२।५।३) 'वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्, पुढे जाते।' यद्यपि कृत्य का सम्पादक पिता होता है, परन्तु फल उत्पन्न पुत्र को प्राप्त होता है। देखिए मिता० (याज्ञ० २०५६ एवं ३।२२०); प्राय० वि० (पृ० १८); व्य० प्र० (पृ० २५३-५४) एवं दत्त० मी० (पृ० १३५) ।
जुहून्याय-जै० (४१३१) । यह तै० सं० (३।७।२) के 'यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शणोति' के समान अन्य वचनों पर आधारित है। ये वचन फलविधि नहीं होते, प्रत्युत अर्थवाद होते हैं ।
तक्रकौण्डिन्यन्याय या ब्राह्मणकौण्डिन्यन्याय-देखिए तन्त्रवा० (पृ० ८६०, दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तकं कौण्डिन्याय); श्लोकवा० (वनवाद, श्लोक १५)। यदि केवल 'दधि...दीयता', कहा जाय तो 'कौण्डिन्य ब्राह्मण है' इसलिए उसमें सम्मिलित माना जायगा, किन्तु यदि सम्पूर्ण वाक्य कहा जायगा तो वह प्रथम अंश में सम्मिलित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org