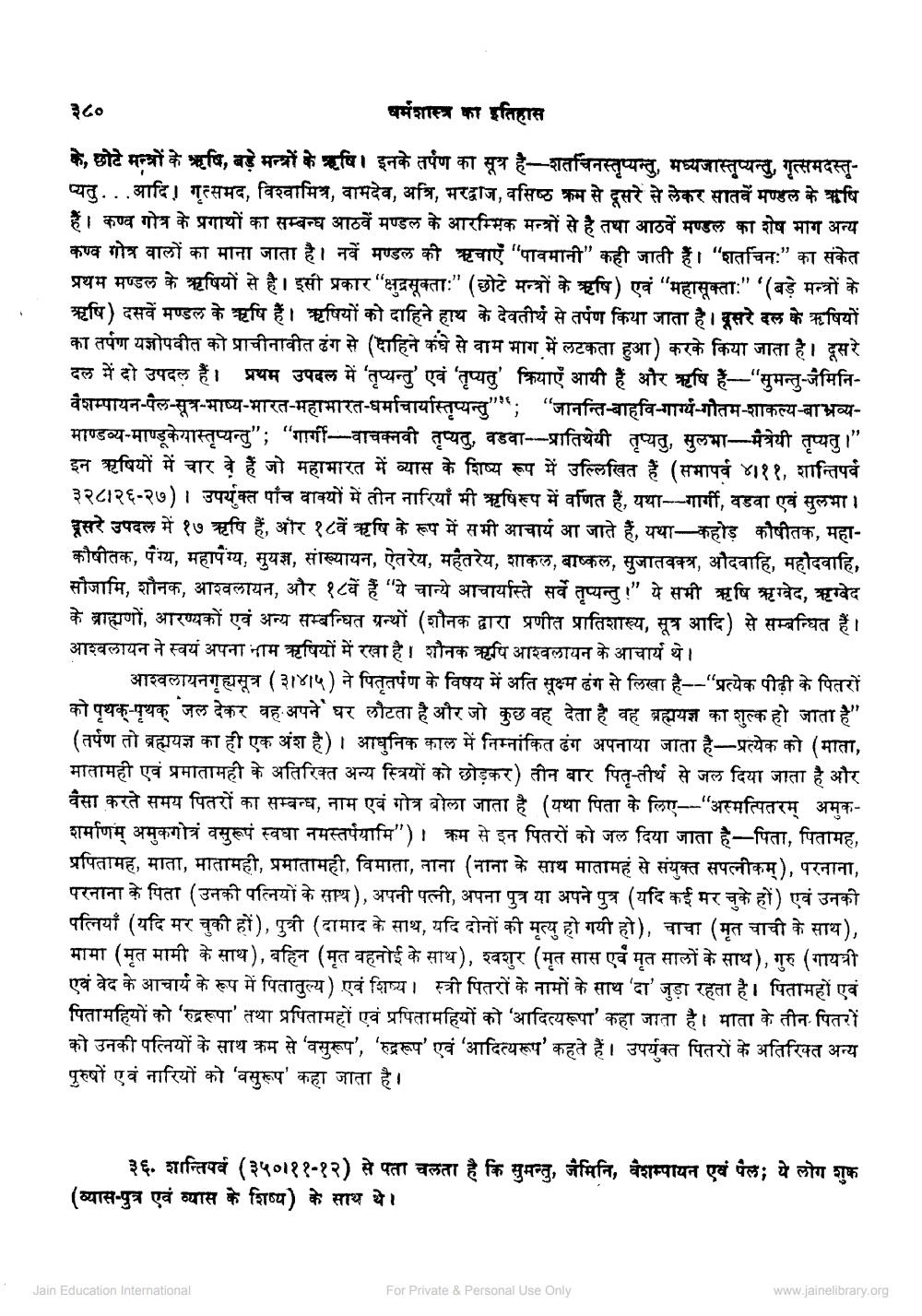________________
३८०
धर्मशास्त्र का इतिहास
के, छोटे मन्त्रों के ऋषि, बड़े मन्त्रों के ऋषि । इनके तर्पण का सूत्र है - शतचनस्तृप्यन्तु मध्यजास्तृप्यन्तु, गृत्समदस्तुप्यतु... आदि । गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ क्रम से दूसरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि हैं । कण्व गोत्र के प्रगायों का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का शेष भाग अन्य ava गोत्र वालों का माना जाता है। नवें मण्डल की ऋचाएँ "पावमानी" कही जाती हैं। "शर्ताचनः" का संकेत प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार "क्षुद्रसूक्ता:" (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं " महासूक्ता: " ' ( बड़े मन्त्रों के ऋषि) दसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देवतीर्थं से तर्पण किया जाता है। दूसरे दल के ऋषियों का तर्पण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढंग से (दाहिने कंधे से वाम भाग में लटकता हुआ) करके किया जाता है । दूसरे दल में दो उपदल हैं । प्रथम उपदल में 'तृप्यन्तु' एवं 'तृप्यतु' क्रियाएँ आयी हैं और ऋषि हैं- "सुमन्तु जैमिनिवैशम्पायन - पैल - सूत्र - भाष्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तृप्यन्तु ""; "जानन्ति बाहवि- गार्ग्य-गौतम- शाकल्य - बाभ्रव्य - माण्डव्य-माण्डूकेयास्तृप्यन्तु"; " गार्गी - वाचक्नवी तृप्यतु, वडवा -- प्रातिथेयी तृप्यतु, सुलभा - मैत्रेयी तृप्यतु ।” इन ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं ( सभापर्व ४।११, शान्तिपर्व ३२८।२६-२७) । उपर्युक्त पाँच वाक्यों में तीन नारियाँ भी ऋषिरूप में वर्णित हैं, यथा--गार्गी, वडवा एवं सुलभा । दूसरे उपदल में १७ ऋषि हैं, और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं, यथा-कहोड़ कौषीतक, महाकौषीतक, पैग्य, महापग्य, सुयश, सांख्यायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजातवक्त्र, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौनक, आश्वलायन, और १८वें हैं "ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु !” ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों ( शौनक द्वारा प्रणीत प्रातिशाख्य, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं । आश्वलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। शौनक ऋषि आश्वलायन के आचार्य थे।
--
आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४/५ ) ने पितृतर्पण के विषय में अति सूक्ष्म ढंग से लिखा है -- "प्रत्येक पीढ़ी के पितरों को पृथक्-पृथक् जल देकर वह अपने घर लौटता है और जो कुछ वह देता है वह ब्रह्मयज्ञ का शुल्क हो जाता है" ( तर्पण तो ब्रह्मयज्ञ का ही एक अंश है ) । आधुनिक काल में निम्नांकित ढंग अपनाया जाता है - प्रत्येक को (माता, मातामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितृ तीर्थ से जल दिया जाता है और वैसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के लिए - " अस्मत्पितरम् अमुकशर्माणम् अमुकगोत्रं वसुरूपं स्वधा नमस्तर्पयामि " ) । क्रम से इन पितरों को जल दिया जाता है - पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना ( नाना के साथ मातामहं से संयुक्त सपत्नीकम् ), परनाना, परनाना के पिता ( उनकी पत्नियों के साथ), अपनी पत्नी, अपना पुत्र या अपने पुत्र ( यदि कई मर चुके हों) एवं उनकी पत्नियाँ ( यदि मर चुकी हों), पुत्री (दामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो ), चाचा (मृत चाची के साथ), मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत बहनोई के साथ), श्वशुर ( मृत सास एवं मृत सालों के साथ), गुरु ( गायत्री एवं वेद के आचार्य के रूप में पितातुल्य) एवं शिष्य । स्त्री पितरों के नामों के साथ 'दा' जुड़ा रहता है । पितामहों एवं पिता महियों को 'रुद्ररूपा तथा प्रपितामहों एवं प्रपितामहियों को 'आदित्यरूपा' कहा जाता है। माता के तीन पितरों को उनकी पत्नियों के साथ क्रम से 'वसुरूप', 'रुद्ररूप' एवं 'आदित्यरूप' कहते हैं। उपर्युक्त पितरों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों एवं नारियों को 'वसुरूप' कहा जाता है।
३६. शान्तिपर्व ( ३५००११-१२) से पता चलता है कि सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल; ये लोग शुक ( व्यास-पुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org