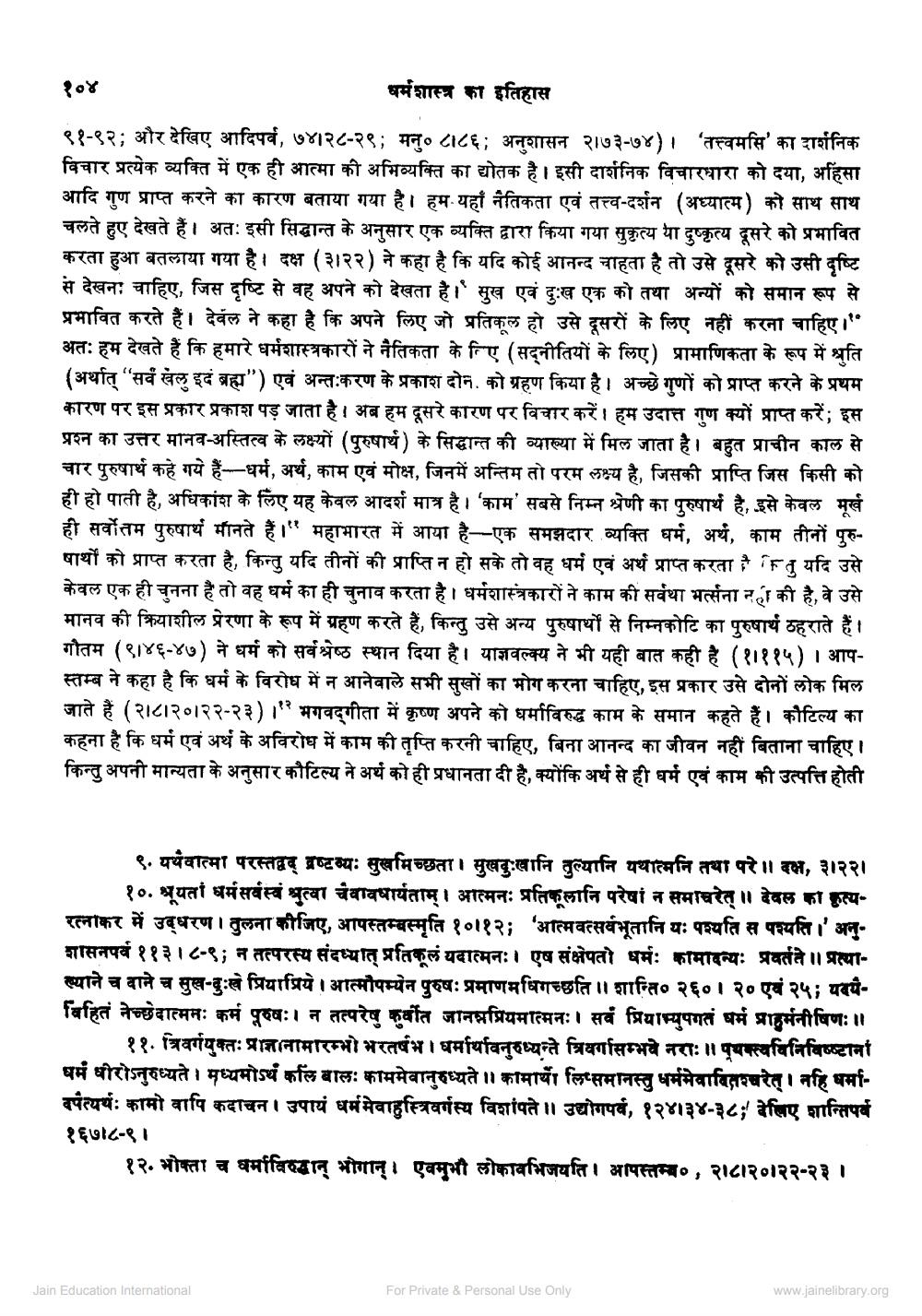________________
१०४
धर्मशास्त्र का इतिहास
९१-९२; और देखिए आदिपर्व ७४।२८-२९; मनु० ८|८६; अनुशासन २।७३-७४) । 'तत्त्वमसि' का दार्शनिक विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का द्योतक है। इसी दार्शनिक विचारधारा को दया, अहिंसा आदि 'गुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यहाँ नैतिकता एवं तत्त्व-दर्शन ( अध्यात्म) को साथ साथ चलते हुए देखते हैं । अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुकृत्य या दुष्कृत्य दूसरे को प्रभावित करता हुआ बतलाया गया है। दक्ष ( ३।२२ ) ने कहा है कि यदि कोई आनन्द चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है। सुख एवं दुःख एक को तथा अन्यों को समान रूप से प्रभावित करते हैं । देवल ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूल हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए।" अतः हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सद्द्वीतियों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में श्रुति ( अर्थात् "सर्वं खेल इदं ब्रह्म" ) एवं अन्तःकरण के प्रकाश दोन. को ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गुण क्यों प्राप्त करें; इस प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तित्व के लक्ष्यों (पुरुषार्थ ) के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से चार पुरुषार्थ कहे गये हैं-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम तो परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को ही हो पाती है, अधिकांश के लिए यह केवल आदर्श मात्र है । 'काम' सबसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ है, इसे केवल मूर्ख ही सर्वोत्तम पुरुषार्थं मानते हैं।" महाभारत में आया है - एक समझदार व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थी को प्राप्त करता है, किन्तु यदि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो वह धर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है कि तु यदि उसे केवल एक ही चुनना है तो वह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा भर्त्सना नहीं की है, वे उसे मानव की क्रियाशील प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, किन्तु उसे अन्य पुरुषार्थों से निम्नकोटि का पुरुषार्थ ठहराते हैं। गौतम ( ९/४६-४७ ) ने धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य ने भी यही बात कही है ( १।११५ ) | आपस्तम्ब ने कहा है कि धर्म के विरोध में न आनेवाले सभी सुखों का भोग करना चाहिए, इस प्रकार उसे दोनों लोक मिल जाते हैं (२८१२०२२-२३) । भगवद्गीता में कृष्ण अपने को धर्माविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का कहना है कि धर्म एवं अर्थ के अविरोध में काम की तृप्ति करनी चाहिए, बिना आनन्द का जीवन नहीं बिताना चाहिए। किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने अर्थ को ही प्रधानता दी है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती
९. यथैवात्मा परस्तद्वद् प्रष्टव्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे । दक्ष, ३।२२। १०. श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् । देवल का कृत्यरत्नाकर में उद्धरण । तुलना कीजिए, आपस्तम्बस्मृति १०।१२; 'आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।' अनुशासनपर्व ११३ । ८- ९; न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः । एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ प्रत्याख्याने च दाने च सुख-दुःखे प्रियाप्रिये। आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ।। शान्ति० २६० । २० एवं २५; यवयैविहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः । न तत्परेषु कुर्वीत जाननप्रियमात्मनः । सवं प्रियाभ्युपगतं धर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥ ११. त्रिवर्गयुक्तः प्राज्ञानामारम्भो भरतर्षभ । धर्मार्थावनुरुध्यन्ते त्रिवर्गासम्भवे नराः ॥ पृथक्त्वविनिविष्टानां घमं धीरोऽनुरुध्यते । मध्यमोऽथं कॉल बालः काममेवानुरुध्यते ॥ कामार्थी लिप्समानस्तु धर्ममेवावितश्चरेत् । नहि धर्मावत्यर्थः कामो वापि कदाचन । उपायं धर्ममेवाहुस्त्रिवर्गस्य विशांपते । उद्योगपर्व, १२४।३४-३८; बेलिए शान्तिपर्व १६७१८-९ ।
१२. भोक्ता च धर्माविरुद्धान् भोगान् । एवमुभौ लोकावभिजयति । अपस्तम्ब०, २१८/२०१२२-२३ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org