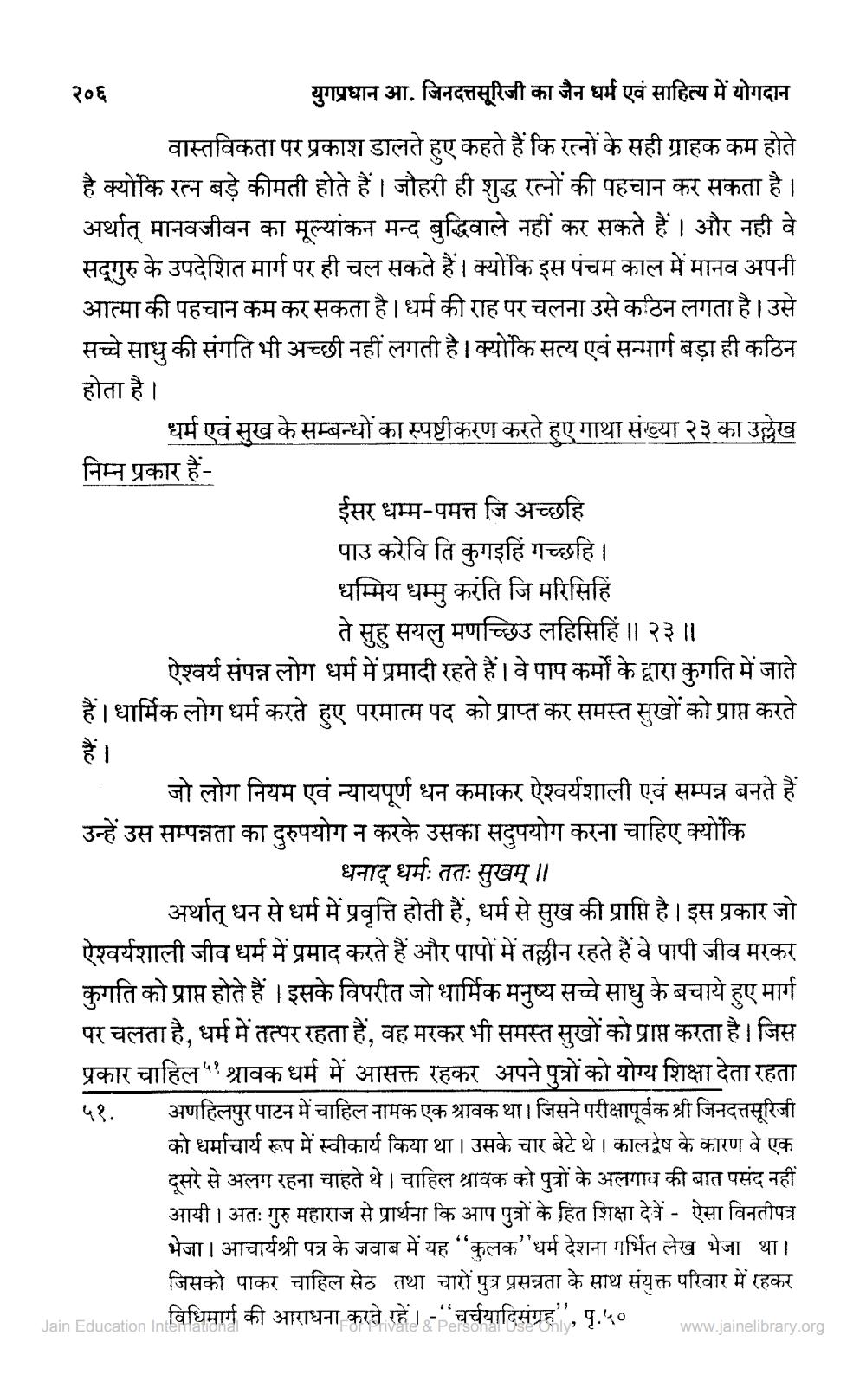________________
२०६
युगप्रधान आ. जिनदत्तसूरिजी का जैन धर्म एवं साहित्य में योगदान वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि रत्नों के सही ग्राहक कम होते है क्योंकि रत्न बड़े कीमती होते हैं। जौहरी ही शुद्ध रत्नों की पहचान कर सकता है। अर्थात् मानवजीवन का मूल्यांकन मन्द बुद्धिवाले नहीं कर सकते हैं। और नही वे सद्गुरु के उपदेशित मार्ग पर ही चल सकते हैं। क्योंकि इस पंचम काल में मानव अपनी आत्मा की पहचान कम कर सकता है। धर्म की राह पर चलना उसे कठिन लगता है। उसे सच्चे साधु की संगति भी अच्छी नहीं लगती है। क्योकि सत्य एवं सन्मार्ग बड़ा ही कठिन होता है।
धर्म एवं सुख के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण करते हुए गाथा संख्या २३ का उल्लेख निम्न प्रकार हैं
ईसर धम्म-पमत्त जि अच्छहि पाउ करेवि ति कुगइहिं गच्छहि। धम्मिय धम्मु करंति जि मरिसिहिं
ते सुहु सयलु मणच्छिउ लहिसिहिं ।। २३ ॥ ऐश्वर्य संपन्न लोग धर्म में प्रमादी रहते हैं। वे पाप कर्मों के द्वारा कुगति में जाते हैं। धार्मिक लोग धर्म करते हुए परमात्म पद को प्राप्त कर समस्त सुखों को प्राप्त करते
जो लोग नियम एवं न्यायपूर्ण धन कमाकर ऐश्वर्यशाली एवं सम्पन्न बनते हैं उन्हें उस सम्पन्नता का दुरुपयोग न करके उसका सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि
धनाद् धर्मः ततः सुखम् ॥ अर्थात् धन से धर्म में प्रवृत्ति होती हैं, धर्म से सुख की प्राप्ति है। इस प्रकार जो ऐश्वर्यशाली जीव धर्म में प्रमाद करते हैं और पापों में तल्लीन रहते हैं वे पापी जीव मरकर कुगति को प्राप्त होते हैं । इसके विपरीत जो धार्मिक मनुष्य सच्चे साधु के बचाये हुए मार्ग पर चलता है, धर्म में तत्पर रहता हैं, वह मरकर भी समस्त सुखों को प्राप्त करता है। जिस प्रकार चाहिल५१ श्रावक धर्म में आसक्त रहकर अपने पुत्रों को योग्य शिक्षा देता रहता ५१. अणहिलपुर पाटन में चाहिल नामक एक श्रावक था। जिसने परीक्षापूर्वक श्री जिनदत्तसूरिजी
को धर्माचार्य रूप में स्वीकार्य किया था। उसके चार बेटे थे। कालद्वेष के कारण वे एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे। चाहिल श्रावक को पुत्रों के अलगाव की बात पसंद नहीं आयी। अतः गुरु महाराज से प्रार्थना कि आप पुत्रों के हित शिक्षा देवें - ऐसा विनतीपत्र भेजा । आचार्यश्री पत्र के जवाब में यह “कुलक"धर्म देशना गर्भित लेख भेजा था।
जिसको पाकर चाहिल सेठ तथा चारों पुत्र प्रसन्नता के साथ संयुक्त परिवार में रहकर Jain Education 1 विधिमार्ग की आराधना करते रहें। -“चर्चयादिसंग्रह', पृ.५०
www.jainelibrary.org