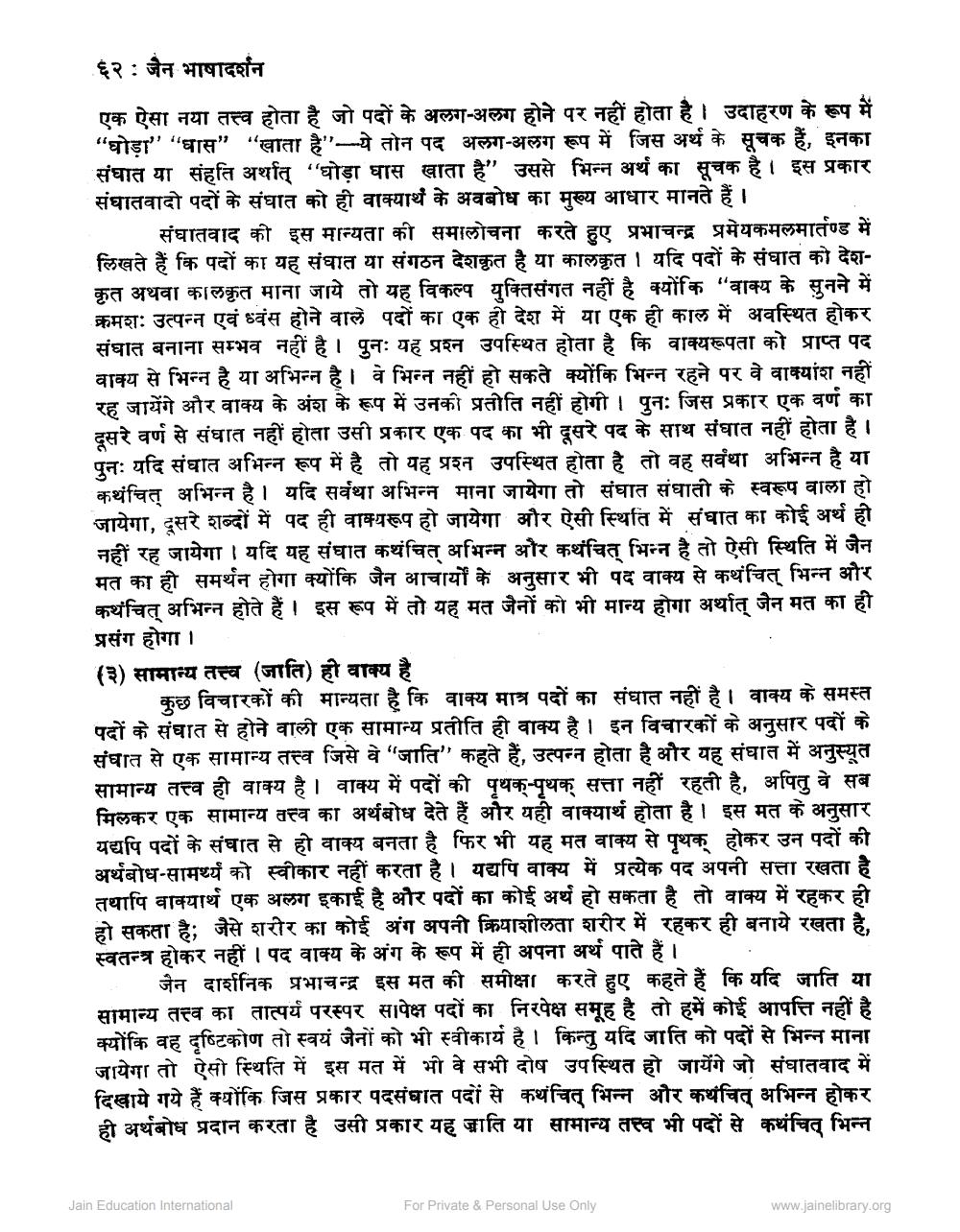________________
६२ : जैन भाषादर्शन एक ऐसा नया तत्त्व होता है जो पदों के अलग-अलग होने पर नहीं होता है। उदाहरण के रूप में "घोड़ा" "घास" "खाता है"-ये तोन पद अलग-अलग रूप में जिस अर्थ के सूचक हैं, इनका संघात या संहति अर्थात् "घोड़ा घास खाता है" उससे भिन्न अर्थ का सूचक है। इस प्रकार संघातवादो पदों के संघात को ही वाक्याथ के अवबोध का मुख्य आधार मानते हैं।
संघातवाद की इस मान्यता की समालोचना करते हुए प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्ड में लिखते हैं कि पदों का यह संघात या संगठन देशकृत है या कालकृत । यदि पदों के संघात को देशकृत अथवा कालकृत माना जाये तो यह विकल्प युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि "वाक्य के सुनने में क्रमशः उत्पन्न एवं ध्वंस होने वाले पदों का एक ही देश में या एक ही काल में अवस्थित होकर संघात बनाना सम्भव नहीं है । पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वाक्यरूपता को प्राप्त पद वाक्य से भिन्न है या अभिन्न है। वे भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि भिन्न रहने पर वे वाक्यांश नहीं रह जायेंगे और वाक्य के अंश के रूप में उनकी प्रतीति नहीं होगी। पुनः जिस प्रकार एक वर्ण का दूसरे वर्ण से संघात नहीं होता उसी प्रकार एक पद का भी दूसरे पद के साथ संघात नहीं होता है । पुनः यदि संघात अभिन्न रूप में है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है तो वह सर्वथा अभिन्न है या कथंचित् अभिन्न है। यदि सर्वथा अभिन्न माना जायेगा तो संघात संघाती के स्वरूप वाला हो जायेगा, दूसरे शब्दों में पद ही वाक्यरूप हो जायेगा और ऐसी स्थिति में संघात का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा । यदि यह संघात कथंचित् अभिन्न और कथंचित् भिन्न है तो ऐसी स्थिति में जैन मत का ही समर्थन होगा क्योंकि जैन आचार्यों के अनुसार भी पद वाक्य से कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न होते हैं। इस रूप में तो यह मत जैनों को भी मान्य होगा अर्थात् जैन मत का ही प्रसंग होगा। (३) सामान्य तत्त्व (जाति) ही वाक्य है
कछ विचारकों की मान्यता है कि वाक्य मात्र पदों का संघात नहीं है। वाक्य के समस्त पदों के संघात से होने वाली एक सामान्य प्रतीति ही वाक्य है। इन विचारकों के अनुसार पदों के संघात से एक सामान्य तत्त्व जिसे वे "जाति" कहते हैं, उत्पन्न होता है और यह संघात में अनुस्यूत सामान्य तत्त्व ही वाक्य है। वाक्य में पदों की पृथक्-पृथक् सत्ता नहीं रहती है, अपितु वे सब मिलकर एक सामान्य तत्त्व का अर्थबोध देते हैं और यही वाक्यार्थ होता है। इस मत के अनुसार यद्यपि पदों के संघात से हो वाक्य बनता है फिर भी यह मत वाक्य से पृथक् होकर उन पदों की अर्थबोध-सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि वाक्य में प्रत्येक पद अपनी सत्ता रखता है
वाक्यार्थ एक अलग इकाई है और पदों का कोई अर्थ हो सकता है तो वाक्य में रहकर ही हो सकता है; जैसे शरीर का कोई अंग अपनी क्रियाशीलता शरीर में रहकर ही बनाये रखता है, स्वतन्त्र होकर नहीं । पद वाक्य के अंग के रूप में ही अपना अर्थ पाते हैं।
जैन दार्शनिक प्रभाचन्द्र इस मत की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि यदि जाति या सामान्य तत्त्व का तात्पर्य परस्पर सापेक्ष पदों का निरपेक्ष समूह है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह दृष्टिकोण तो स्वयं जैनों को भी स्वीकार्य है। किन्तु यदि जाति को पदों से भिन्न माना
गा तो ऐसी स्थिति में इस मत में भी वे सभी दोष उपस्थित हो जायेंगे जो संघातवाद में दिखाये गये हैं क्योंकि जिस प्रकार पदसंघात पदों से कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न होकर ही अर्थबोध प्रदान करता है उसी प्रकार यह जाति या सामान्य तत्व भी पदों से कथंचित् भिन्न
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org