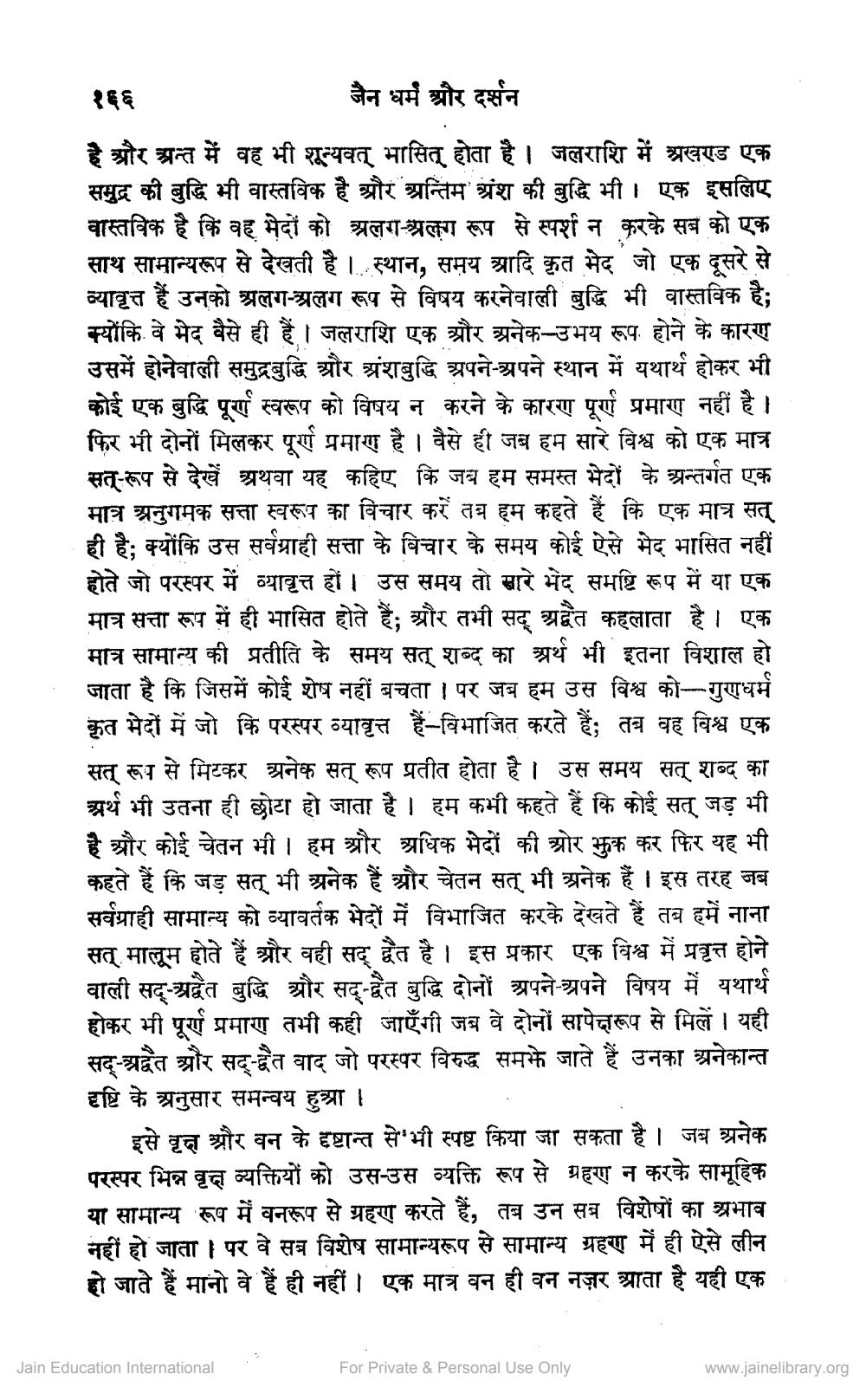________________
१६६
जैन धर्म और दर्शन है और अन्त में वह भी शून्यवत् भासित् होता है। जलराशि में अखण्ड एक समुद्र की बुद्धि भी वास्तविक है और अन्तिम अंश की बुद्धि भी। एक इसलिए वास्तविक है कि वह भेदों को अलग-अलग रूप से स्पर्श न करके सब को एक साथ सामान्यरूप से देखती है। स्थान, समय आदि कृत भेद जो एक दूसरे से व्यावृत्त हैं उनको अलग-अलग रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी वास्तविक है; क्योंकि वे भेद वैसे ही हैं । जलराशि एक और अनेक-उभय रूप होने के कारण उसमें होनेवाली समुद्रबुद्धि और अंशबुद्धि अपने-अपने स्थान में यथार्थ होकर भी कोई एक बुद्धि पूर्ण स्वरूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। फिर भी दोनों मिलकर पूर्ण प्रमाण है। वैसे ही जब हम सारे विश्व को एक मात्र सत्-रूप से देखें अथवा यह कहिए कि जब हम समस्त भेदों के अन्तर्गत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वरूप का विचार करें तब हम कहते हैं कि एक मात्र सत् ही है; क्योंकि उस सर्वग्राही सत्ता के विचार के समय कोई ऐसे भेद भासित नहीं होते जो परस्पर में व्यावृत्त हों। उस समय तो सारे भेद समष्टि रूप में या एक मात्र सत्ता रूप में ही भासित होते हैं; और तभी सद् अद्वैत कहलाता है। एक मात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत् शब्द का अर्थ भी इतना विशाल हो जाता है कि जिसमें कोई शेष नहीं बचता। पर जब हम उस विश्व को-गुणधर्म कृत भेदों में जो कि परस्पर व्यावृत्त हैं-विभाजित करते हैं; तब वह विश्व एक सत् रूप से मिटकर अनेक सत् रूप प्रतीत होता है। उस समय सत् शब्द का अर्थ भी उतना ही छोटा हो जाता है। हम कभी कहते हैं कि कोई सत् जड़ भी है और कोई चेतन भी। हम और अधिक भेदों की ओर झुक कर फिर यह भी कहते हैं कि जड़ सत् भी अनेक हैं और चेतन सत् भी अनेक हैं । इस तरह जब सर्वग्राही सामान्य को व्यावर्तक भेदों में विभाजित करके देखते हैं तब हमें नाना सत् मालूम होते हैं और वही सद् द्वैत है। इस प्रकार एक विश्व में प्रवृत्त होने वाली सद्-अद्वैत बुद्धि और सद्-द्वैत बुद्धि दोनों अपने-अपने विषय में यथार्थ होकर भी पूर्ण प्रमाण तभी कही जाएँगी जब वे दोनों सापेक्षरूप से मिलें । यही सद्-अद्वैत और सद्-द्वैत वाद जो परस्पर विरुद्ध समझे जाते हैं उनका अनेकान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुआ ।
इसे वृक्ष और वन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब अनेक परस्पर भिन्न वृक्ष व्यक्तियों को उस-उस व्यक्ति रूप से ग्रहण न करके सामूहिक या सामान्य रूप में वनरूप से ग्रहण करते हैं, तब उन सब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता। पर वे सब विशेष सामान्यरूप से सामान्य ग्रहण में ही ऐसे लीन हो जाते हैं मानो वे हैं ही नहीं। एक मात्र वन ही वन नज़र आता है यही एक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org