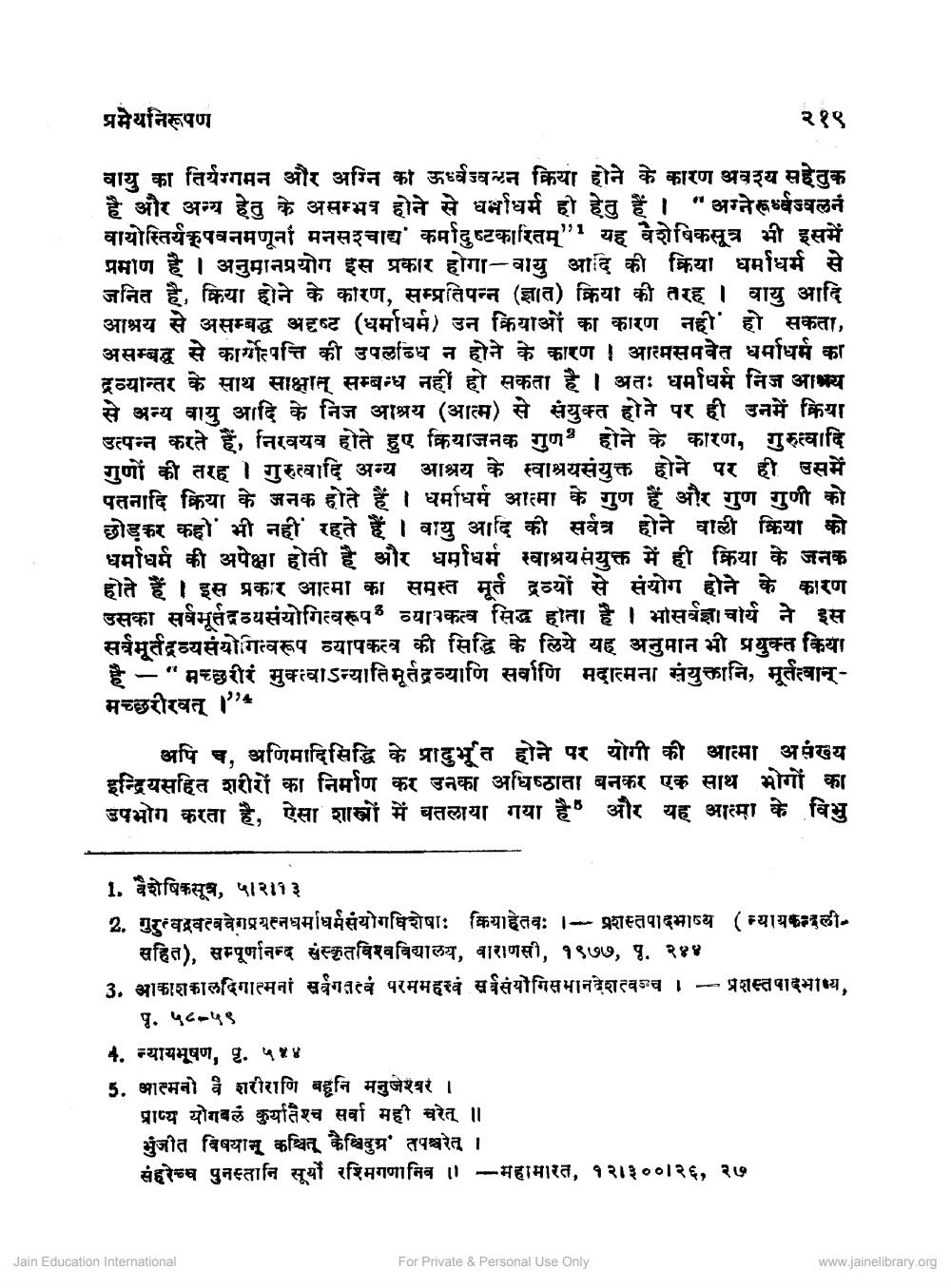________________
प्रमेयनिरूपण
२१९
वायु का तिर्यग्गमन और अग्नि को ऊर्ध्वग्वलन क्रिया होने के कारण अवश्य सहेतुक है और अन्य हेतु के असम्भव होने से ध धर्म हो हेतु हैं । "अग्नेरूज्वलन वायोस्तियपवनमणून मनसश्चाद्य कर्मादुष्टकारितम्"1 यह वैशेषिकसूत्र भी इसमें प्रमाण है । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा-वायु आदि की क्रिया धर्माधर्म से जनित है, किया होने के कारण, सम्प्रतिपन्न (ज्ञात) क्रिया की तरह । वायु आदि आश्रय से असम्बद्ध अदृष्ट (धर्माधर्म) उन क्रियाओं का कारण नहीं हो सकता, असम्बद्ध से कार्गोत्पत्ति की उपलब्धि न होने के कारण । आत्मसमवेत धर्माधर्म का द्रव्यान्तर के साथ साक्षात् सम्बन्ध नहीं हो सकता है। अतः धर्माधर्म निज आश्रय से अन्य वायु आदि के निज आश्रय (आत्म) से संयुक्त होने पर ही उनमें क्रिया उत्पन्न करते हैं, निरवयव होते हुए क्रियाजनक गुण' होने के कारण, गुरुत्वादि गुणों की तरह । गुरुत्वादि अन्य आश्रय के स्वाश्रयसंयुक्त होने पर ही उसमें पतनादि क्रिया के जनक होते हैं । धर्माधर्म आत्मा के गुण हैं और गुण गुणी को छोड़कर कहीं भी नहीं रहते हैं। वायु आदि की सर्वत्र होने वाली क्रिया को धर्माधर्म की अपेक्षा होती है और धर्माधर्म स्वाश्रयसंयुक्त में ही क्रिया के जनक होते हैं । इस प्रकार आत्मा का समस्त मूर्त द्रव्यों से संयोग होने के कारण उसका सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वरूप व्यारकत्व सिद्ध होता है। भोसर्वज्ञाचार्य ने इस सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वरूप व्यापकत्व की सिद्धि के लिये यह अनुमान भी प्रयुक्त किया है - " मच्छरीरं मुक्त्वाऽन्यातिमूर्तद्रव्याणि सर्वाणि मदात्मना संयुक्तानि, मूर्तत्वान्मच्छरीरवत् ।
अपि च, अणिमादिसिद्धि के प्रादुर्भूत होने पर योगी की आत्मा असंख्य इन्द्रियसहित शरीरों का निर्माण कर उनका अधिष्ठाता बनकर एक साथ भोगों का उपभोग करता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है और यह आत्मा के विभु
1. वैशेषिकसूत्र, ५।२।१३ 2. गुरुत्वद्वत्ववेगप्रयत्नधर्माधर्मसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः ।- प्रशस्तपादभाष्य (न्यायकदली.
सहित), सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७७, पृ. २४४ 3. आकाशकालदिगात्मनां सर्वगतत्वं परममहरवं सर्वसंयोगिसमानदेशत्वञ्च । --प्रशस्तपादभाष्य,
पृ. ५८-५९ 4. न्यायभूषण, पृ. ५४४ 5. आत्मनो वै शरीराणि बहुनि मनुजेश्वर ।
प्राप्य योगबलं कुर्यातश्च सर्वा मही चरेत् ॥ भुंजीत विषयान् कश्चित् कैश्चिदुन तपश्चरेत् । संहरेच्च पुनस्तानि सूर्यों रश्मिगणानिव ।। -महामारत, १२।३००।२६, २७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org