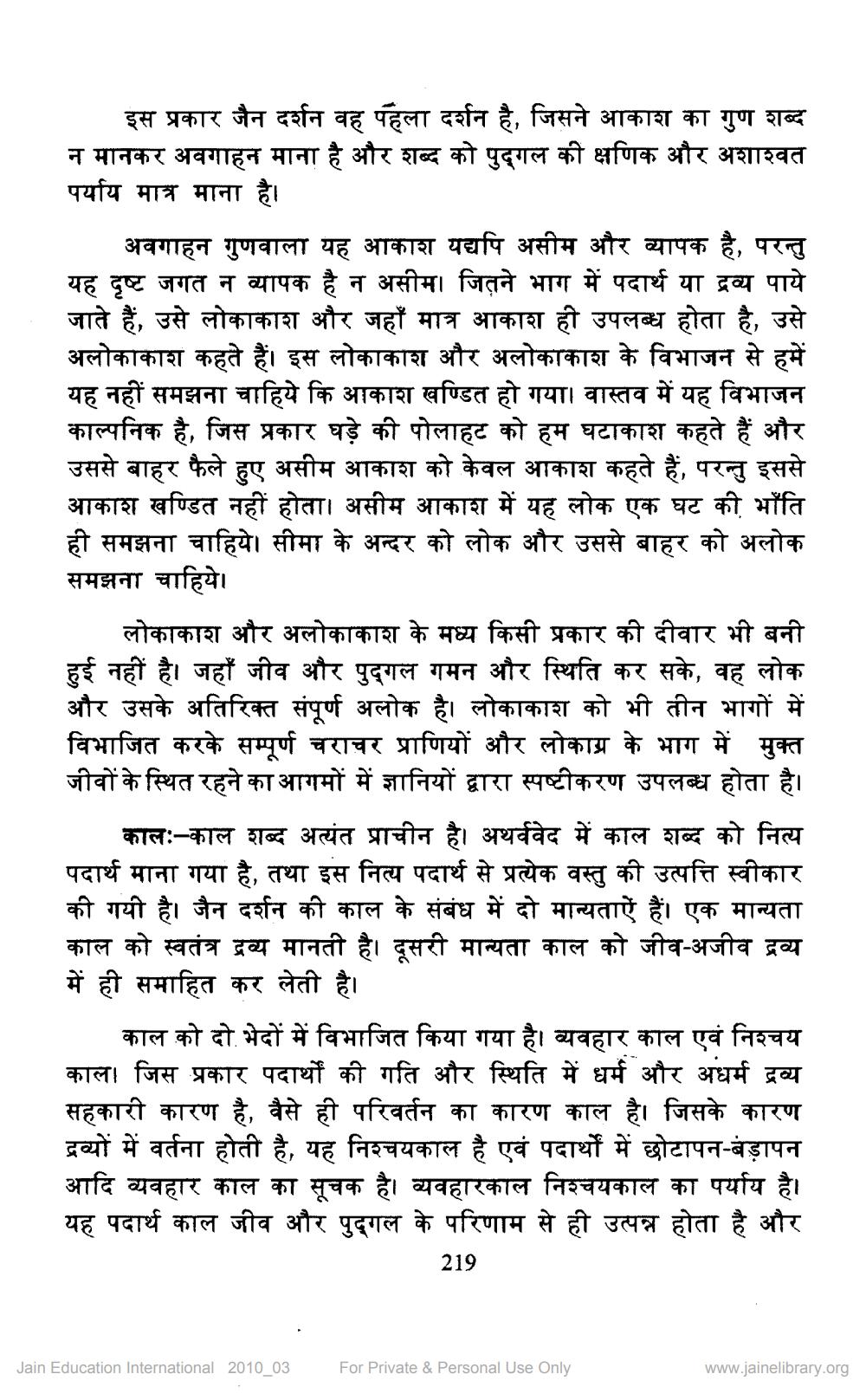________________
इस प्रकार जैन दर्शन वह पहला दर्शन है, जिसने आकाश का गुण शब्द न मानकर अवगाहन माना है और शब्द को पुद्गल की क्षणिक और अशाश्वत पर्याय मात्र माना है।
अवगाहन गुणवाला यह आकाश यद्यपि असीम और व्यापक है, परन्तु यह दृष्ट जगत न व्यापक है न असीम। जितने भाग में पदार्थ या द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोकाकाश और जहाँ मात्र आकाश ही उपलब्ध होता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाजन से हमें यह नहीं समझना चाहिये कि आकाश खण्डित हो गया। वास्तव में यह विभाजन काल्पनिक है, जिस प्रकार घड़े की पोलाहट को हम घटाकाश कहते हैं और उससे बाहर फैले हुए असीम आकाश को केवल आकाश कहते हैं, परन्तु इससे आकाश खण्डित नहीं होता। असीम आकाश में यह लोक एक घट की भाँति ही समझना चाहिये। सीमा के अन्दर को लोक और उससे बाहर को अलोक समझना चाहिये।
लोकाकाश और अलोकाकाश के मध्य किसी प्रकार की दीवार भी बनी हुई नहीं है। जहाँ जीव और पुद्गल गमन और स्थिति कर सके, वह लोक
और उसके अतिरिक्त संपूर्ण अलोक है। लोकाकाश को भी तीन भागों में विभाजित करके सम्पूर्ण चराचर प्राणियों और लोकाग्र के भाग में मुक्त जीवों के स्थित रहने का आगमों में ज्ञानियों द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध होता है।
कालः-काल शब्द अत्यंत प्राचीन है। अथर्ववेद में काल शब्द को नित्य पदार्थ माना गया है, तथा इस नित्य पदार्थ से प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति स्वीकार की गयी है। जैन दर्शन की काल के संबंध में दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता काल को स्वतंत्र द्रव्य मानती है। दूसरी मान्यता काल को जीव-अजीव द्रव्य में ही समाहित कर लेती है।
काल को दो भेदों में विभाजित किया गया है। व्यवहार काल एवं निश्चय काल। जिस प्रकार पदार्थों की गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है, वैसे ही परिवर्तन का कारण काल है। जिसके कारण द्रव्यों में वर्तना होती है, यह निश्चयकाल है एवं पदार्थों में छोटापन-बड़ापन आदि व्यवहार काल का सूचक है। व्यवहारकाल निश्चयकाल का पर्याय है। यह पदार्थ काल जीव और पुद्गल के परिणाम से ही उत्पन्न होता है और
219
___Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org