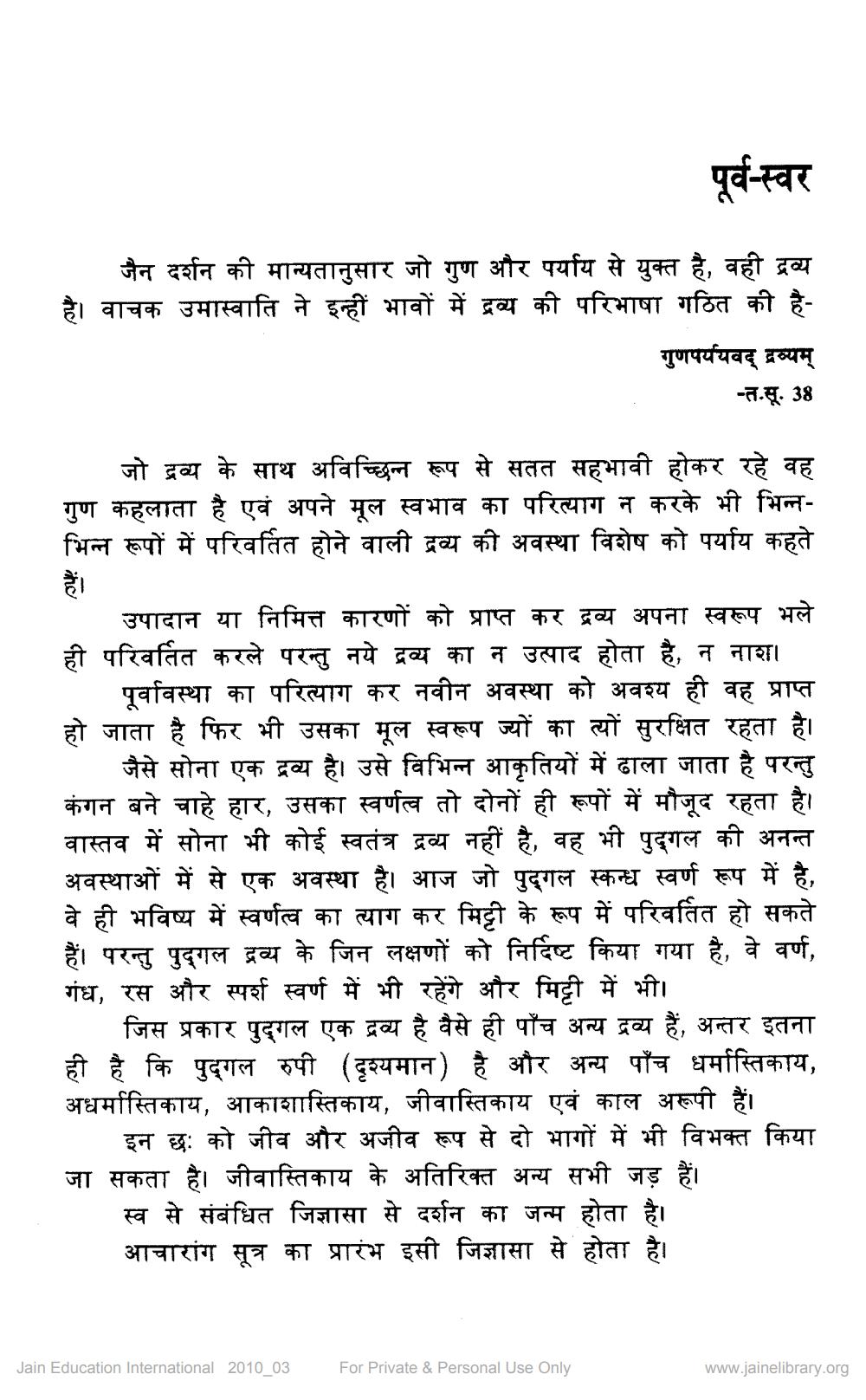________________
पूर्व-स्वर
जैन दर्शन की मान्यतानुसार जो गुण और पर्याय से युक्त है, वही द्रव्य है। वाचक उमास्वाति ने इन्हीं भावों में द्रव्य की परिभाषा गठित की है
गुणपर्ययवद् द्रव्यम्
-त.सू. 38
जो द्रव्य के साथ अविच्छिन्न रूप से सतत सहभावी होकर रहे वह गुण कहलाता है एवं अपने मूल स्वभाव का परित्याग न करके भी भिन्नभिन्न रूपों में परिवर्तित होने वाली द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते
उपादान या निमित्त कारणों को प्राप्त कर द्रव्य अपना स्वरूप भले ही परिवर्तित करले परन्तु नये द्रव्य का न उत्पाद होता है, न नाश।।
पूर्वावस्था का परित्याग कर नवीन अवस्था को अवश्य ही वह प्राप्त हो जाता है फिर भी उसका मूल स्वरूप ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है।
जैसे सोना एक द्रव्य है। उसे विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता है परन्तु कंगन बने चाहे हार, उसका स्वर्णत्व तो दोनों ही रूपों में मौजूद रहता है। वास्तव में सोना भी कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वह भी पुद्गल की अनन्त अवस्थाओं में से एक अवस्था है। आज जो पुद्गल स्कन्ध स्वर्ण रूप में है, वे ही भविष्य में स्वर्णत्व का त्याग कर मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। परन्तु पुद्गल द्रव्य के जिन लक्षणों को निर्दिष्ट किया गया है, वे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श स्वर्ण में भी रहेंगे और मिट्टी में भी।
जिस प्रकार पुद्गल एक द्रव्य है वैसे ही पाँच अन्य द्रव्य हैं, अन्तर इतना ही है कि पुद्गल रुपी (दृश्यमान) है और अन्य पाँच धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय एवं काल अरूपी हैं।
इन छ: को जीव और अजीव रूप से दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। जीवास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य सभी जड़ हैं।
स्व से संबंधित जिज्ञासा से दर्शन का जन्म होता है। आचारांग सूत्र का प्रारंभ इसी जिज्ञासा से होता है।
Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org