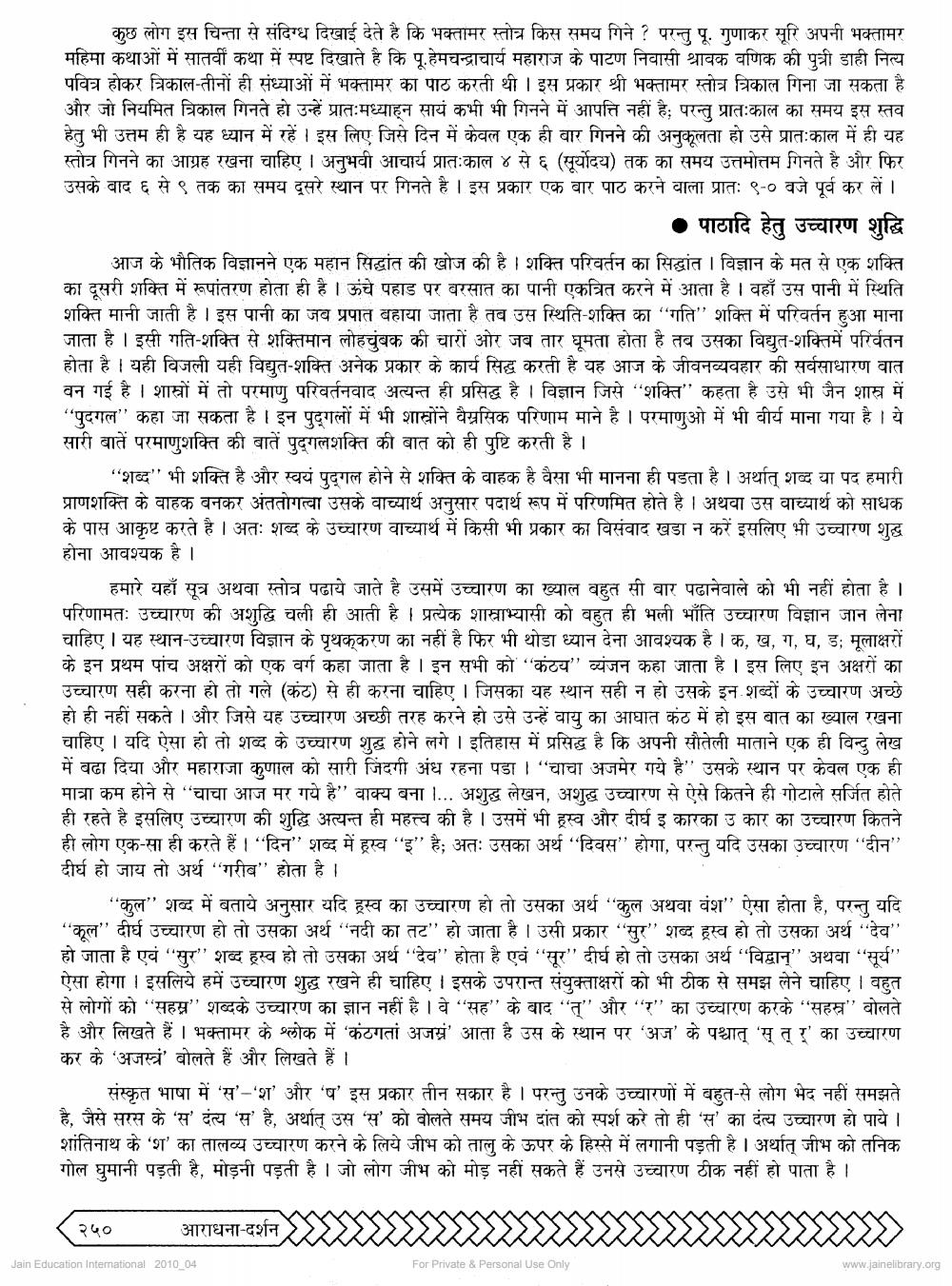________________
कुछ लोग इस चिन्ता से संदिग्ध दिखाई देते है कि भक्तामर स्तोत्र किस समय गिने ? परन्तु पू. गुणाकर सूरि अपनी भक्तामर महिमा कथाओं में साती कथा में स्पष्ट दिखाते है कि पू.हेमचन्द्राचार्य महाराज के पाटण निवासी श्रावक वणिक की पुत्री डाही नित्य पवित्र होकर त्रिकाल-तीनों ही संध्याओं में भक्तामर का पाठ करती थी । इस प्रकार श्री भक्तामर स्तोत्र त्रिकाल गिना जा सकता है
और जो नियमित त्रिकाल गिनते हो उन्हें प्रातःमध्याहन सायं कभी भी गिनने में आपत्ति नहीं है; परन्तु प्रातःकाल का समय इस स्तव हेतु भी उत्तम ही है यह ध्यान में रहें । इस लिए जिसे दिन में केवल एक ही बार गिनने की अनुकूलता हो उसे प्रातःकाल में ही यह स्तोत्र गिनने का आग्रह रखना चाहिए । अनुभवी आचार्य प्रातःकाल ४ से ६ (सूर्योदय) तक का समय उत्तमोत्तम गिनते है और फिर उसके बाद ६ से ९ तक का समय दूसरे स्थान पर गिनते है । इस प्रकार एक बार पाठ करने वाला प्रातः ९-० बजे पूर्व कर लें।
• पाठादि हेतु उच्चारण शुद्धि आज के भौतिक विज्ञानने एक महान सिद्धांत की खोज की है। शक्ति परिवर्तन का सिद्धांत | विज्ञान के मत से एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतरण होता ही है । ऊंचे पहाड पर बरसात का पानी एकत्रित करने में आता है । वहाँ उस पानी में स्थिति शक्ति मानी जाती है । इस पानी का जब प्रपात बहाया जाता है तब उस स्थिति-शक्ति का “गति" शक्ति में परिवर्तन हुआ माना जाता है । इसी गति-शक्ति से शक्तिमान लोहचुंबक की चारों ओर जब तार घूमता होता है तब उसका विद्युत-शक्तिमें परिर्वतन होता है । यही विजली यही विद्युत-शक्ति अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध करती है यह आज के जीवनव्यवहार की सर्वसाधारण वात वन गई है | शास्त्रों में तो परमाणु परिवर्तनवाद अत्यन्त ही प्रसिद्ध है । विज्ञान जिसे “शक्ति" कहता है उसे भी जैन शास्त्र में “पुदगल" कहा जा सकता है। इन पुद्गलों में भी शास्रोंने वैनसिक परिणाम माने है । परमाणुओ में भी वीर्य माना गया है। ये सारी बातें परमाणुशक्ति की बातें पुद्गलशक्ति की बात को ही पुष्टि करती है ।
___ "शब्द" भी शक्ति है और स्वयं पुद्गल होने से शक्ति के वाहक है वैसा भी मानना ही पड़ता है। अर्थात् शब्द या पद हमारी प्राणशक्ति के वाहक बनकर अंततोगत्वा उसके वाच्यार्थ अनुसार पदार्थ रूप में परिणमित होते है । अथवा उस वाच्यार्थ को साधक के पास आकृष्ट करते है | अतः शब्द के उच्चारण वाच्यार्थ में किसी भी प्रकार का विसंवाद खडा न करें इसलिए भी उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है।
हमारे यहाँ सूत्र अथवा स्तोत्र पढाये जाते है उसमें उच्चारण का ख्याल बहुत सी बार पढानेवाले को भी नहीं होता है । परिणामतः उच्चारण की अशुद्धि चली ही आती है । प्रत्येक शास्राभ्यासी को बहुत ही भली भाँति उच्चारण विज्ञान जान लेना चाहिए । यह स्थान-उच्चारण विज्ञान के पृथक्करण का नहीं है फिर भी थोडा ध्यान देना आवश्यक है । क, ख, ग, घ, ड; मूलाक्षरों के इन प्रथम पांच अक्षरों को एक वर्ग कहा जाता है | इन सभी को “कंठय' व्यंजन कहा जाता है । इस लिए इन अक्षरों का उच्चारण सही करना हो तो गले (कंठ) से ही करना चाहिए । जिसका यह स्थान सही न हो उसके इन शब्दों के उच्चारण अच्छे हो ही नहीं सकते । और जिसे यह उच्चारण अच्छी तरह करने हो उसे उन्हें वायु का आघात कंठ में हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए । यदि ऐसा हो तो शब्द के उच्चारण शुद्ध होने लगे । इतिहास में प्रसिद्ध है कि अपनी सौतेली माताने एक ही विन्दु लेख में बढ़ा दिया और महाराजा कुणाल को सारी जिंदगी अंध रहना पडा । "चाचा अजमेर गये है उसके स्थान पर केवल एक ही मात्रा कम होने से “चाचा आज मर गये है" वाक्य बना ।... अशुद्ध लेखन, अशुद्ध उच्चारण से ऐसे कितने ही गोटाले सर्जित होते ही रहते है इसलिए उच्चारण की शुद्धि अत्यन्त ही महत्त्व की है । उसमें भी ह्रस्व और दीर्घ इ कारका उ कार का उच्चारण कितने ही लोग एक-सा ही करते हैं । “दिन" शब्द में ह्रस्व “इ” है; अतः उसका अर्थ “दिवस' होगा, परन्तु यदि उसका उच्चारण “दीन" दीर्घ हो जाय तो अर्थ “गरीब" होता है।
"कुल" शब्द में बताये अनुसार यदि ह्रस्व का उच्चारण हो तो उसका अर्थ “कुल अथवा वंश" ऐसा होता है, परन्तु यदि "कूल' दीर्घ उच्चारण हो तो उसका अर्थ “नदी का तट" हो जाता है । उसी प्रकार “सुर" शब्द ह्रस्व हो तो उसका अर्थ "देव' हो जाता है एवं “सुर" शब्द ह्रस्व हो तो उसका अर्थ "देव' होता है एवं 'सूर' दीर्घ हो तो उसका अर्थ "विद्वान्' अथवा “सूर्य' ऐसा होगा । इसलिये हमें उच्चारण शुद्ध रखने ही चाहिए । इसके उपरान्त संयुक्ताक्षरों को भी ठीक से समझ लेने चाहिए । बहुत से लोगों को “सहन' शब्दके उच्चारण का ज्ञान नहीं है । वे “सह" के बाद “त्" और "र" का उच्चारण करके “सहस्र” बोलते है और लिखते हैं । भक्तामर के श्लोक में 'कंठगतां अजस्रं आता है उस के स्थान पर 'अज' के पश्चात् 'स त् र' का उच्चारण कर के 'अजस्त्रं' बोलते हैं और लिखते हैं।
संस्कृत भाषा में 'स'-'श' और 'ष' इस प्रकार तीन सकार है । परन्तु उनके उच्चारणों में बहुत-से लोग भेद नहीं समझते है, जैसे सरस के 'स' दंत्य ‘स' है, अर्थात् उस 'स' को बोलते समय जीभ दांत को स्पर्श करे तो ही 'स' का दंत्य उच्चारण हो पाये । शांतिनाथ के 'श' का तालव्य उच्चारण करने के लिये जीभ को तालु के ऊपर के हिस्से में लगानी पड़ती है । अर्थात् जीभ को तनिक गोल घुमानी पड़ती है, मोड़नी पड़ती है। जो लोग जीभ को मोड़ नहीं सकते हैं उनसे उच्चारण ठीक नहीं हो पाता है ।
(२५०
२५०
आराधना-दर्शन XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
आराधना-दर्शन
Jain Education International 2010_04
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org