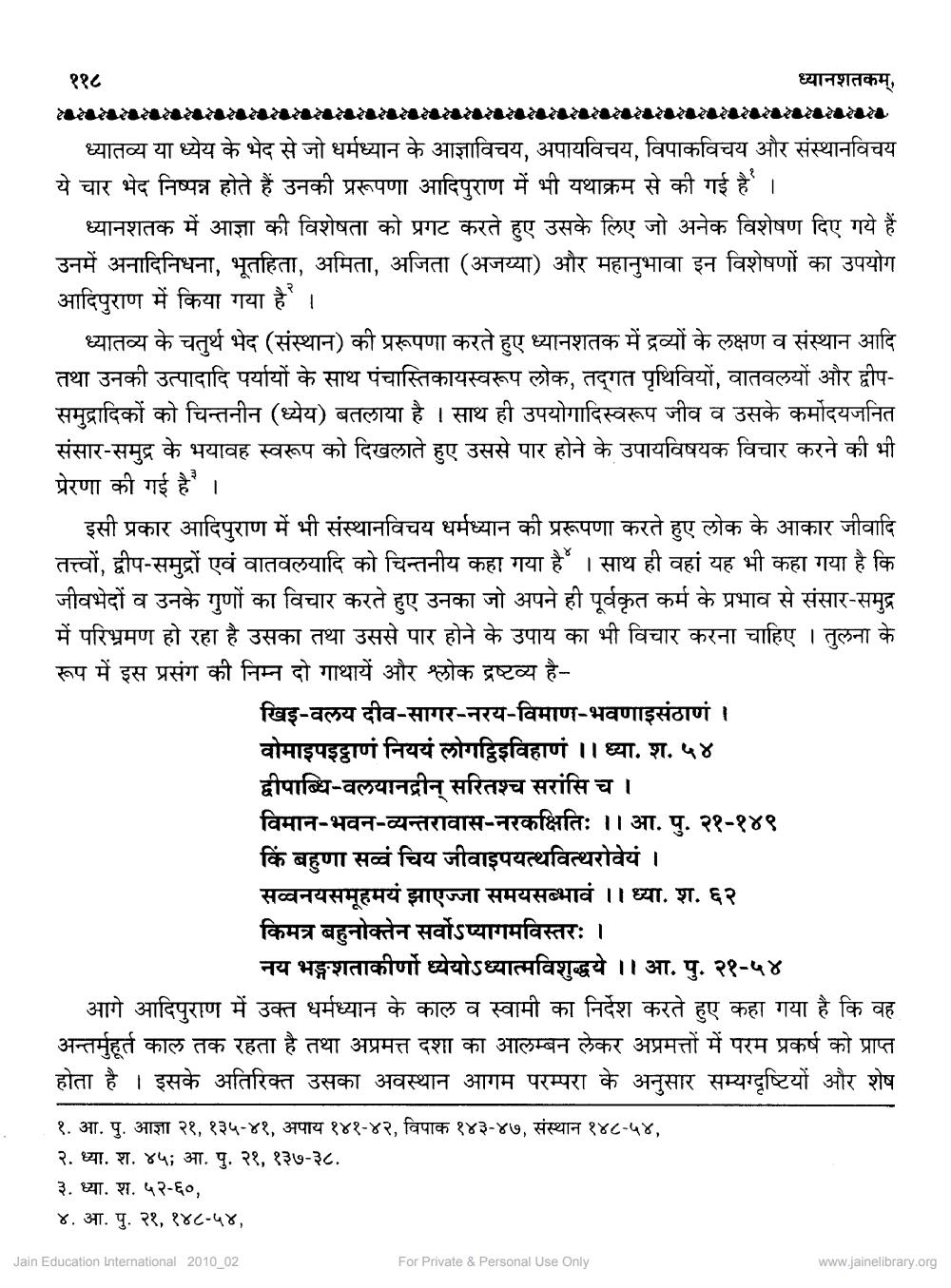________________
११८
ध्यानशतकम्, asaaraaaaaaaantarandaratataaraksharararakarararakaraararararara __ ध्यातव्य या ध्येय के भेद से जो धर्मध्यान के आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय ये चार भेद निष्पन्न होते हैं उनकी प्ररूपणा आदिपुराण में भी यथाक्रम से की गई है ।
ध्यानशतक में आज्ञा की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके लिए जो अनेक विशेषण दिए गये हैं उनमें अनादिनिधना, भूतहिता, अमिता, अजिता (अजय्या) और महानुभावा इन विशेषणों का उपयोग आदिपुराण में किया गया है। ___ ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) की प्ररूपणा करते हुए ध्यानशतक में द्रव्यों के लक्षण व संस्थान आदि तथा उनकी उत्पादादि पर्यायों के साथ पंचास्तिकायस्वरूप लोक, तद्गत पृथिवियों, वातवलयों और द्वीपसमुद्रादिकों को चिन्तनीन (ध्येय) बतलाया है । साथ ही उपयोगादिस्वरूप जीव व उसके कर्मोदयजनित संसार-समुद्र के भयावह स्वरूप को दिखलाते हुए उससे पार होने के उपायविषयक विचार करने की भी प्रेरणा की गई है।
इसी प्रकार आदिपुराण में भी संस्थानविचय धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए लोक के आकार जीवादि तत्त्वों, द्वीप-समुद्रों एवं वातवलयादि को चिन्तनीय कहा गया है । साथ ही वहां यह भी कहा गया है कि जीवभेदों व उनके गुणों का विचार करते हुए उनका जो अपने ही पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से संसार-समुद्र में परिभ्रमण हो रहा है उसका तथा उससे पार होने के उपाय का भी विचार करना चाहिए । तुलना के रूप में इस प्रसंग की निम्न दो गाथायें और श्लोक द्रष्टव्य है
खिइ-वलय दीव-सागर-नरय-विमाण-भवणाइसंठाणं । वोमाइपइट्ठाणं निययं लोगट्टिइविहाणं ।। ध्या. श. ५४ द्वीपाब्धि-वलयानद्रीन् सरितश्च सरांसि च । विमान-भवन-व्यन्तरावास-नरकक्षितिः ।। आ. पु. २१-१४९ किं बहुणा सव्वं चिय जीवाइपयत्थवित्थरोवेयं । सव्वनयसमूहमयं झाएज्जा समयसब्भावं ।। ध्या. श. ६२ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोऽप्यागमविस्तरः ।
नय भङ्गशताकीर्णो ध्येयोऽध्यात्मविशुद्धये ।। आ. पु. २१-५४ आगे आदिपुराण में उक्त धर्मध्यान के काल व स्वामी का निर्देश करते हुए कहा गया है कि वह अन्तर्मुहूर्त काल तक रहता है तथा अप्रमत्त दशा का आलम्बन लेकर अप्रमत्तों में परम प्रकर्ष को प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त उसका अवस्थान आगम परम्परा के अनुसार सम्यग्दृष्टियों और शेष
१. आ. पु. आज्ञा २१, १३५-४१, अपाय १४१-४२, विपाक १४३-४७, संस्थान १४८-५४, २. ध्या. श. ४५; आ. पु. २१, १३७-३८. ३. ध्या. श. ५२-६०, ४. आ. पु. २१, १४८-५४,
Jain Education International 2010_02
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org