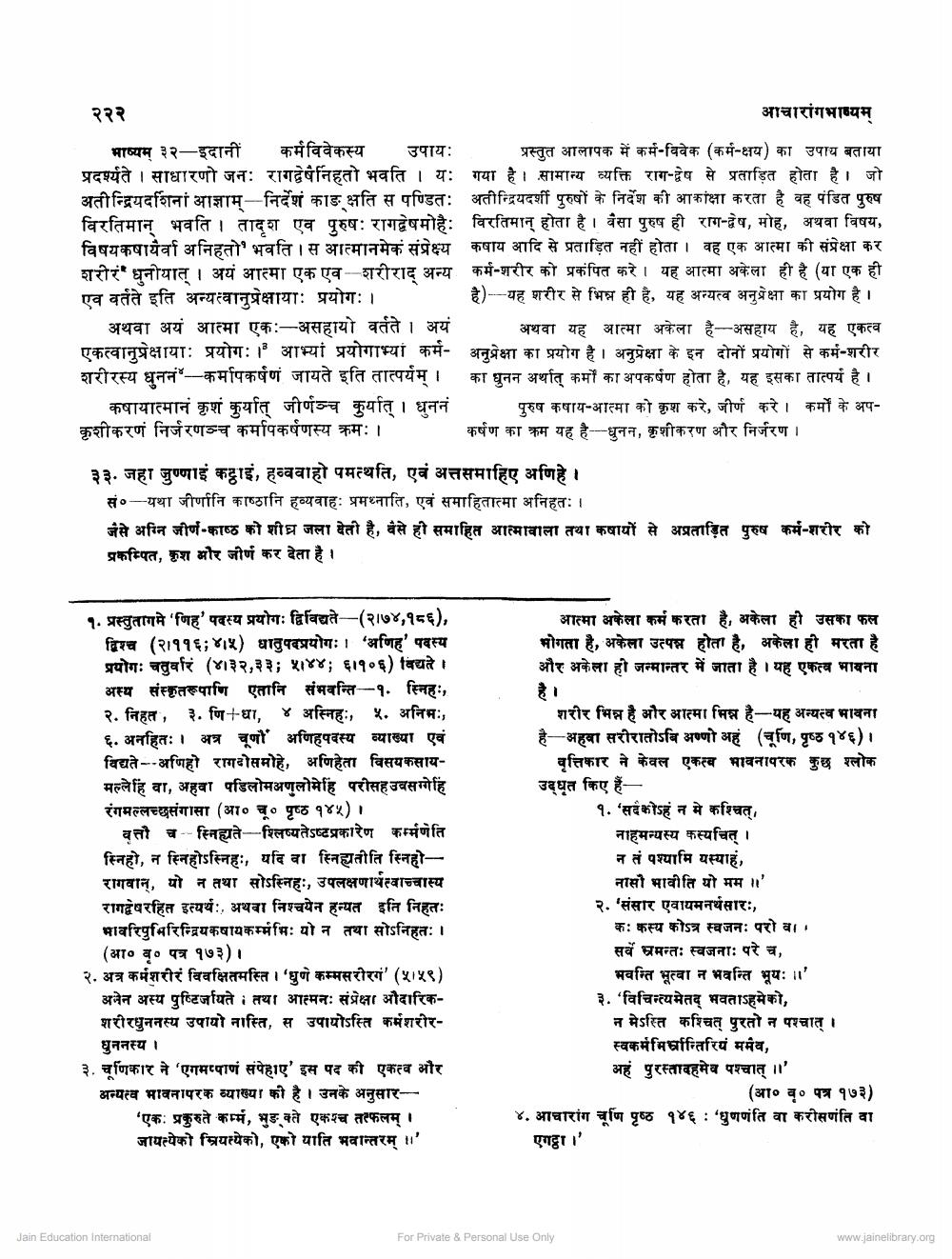________________
२२२
आचारांगभाष्यम्
भाष्यम् ३२–इदानीं कर्मविवेकस्य उपायः प्रस्तुत आलापक में कर्म-विवेक (कर्म-क्षय) का उपाय बताया प्रदर्श्यते । साधारणो जनः रागद्वेषैनिहतो भवति । यः गया है। सामान्य व्यक्ति राग-द्वेष से प्रताड़ित होता है। जो अतीन्द्रियदर्शिनां आज्ञाम्-निर्देश काङ क्षति स पण्डितः अतीन्द्रियदर्शी पुरुषों के निर्देश की आकांक्षा करता है बह पंडित पुरुष विरतिमान् भवति । तादृश एव पुरुष: रागद्वेषमोहै: विरतिमान् होता है। वैसा पुरुष ही राग-द्वेष, मोह, अथवा विषय, विषयकषायैर्वा अनिहतो' भवति । स आत्मानमेकं संप्रेक्ष्य कषाय आदि से प्रताड़ित नहीं होता। वह एक आत्मा की संप्रेक्षा कर शरीरं धुनीयात् । अयं आत्मा एक एव-शरीराद् अन्य कर्म-शरीर को प्रकंपित करे। यह आत्मा अकेला ही है (या एक ही एव वर्तते इति अन्यत्वानुप्रेक्षायाः प्रयोगः ।
है)----यह शरीर से भिन्न ही है, यह अन्यत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग है । अथवा अयं आत्मा एक:-असहायो वर्तते । अयं अथवा यह आत्मा अकेला है-असहाय है, यह एकत्व एकत्वानुप्रेक्षायाः प्रयोगः। आभ्यां प्रयोगाभ्यां कर्म- अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। अनुप्रेक्षा के इन दोनों प्रयोगों से कर्म-शरीर शरीरस्य धुनन-कर्मापकर्षणं जायते इति तात्पर्यम् । का धुनन अर्थात् कर्मों का अपकर्षण होता है, यह इसका तात्पर्य है ।
कषायात्मानं कृशं कुर्यात् जीर्णञ्च कुर्यात् । धुननं पुरुष कषाय-आत्मा को कृश करे, जीर्ण करे। कर्मों के अपकृशीकरणं निर्जरणञ्च कर्मापकर्षणस्य क्रमः । कर्षण का क्रम यह है-धुनन, कृशीकरण और निर्जरण ।
३३. जहा जुण्णाई कटाई, हव्ववाहो पमत्थति, एवं अत्तसमाहिए अणिहे। सं०-यथा जीर्णानि काष्ठानि हव्यवाहः प्रमथ्नाति, एवं समाहितात्मा अनिहतः । जैसे अग्नि जीर्ण-काष्ठ को शीघ्र जला देती है, वैसे ही समाहित आत्मावाला तथा कषायों से अप्रताड़ित पुरुष कर्म-शरीर को प्रकम्पित, कृश और जीर्ण कर देता है ।
आत्मा अकेला कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही जन्मान्तर में जाता है । यह एकत्व भावना
१. प्रस्तुतागमे 'णिह' पदस्य प्रयोगः द्विविद्यते-(२।७४,१८६), द्विश्च (२।११६४१५) धातुपदप्रयोगः। 'अणिह' पवस्य प्रयोगः चतुरिं (४।३२,३३, १४४६१०६) विद्यते । अस्य संस्कृतरूपाणि एतानि संभवन्ति-१. स्निहः, २. निहत, ३. णि+धा, ४ अस्निहः, ५. अनिमः, ६. अनहितः। अत्र चूणो अणिहपवस्य व्याख्या एवं विद्यते--अणिहो रागदोसमोहे, अणिहेता विसयकसायमल्लेहिं वा, अहवा पडिलोमअणुलोमेहि परीसह उवसग्गेहि रंगमल्लच्छसंगासा (आ० चू० पृष्ठ १४५)।
वृत्तौ च --स्निह्यते-श्लिष्यतेऽष्टप्रकारेण कर्मणेति स्निहो, न स्निहोऽस्निहः, यदि वा स्निह्यतीति स्निहोरागवान्, यो न तथा सोऽस्निहः, उपलक्षणार्थत्वाच्चास्य रागद्वेषरहित इत्यर्थः, अथवा निश्चयेन हन्यत इति निहतः भावरिपुभिरिन्द्रियकषायकर्मभिः यो न तथा सोऽनिहतः । (आ० वृ० पत्र १७३)। २. अत्र कर्मशरीरं विवक्षितमस्ति । 'धुणे कम्मसरीरगं' (५।५९)
अनेन अस्य पुष्टिर्जायते । तथा आत्मनः संप्रेक्षा औदारिकशरीरधुननस्य उपायो नास्ति, स उपायोऽस्ति कर्मशरीर
धुननस्य। ३. चूणिकार ने 'एगमप्पाणं संपेहाए' इस पद की एकत्व और अन्यत्व भावनापरक व्याख्या की है। उनके अनुसार
'एकः प्रकुरुते कर्म, भुङ्क्ते एकश्च तत्फलम् । जायत्येको म्रियत्येको, एको याति भवान्तरम् ॥'
शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है-यह अन्यत्व भावना है—अहवा सरीरातोऽबि अण्णो अहं (चूणि, पृष्ठ १४६)।
वृत्तिकार ने केवल एकत्व भावनापरक कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं
१. 'सदकोऽहं न मे कश्चित्, नाहमन्यस्य कस्यचित् । न तं पश्यामि यस्याहं, नासौ भावीति यो मम ॥' २. 'संसार एवायमनर्थसारः,
कः कस्य कोऽत्र स्वजनः परो वा । सर्वे भ्रमन्तः स्वजनाः परे च,
भवन्ति भूत्वा न भवन्ति भूयः ।।' ३. 'विचिन्त्यमेतद् भवताऽहमेको,
न मेऽस्ति कश्चित् पुरतो न पश्चात् । स्वकर्ममिर्धान्तिरियं ममैव, अहं पुरस्तावहमेव पश्चात् ॥'
(आ० वृ० पत्र १७३) ४. आचारांग चूणि पृष्ठ १४६ : 'धुणणंति वा करीसणंति वा एगट्ठा।
Jain Education international
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org