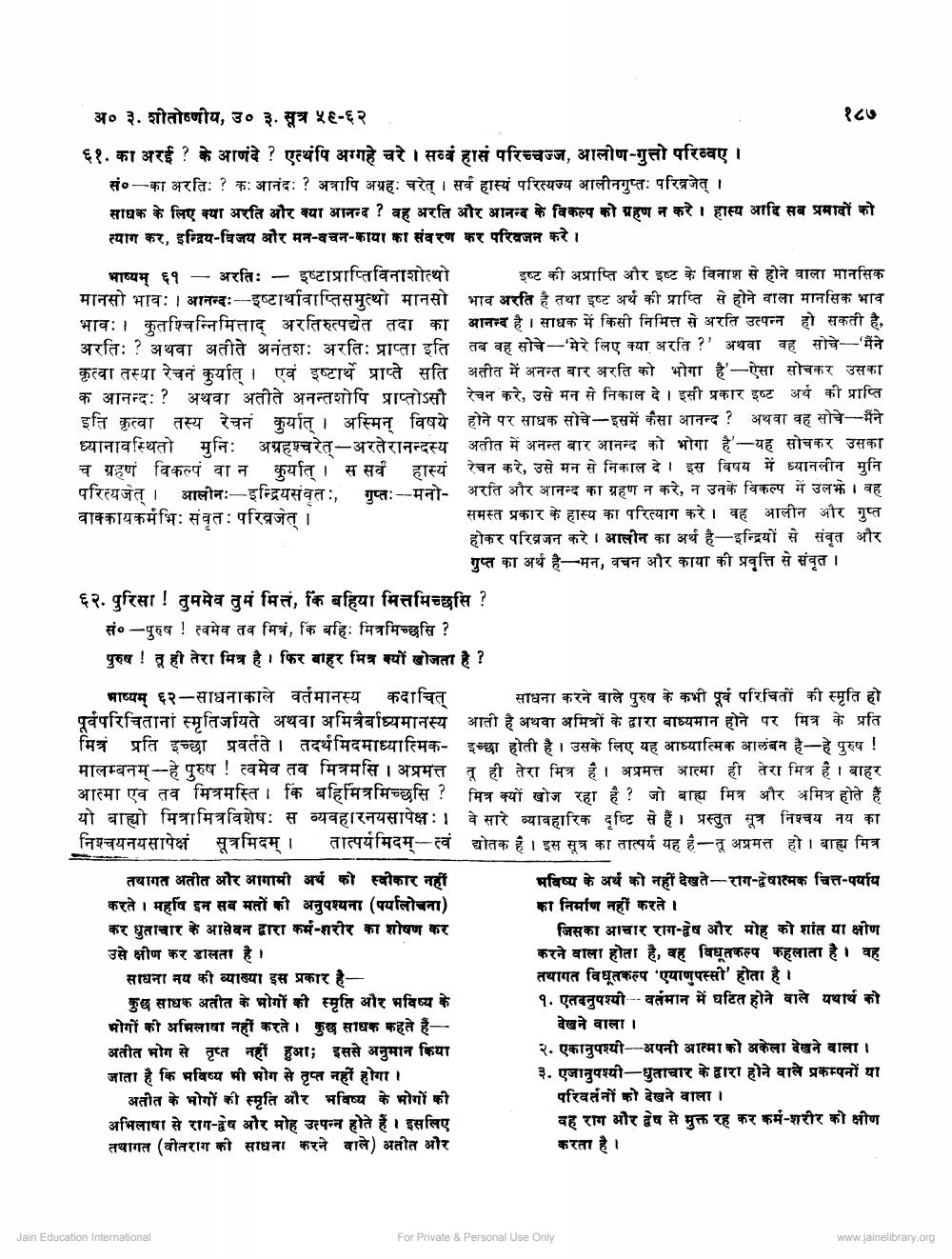________________
अ० ३. शीतोष्णीय, उ०३. सूत्र ५६-६२ ..
१८७ ६१. का अरई ? के आणंदे ? एत्थंपि अग्गहे चरे । सव्वं हासं परिच्चज्ज, आलोण-गुत्तो परिव्वए ।
सं०-का अरतिः ? कः आनंदः ? अत्रापि अग्रहः चरेत् । सर्व हास्यं परित्यज्य आलीनगुप्तः परिव्रजेत् । साधक के लिए क्या अरति और क्या आनन्द ? वह अरति और आनन्द के विकल्प को ग्रहण न करे । हास्य आदि सब प्रमावों को त्याग कर, इन्द्रिय-विजय और मन-वचन-काया का संवरण कर परिवजन करे।
भाष्यम् ६१ - अरतिः - इष्टाप्राप्तिविनाशोत्थो इष्ट की अप्राप्ति और इष्ट के विनाश से होने वाला मानसिक मानसो भावः । आनन्दः--इष्टार्थावाप्तिसमुत्थो मानसो भाव अरति है तथा इष्ट अर्थ की प्राप्ति से होने वाला मानसिक भाव भावः। कुतश्चिन्निमित्ताद् अरतिरुत्पद्येत तदा का आनन्द है । साधक में किसी निमित्त से अरति उत्पन्न हो सकती है, अरतिः ? अथवा अतीते अनंतश: अरतिः प्राप्ता इति तब वह सोचे-'मेरे लिए क्या अरति ?' अथवा वह सोचे-'मैंने कृत्वा तस्या रेचनं कुर्यात् । एवं इष्टार्थे प्राप्ते सति अतीत में अनन्त बार अरति को भोगा है'-ऐसा सोचकर उसका क आनन्दः? अथवा अतीते अनन्तशोपि प्राप्तोऽसौ रेचन करे, उसे मन से निकाल दे। इसी प्रकार इष्ट अर्थ की प्राप्ति इति कृत्वा तस्य रेचनं कुर्यात् । अस्मिन विषये होने पर साधक सोचे-इसमें कैसा आनन्द ? अथवा वह सोचे-मैंने ध्यानावस्थितो मुनिः अग्रहश्चरेत्-अरतेरानन्दस्य अतीत में अनन्त बार आनन्द को भोगा है-यह सोचकर उसका च ग्रहणं विकल्पं वा न कुर्यात् । स सर्व हास्यं रेचन करे, उसे मन से निकाल दे। इस विषय में ध्यानलीन मुनि परित्यजेत् । आलीन:-इन्द्रियसंवतः, गुप्तः--मनो- अरति और आनन्द का ग्रहण न करे, न उनके विकल्प में उलझे । वह वाक्कायकर्मभिः संवृतः परिव्रजेत् ।
समस्त प्रकार के हास्य का परित्याग करे। वह आलीन और गुप्त होकर परिव्रजन करे । आलीन का अर्थ है-इन्द्रियों से संवृत और
गुप्त का अर्थ है-मन, वचन और काया की प्रवृत्ति से संवृत । ६२. पुरिसा! तुममेव तुम मित्तं, कि बहिया मित्तमिच्छसि ?
सं०-पुरुष ! त्वमेव तव मित्रं, कि बहिः मित्रमिच्छसि ? पुरुष ! तू ही तेरा मित्र है। फिर बाहर मित्र क्यों खोजता है ?
भाष्यम् ६२-साधनाकाले वर्तमानस्य कदाचित् साधना करने वाले पुरुष के कभी पूर्व परिचितों की स्मृति हो पूर्वपरिचितानां स्मृतिर्जायते अथवा अमित्रैर्बाध्यमानस्य आती है अथवा अमित्रों के द्वारा बाध्यमान होने पर मित्र के प्रति मित्र प्रति इच्छा प्रवर्तते । तदर्थमिदमाध्यात्मिक- इच्छा होती है। उसके लिए यह आध्यात्मिक आलंबन है-हे पुरुष ! मालम्बनम-हे पूरुष ! त्वमेव तव मित्रमसि । अप्रमत्त तू ही तेरा मित्र है। अप्रमत्त आत्मा ही तेरा मित्र है । बाहर आत्मा एव तव मित्रमस्ति । कि बहिमित्रमिच्छसि ? मित्र क्यों खोज रहा है? जो बाह्य मित्र और अमित्र होते हैं यो बाह्यो मित्रामित्रविशेषः स व्यवहारनयसापेक्षः। वे सारे व्यावहारिक दृष्टि से हैं। प्रस्तुत सूत्र निश्चय नय का निश्चयनयसापेक्षं सूत्रमिदम् । तात्पर्यमिदम्-त्वं द्योतक है। इस सूत्र का तात्पर्य यह है-तू अप्रमत्त हो । बाह्य मित्र तथागत अतीत और आगामी अर्थ को स्वीकार नहीं
भविष्य के अर्थ को नहीं देखते-राग-द्वेषात्मक चित्त-पर्याय करते । महर्षि इन सब मतों की अनुपश्यना (पर्यालोचना)
का निर्माण नहीं करते। कर धुताचार के आसेवन द्वारा कर्म-शरीर का शोषण कर
जिसका आचार राग-द्वेष और मोह को शांत या क्षीण उसे क्षीण कर डालता है।
करने वाला होता है, वह विधूतकल्प कहलाता है। वह साधना नय की व्याख्या इस प्रकार है
तथागत विधूतकल्प 'एयाणुपस्सी' होता है। कुछ साधक अतीत के भोगों को स्मृति और भविष्य के
१. एतदनुपश्यी-- वर्तमान में घटित होने वाले यथार्थ को भोगों की अभिलाषा नहीं करते। कुछ साधक कहते हैं
देखने वाला। अतीत भोग से तृप्त नहीं हुआ, इससे अनुमान किया
२. एकानुपश्यी-अपनी आत्मा को अकेला देखने वाला। जाता है कि भविष्य भी भोग से तृप्त नहीं होगा।
३. एजानुपश्यी-धुताचार के द्वारा होने वाले प्रकम्पनों या __ अतीत के भोगों की स्मृति और भविष्य के भोगों की
परिवर्तनों को देखने वाला। अभिलाषा से राग-द्वेष और मोह उत्पन्न होते हैं । इसलिए
वह राग और द्वेष से मुक्त रह कर कर्म-शरीर को क्षीण तथागत (वीतराग की साधना करने वाले) अतीत और
करता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org