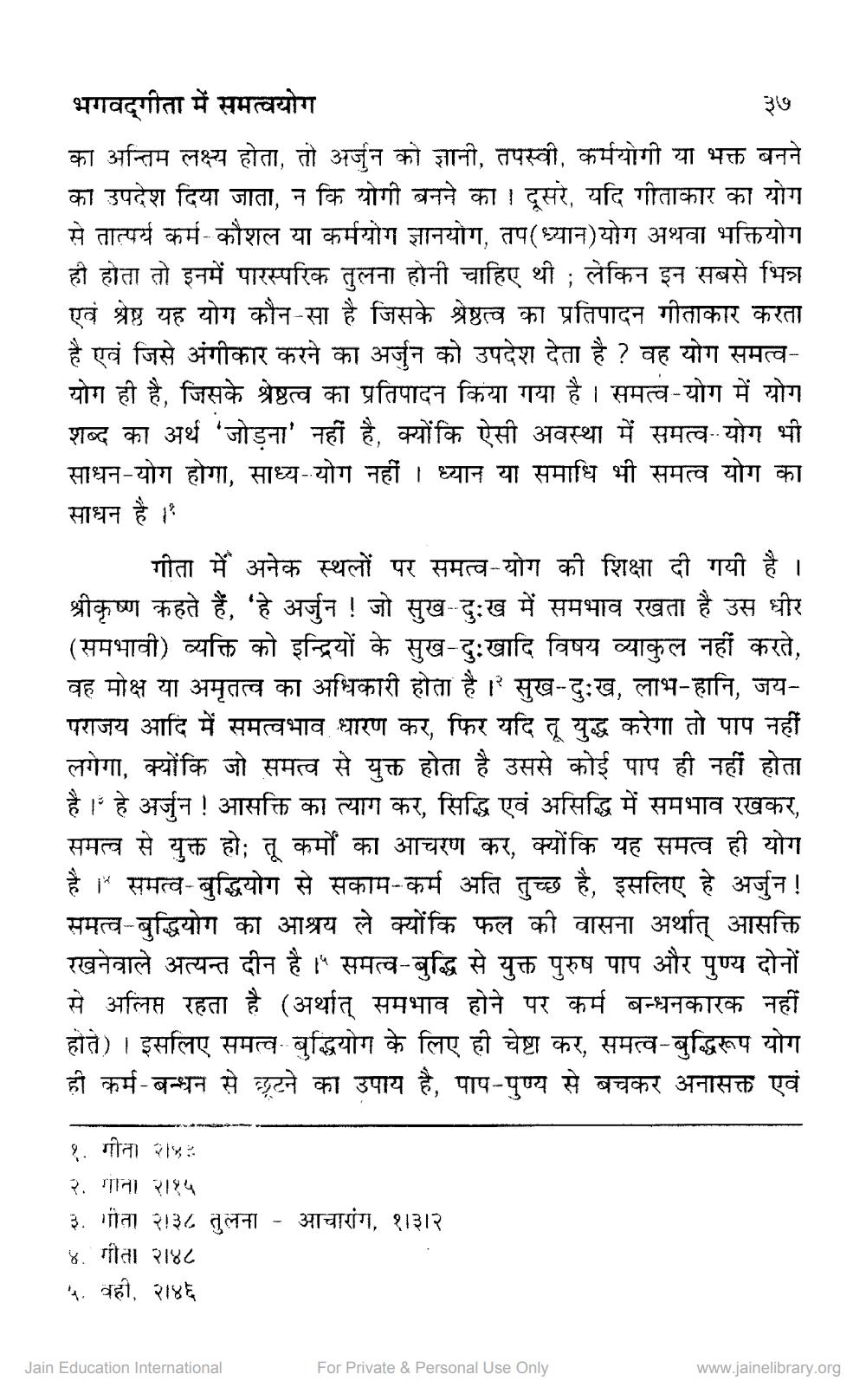________________
भगवद्गीता में समत्वयोग
३७
का अन्तिम लक्ष्य होता, तो अर्जुन को ज्ञानी, तपस्वी, कर्मयोगी या भक्त बनने का उपदेश दिया जाता, न कि योगी बनने का। दूसरे, यदि गीताकार का योग से तात्पर्य कर्म- कौशल या कर्मयोग ज्ञानयोग, तप ( ध्यान ) योग अथवा भक्तियोग ही होता तो इनमें पारस्परिक तुलना होनी चाहिए थी; लेकिन इन सबसे भिन्न एवं श्रेष्ठ यह योग कौन-सा है जिसके श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन गीताकार करता है एवं जिसे अंगीकार करने का अर्जुन को उपदेश देता है ? वह योग समत्वयोग ही है, जिसके श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया गया है । समत्व - योग में योग शब्द का अर्थ 'जोड़ना' नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में समत्व- योग भी साधन - योग होगा, साध्य - योग नहीं । ध्यान या समाधि भी समत्व योग का साधन हैं ।
गीता में अनेक स्थलों पर समत्व-योग की शिक्षा दी गयी है । श्रीकृष्ण कहते हैं, 'हे अर्जुन ! जो सुख - दुःख में समभाव रखता है उस धीर (समभावी) व्यक्ति को इन्द्रियों के सुख - दुःखादि विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष या अमृतत्व का अधिकारी होता है। सुख-दुःख, लाभ-हानि, जयपराजय आदि में समत्वभाव धारण कर, फिर यदि तू युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो समत्व से युक्त होता है उससे कोई पाप ही नहीं होता है। हे अर्जुन ! आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव रखकर, समत्व से युक्त हो; तू कर्मों का आचरण कर, क्योंकि यह समत्व ही योग है । समत्व - बुद्धियोग से सकाम कर्म अति तुच्छ है, इसलिए हे अर्जुन ! समत्व - बुद्धियोग का आश्रय ले क्योंकि फल की वासना अर्थात् आसक्ति रखनेवाले अत्यन्त दीन है । समत्व - बुद्धि से युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है (अर्थात् समभाव होने पर कर्म बन्धनकारक नहीं होते) । इसलिए समत्व - बुद्धियोग के लिए ही चेष्टा कर, समत्व - बुद्धिरूप योग ही कर्म - बन्धन से छूटने का उपाय है, पाप-पुण्य से बचकर अनासक्त एवं
१. गीता २२४३
२. गाना २११५
३. गीता २२३८ तुलना
४. गीता २२४८
५. वही, २०४६
Jain Education International
आचारांग, १३३|२
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org