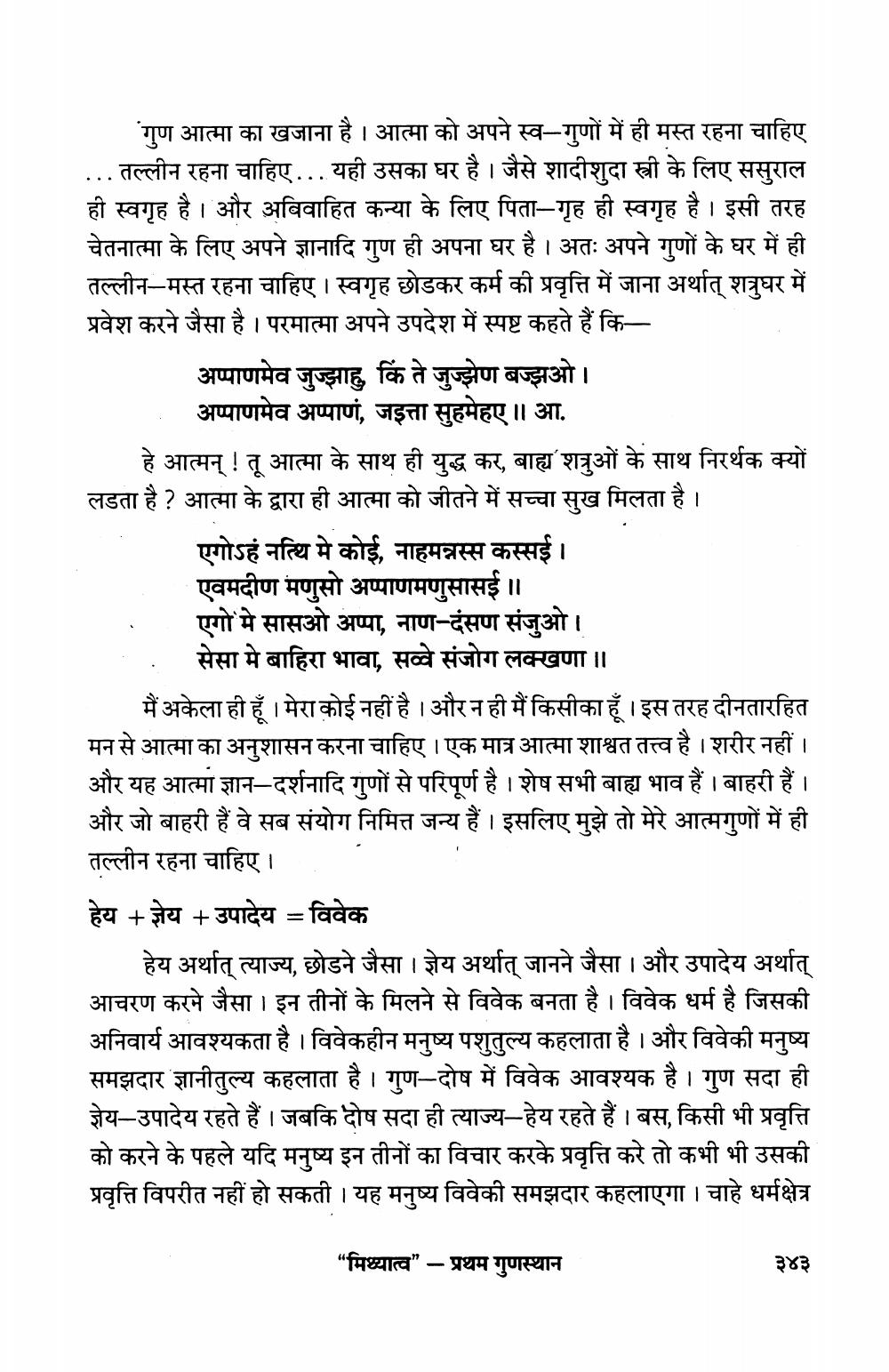________________
गुण आत्मा का खजाना है । आत्मा को अपने स्व-गुणों में ही मस्त रहना चाहिए ... तल्लीन रहना चाहिए... यही उसका घर है । जैसे शादीशुदा स्त्री के लिए ससुराल ही स्वगृह है । और अविवाहित कन्या के लिए पिता-गृह ही स्वगृह है । इसी तरह चेतनात्मा के लिए अपने ज्ञानादि गुण ही अपना घर है । अतः अपने गुणों के घर में ही तल्लीन-मस्त रहना चाहिए। स्वगृह छोडकर कर्म की प्रवृत्ति में जाना अर्थात् शत्रुघर में प्रवेश करने जैसा है । परमात्मा अपने उपदेश में स्पष्ट कहते हैं कि
अप्पाणमेव जुज्झाहु किं ते जुज्झेण बज्झओ।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ।। आ. हे आत्मन् ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाह्य शत्रुओं के साथ निरर्थक क्यों लडता है ? आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जीतने में सच्चा सुख मिलता है ।
एगोऽहं नत्थि मे कोई, नाहमन्नस्स कस्सई। एवमदीण मणुसो अप्पाणमणुसासई॥ एगों मे सासओ अप्पा, नाण-दंसण संजुओ।
सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्खणा ।। मैं अकेला ही हूँ । मेरा कोई नहीं है । और न ही मैं किसीका हूँ । इस तरह दीनतारहित मन से आत्मा का अनुशासन करना चाहिए । एक मात्र आत्मा शाश्वत तत्त्व है । शरीर नहीं । और यह आत्मा ज्ञान–दर्शनादि गुणों से परिपूर्ण है। शेष सभी बाह्य भाव हैं । बाहरी हैं। और जो बाहरी हैं वे सब संयोग निमित्त जन्य हैं । इसलिए मुझे तो मेरे आत्मगुणों में ही तल्लीन रहना चाहिए। हेय + ज्ञेय + उपादेय = विवेक
हेय अर्थात् त्याज्य, छोडने जैसा । ज्ञेय अर्थात् जानने जैसा । और उपादेय अर्थात् आचरण करने जैसा । इन तीनों के मिलने से विवेक बनता है । विवेक धर्म है जिसकी अनिवार्य आवश्यकता है । विवेकहीन मनुष्य पशुतुल्य कहलाता है । और विवेकी मनुष्य समझदार ज्ञानीतुल्य कहलाता है। गुण-दोष में विवेक आवश्यक है। गुण सदा ही ज्ञेय-उपादेय रहते हैं । जबकि दोष सदा ही त्याज्य हेय रहते हैं । बस, किसी भी प्रवृत्ति को करने के पहले यदि मनुष्य इन तीनों का विचार करके प्रवृत्ति करे तो कभी भी उसकी प्रवृत्ति विपरीत नहीं हो सकती । यह मनुष्य विवेकी समझदार कहलाएगा । चाहे धर्मक्षेत्र
"मिथ्यात्व" - प्रथम गुणस्थान
३४३