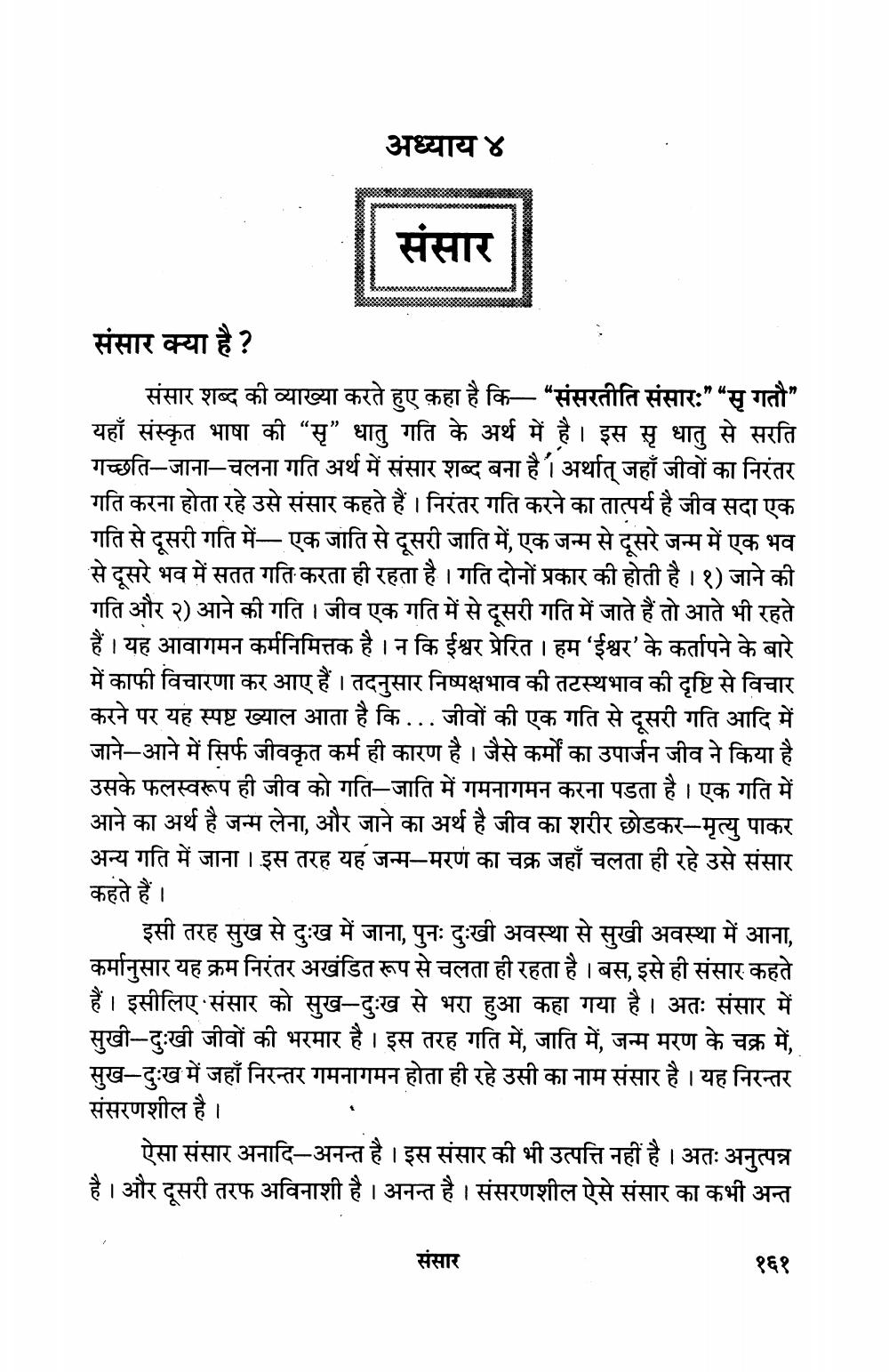________________
अध्याय ४
संसार
388888888888999088E
संसार क्या है?
संसार शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि- "संसरतीति संसारः" "स गतौ" यहाँ संस्कृत भाषा की “सृ" धातु गति के अर्थ में है। इस सृ धातु से सरति गच्छति–जाना-चलना गति अर्थ में संसार शब्द बना है । अर्थात् जहाँ जीवों का निरंतर गति करना होता रहे उसे संसार कहते हैं । निरंतर गति करने का तात्पर्य है जीव सदा एक गति से दूसरी गति में— एक जाति से दूसरी जाति में, एक जन्म से दूसरे जन्म में एक भव से दूसरे भव में सतत गति करता ही रहता है । गति दोनों प्रकार की होती है। १) जाने की गति और २) आने की गति । जीव एक गति में से दूसरी गति में जाते हैं तो आते भी रहते हैं। यह आवागमन कर्मनिमित्तक है । न कि ईश्वर प्रेरित । हम 'ईश्वर' के कर्तापने के बारे में काफी विचारणा कर आए हैं । तदनुसार निष्पक्षभाव की तटस्थभाव की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट ख्याल आता है कि... जीवों की एक गति से दूसरी गति आदि में जाने-आने में सिर्फ जीवकृत कर्म ही कारण है । जैसे कर्मों का उपार्जन जीव ने किया है उसके फलस्वरूप ही जीव को गति–जाति में गमनागमन करना पडता है। एक गति में आने का अर्थ है जन्म लेना, और जाने का अर्थ है जीव का शरीर छोडकर-मृत्यु पाकर अन्य गति में जाना । इस तरह यह जन्म-मरण का चक्र जहाँ चलता ही रहे उसे संसार कहते हैं।
इसी तरह सुख से दुःख में जाना, पुनः दुःखी अवस्था से सुखी अवस्था में आना, कर्मानुसार यह क्रम निरंतर अखंडित रूप से चलता ही रहता है । बस, इसे ही संसार कहते हैं। इसीलिए संसार को सुख-दुःख से भरा हुआ कहा गया है। अतः संसार में सुखी-दुःखी जीवों की भरमार है। इस तरह गति में, जाति में, जन्म मरण के चक्र में, सुख-दुःख में जहाँ निरन्तर गमनागमन होता ही रहे उसी का नाम संसार है । यह निरन्तर संसरणशील है।
ऐसा संसार अनादि-अनन्त है। इस संसार की भी उत्पत्ति नहीं है । अतः अनुत्पन्न है। और दूसरी तरफ अविनाशी है । अनन्त है । संसरणशील ऐसे संसार का कभी अन्त
संसार
१६१