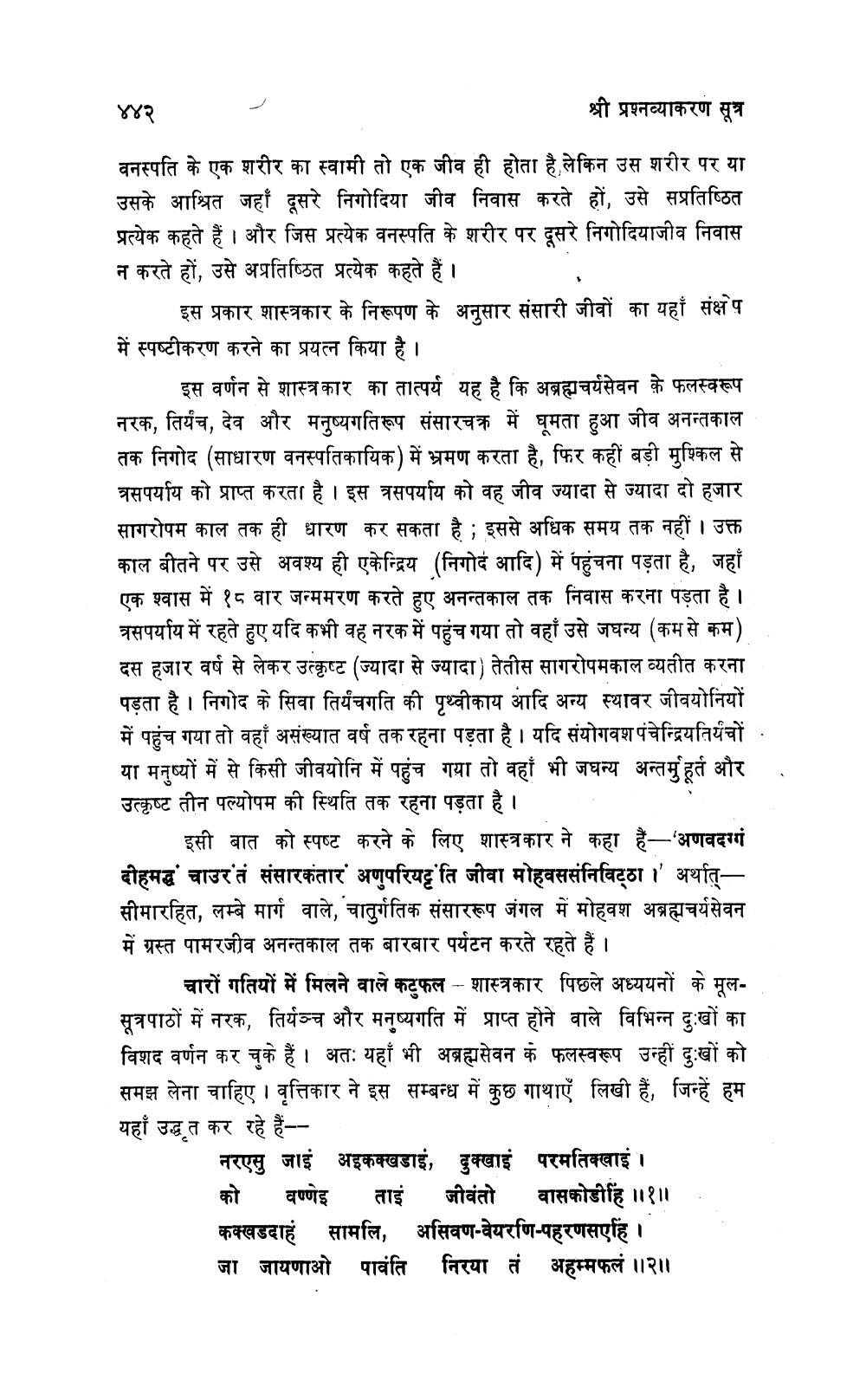________________
४४२
-
श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र
वनस्पति के एक शरीर का स्वामी तो एक जीव ही होता है, लेकिन उस शरीर पर या उसके आश्रित जहाँ दूसरे निगोदिया जीव निवास करते हों, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । और जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर पर दूसरे निगोदियाजीव निवास न करते हों, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ।
इस प्रकार शास्त्रकार के निरूपण के अनुसार संसारी जीवों का यहाँ संक्षेप में स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है।
इस वर्णन से शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि अब्रह्मचर्यसेवन के फलस्वरूप नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्यगतिरूप संसारचक्र में घूमता हुआ जीव अनन्तकाल तक निगोद (साधारण वनस्पतिकायिक) में भ्रमण करता है, फिर कहीं बड़ी मुश्किल से त्रसपर्याय को प्राप्त करता है । इस त्रसपर्याय को वह जीव ज्यादा से ज्यादा दो हजार सागरोपम काल तक ही धारण कर सकता है ; इससे अधिक समय तक नहीं । उक्त काल बीतने पर उसे अवश्य ही एकेन्द्रिय (निगोद आदि) में पहुंचना पड़ता है, जहाँ एक श्वास में १८ वार जन्ममरण करते हुए अनन्तकाल तक निवास करना पड़ता है। त्रसपर्याय में रहते हुए यदि कभी वह नरक में पहुंच गया तो वहाँ उसे जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष से लेकर उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा) तेतीस सागरोपमकाल व्यतीत करना पड़ता है। निगोद के सिवा तिर्यंचगति की पृथ्वीकाय आदि अन्य स्थावर जीवयोनियों में पहुंच गया तो वहाँ असंख्यात वर्ष तक रहना पड़ता है। यदि संयोगवश पंचेन्द्रियतिथंचों . या मनुष्यों में से किसी जीवयोनि में पहुंच गया तो वहाँ भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की स्थिति तक रहना पड़ता है।
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने कहा हैं—'अणवदग्गं दोहमद्ध चाउरतं संसारकतार अणुपरियति जीवा मोहवससंनिविट्ठा ।' अर्थात्सीमारहित, लम्बे मार्ग वाले, चातुर्गतिक संसाररूप जंगल में मोहवश अब्रह्मचर्यसेवन में ग्रस्त पामरजीव अनन्तकाल तक बारबार पर्यटन करते रहते हैं।
चारों गतियों में मिलने वाले कटुफल - शास्त्रकार पिछले अध्ययनों के मूलसूत्रपाठों में नरक, तिर्यञ्च और मनुष्यगति में प्राप्त होने वाले विभिन्न दुःखों का विशद वर्णन कर चुके हैं। अतः यहाँ भी अब्रह्मसेवन के फलस्वरूप उन्हीं दुःखों को समझ लेना चाहिए । वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में कुछ गाथाएँ लिखी हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धत कर रहे हैं--
नरएसु जाइं अइकक्खडाई, दुक्खाइं परमतिक्खाई । को वण्णेइ ताइं जीवंतो वासकोडीहिं ॥१॥ कक्खडदाहं सामलि, असिवण-वेयरणि-पहरणसएहि । जा जायणाओ पावंति निरया तं अहम्मफलं ॥२॥