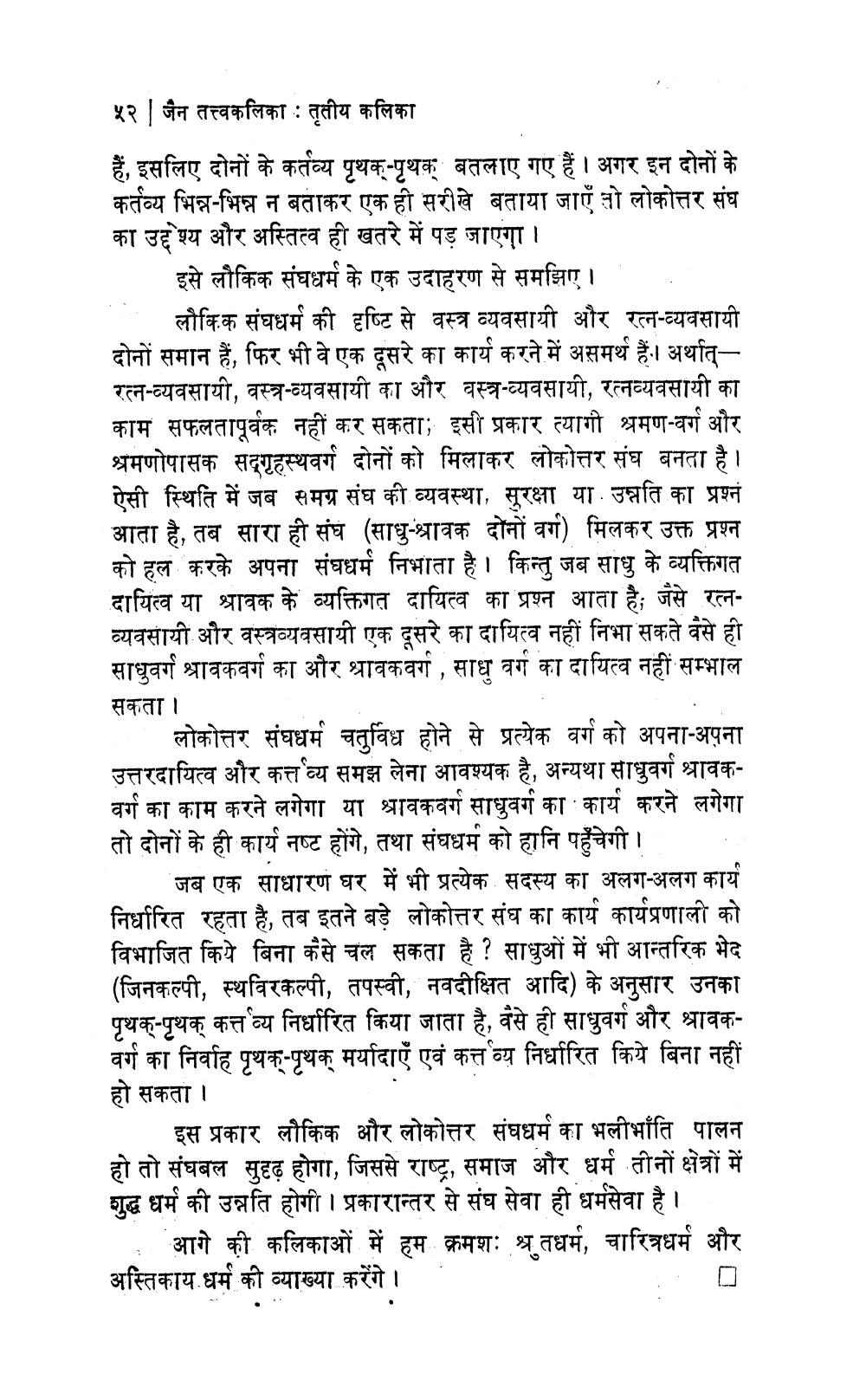________________
५२ | जैन तत्त्वकलिका : तृतीय कलिका
हैं, इसलिए दोनों के कर्तव्य पृथक-पृथक बतलाए गए हैं। अगर इन दोनों के कर्तव्य भिन्न-भिन्न न बताकर एक ही सरीखे बताया जाएँ तो लोकोत्तर संघ का उद्देश्य और अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा ।
इसे लौकिक संघधर्म के एक उदाहरण से समझिए ।
लौकिक संघधर्म की दृष्टि से वस्त्र व्यवसायी और रत्न- व्यवसायी दोनों समान हैं, फिर भी वे एक दूसरे का कार्य करने में असमर्थ हैं । अर्थात् — रत्न- व्यवसायी, वस्त्र व्यवसायी का और वस्त्र व्यवसायी, रत्नव्यवसायी का काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, इसी प्रकार त्यागी श्रमण-वर्ग और श्रमणोपासक सद्गृहस्थवर्ग दोनों को मिलाकर लोकोत्तर संघ बनता है । ऐसी स्थिति में जब समग्र संघ की व्यवस्था, सुरक्षा या उन्नति का प्रश्नं आता है, तब सारा ही संघ ( साधु श्रावक दोनों वर्ग ) मिलकर उक्त प्रश्न को हल करके अपना संघधर्म निभाता है । किन्तु जब साधु के व्यक्तिगत दायित्व या श्रावक के व्यक्तिगत दायित्व का प्रश्न आता है; जैसे रत्नव्यवसायी और वस्त्रव्यवसायी एक दूसरे का दायित्व नहीं निभा सकते वैसे ही साधुवर्ग श्रावकवर्ग का और श्रावकवर्ग, साधु वर्ग का दायित्व नहीं सम्भाल
सकता ।
लोकोत्तर संघधर्म चतुर्विध होने से प्रत्येक वर्ग को अपना-अपना उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य समझ लेना आवश्यक है, अन्यथा साधुवर्ग श्रावकवर्ग का काम करने लगेगा या श्रावकवर्ग साधुवर्ग का कार्य करने लगेगा तो दोनों के ही कार्य नष्ट होंगे, तथा संघधर्म को हानि पहुँचेगी ।
जब एक साधारण घर में भी प्रत्येक सदस्य का अलग-अलग कार्य निर्धारित रहता है, तब इतने बड़े लोकोत्तर संघ का कार्य कार्यप्रणाली को विभाजित किये बिना कैसे चल सकता है ? साधुओं में भी आन्तरिक भेद (जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, तपस्वी, नवदीक्षित आदि) के अनुसार उनका पृथक्-पृथक् कर्त्तव्य निर्धारित किया जाता है, वैसे ही साधुवर्ग और श्रावकवर्ग का निर्वाह पृथक्-पृथक् मर्यादाएँ एवं कत्तव्य निर्धारित किये बिना नहीं हो सकता ।
इस प्रकार लौकिक और लोकोत्तर संघधर्म का भलीभाँति पालन हो तो संघबल सुदृढ़ होगा, जिससे राष्ट्र, समाज और धर्म तीनों क्षेत्रों में शुद्ध धर्म की उन्नति होगी । प्रकारान्तर से संघ सेवा ही धर्मसेवा है ।
आगे की कलिकाओं में हम क्रमशः श्रुतधर्म, चारित्रधर्म और अस्तिकाय धर्म की व्याख्या करेंगे ।