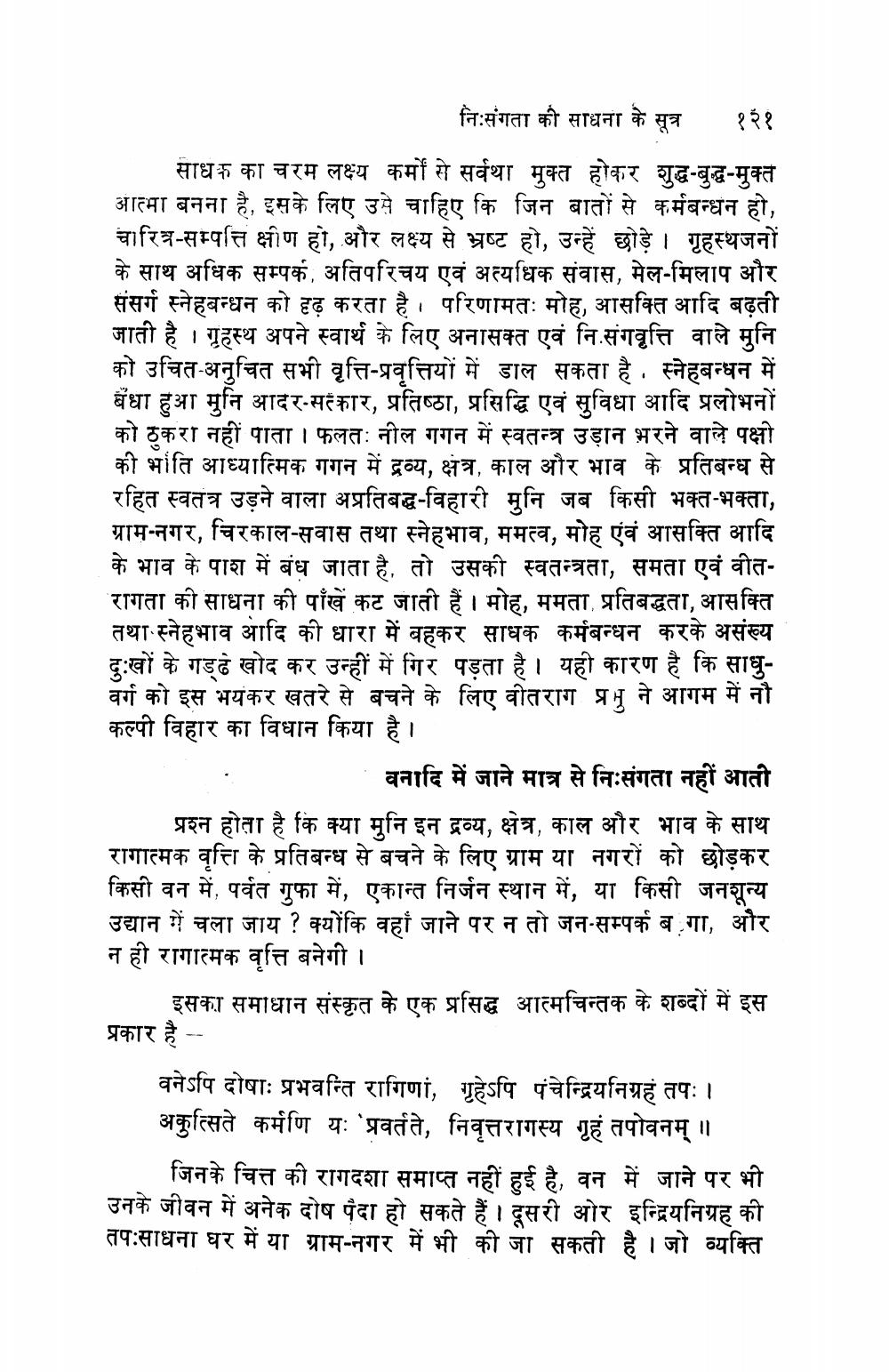________________
निःसंगता की साधना के
सूत्र १२१
साधक का चरम लक्ष्य कर्मों से सर्वथा मुक्त होकर शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा बनना है, इसके लिए उसे चाहिए कि जिन बातों से कर्मबन्धन हो, चारित्र - सम्पत्ति क्षीण हो, और लक्ष्य से भ्रष्ट हो, उन्हें छोड़े । गृहस्थजनों के साथ अधिक सम्पर्क, अतिपरिचय एवं अत्यधिक संवास, मेल-मिलाप और संसर्ग स्नेहबन्धन को दृढ़ करता है। परिणामतः मोह, आसक्ति आदि बढ़ती
1
त है। गृहस्थ अपने स्वार्थ के लिए अनासक्त एवं निःसंगवृत्ति वाले मुनि को उचित - अनुचित सभी वृत्ति प्रवृत्तियों में डाल सकता है स्नेहबन्धन में बँधा हुआ मुनि आदर-सत्कार, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि एवं सुविधा आदि प्रलोभनों को ठुकरा नहीं पाता । फलतः नील गगन में स्वतन्त्र उड़ान भरने वाले पक्षी की भांति आध्यात्मिक गगन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के प्रतिबन्ध से रहित स्वतंत्र उड़ने वाला अप्रतिबद्ध - विहारी मुनि जब किसी भक्त भक्ता, ग्राम-नगर, चिरकाल-सवास तथा स्नेहभाव, ममत्व, मोह एवं आसक्ति आदि के भाव के पाश में बंध जाता है, तो उसकी स्वतन्त्रता, समता एवं वीतरागता की साधना की पाँखें कट जाती हैं। मोह, ममता, प्रतिबद्धता, आसक्ति तथा स्नेहभाव आदि की धारा में बहकर साधक कर्मबन्धन करके असंख्य दुःखों के गड्ढे खोद कर उन्हीं में गिर पड़ता है । यही कारण है कि साधुवर्ग को इस भयंकर खतरे से बचने के लिए वीतराग प्रभु ने आगम में नौ कल्पी विहार का विधान किया है ।
वनादि में जाने मात्र से निःसंगता नहीं आती
प्रश्न होता है कि क्या मुनि इन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ रागात्मक वृत्ति के प्रतिबन्ध से बचने के लिए ग्राम या नगरों को छोड़कर किसी वन में, पर्वत गुफा में, एकान्त निर्जन स्थान में, या किसी जनशून्य उद्यान में चला जाय ? क्योंकि वहाँ जाने पर न तो जन-सम्पर्क बगा, और न ही रागात्मक वृत्ति बनेगी ।
इसका समाधान संस्कृत के एक प्रसिद्ध आत्मचिन्तक के शब्दों में इस प्रकार है
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पंचेन्द्रियनिग्रहं तपः । अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥
जिनके चित्त की रागदशा समाप्त नहीं हुई है, वन में जाने पर भी उनके जीवन में अनेक दोष पैदा हो सकते हैं । दूसरी ओर इन्द्रियनिग्रह की तप:साधना घर में या ग्राम-नगर में भी की जा सकती है । जो व्यक्ति