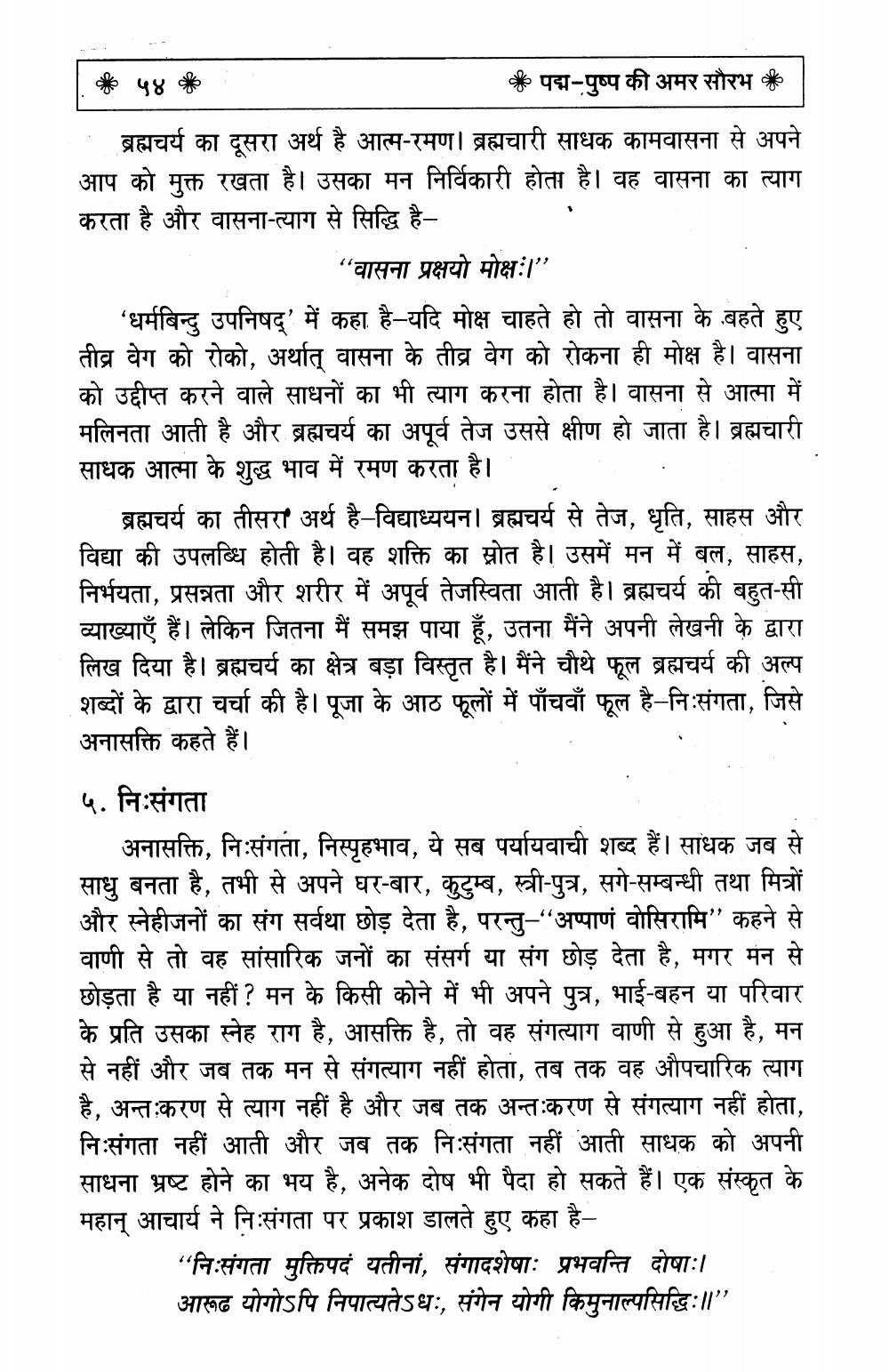________________
५४
* पद्म-पुष्प की अमर सौरभ
ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है आत्म- रमण । ब्रह्मचारी साधक कामवासना से अपने आप को मुक्त रखता है। उसका मन निर्विकारी होता है। वह वासना का त्याग करता है और वासना-त्याग से सिद्धि है
"वासना प्रक्षयो मोक्षः ।”
'धर्मबिन्दु उपनिषद्' में कहा है- यदि मोक्ष चाहते हो तो वासना के बहते हुए तीव्र वेग को रोको, अर्थात् वासना के तीव्र वेग को रोकना ही मोक्ष है । वासना को उद्दीप्त करने वाले साधनों का भी त्याग करना होता है। वासना से आत्मा में मलिनता आती है और ब्रह्मचर्य का अपूर्व तेज उससे क्षीण हो जाता है । ब्रह्मचारी साधक आत्मा के शुद्ध भाव में रमण करता है ।
1
ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ है - विद्याध्ययन । ब्रह्मचर्य से तेज, धृति, साहस और विद्या की उपलब्धि होती है । वह शक्ति का स्रोत है । उसमें मन में बल, साहस, निर्भयता, प्रसन्नता और शरीर में अपूर्व तेजस्विता आती है । ब्रह्मचर्य की बहुत-सी व्याख्याएँ हैं। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, उतना मैंने अपनी लेखनी के द्वारा लिख दिया है। ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । मैंने चौथे फूल ब्रह्मचर्य की अल्प शब्दों के द्वारा चर्चा की है। पूजा के आठ फूलों में पाँचवाँ फूल है - निःसंगता, जिसे अनासक्ति कहते हैं।
५. निःसंगता
अनासक्ति, निःसंगता, निस्पृहभाव, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। साधक जब से साधु बनता है, तभी से अपने घर-बार, कुटुम्ब, स्त्री-पुत्र, सगे-सम्बन्धी तथा मित्रों और स्नेहीजनों का संग सर्वथा छोड़ देता है, परन्तु - " अप्पाणं वोसिरामि" कहने से वाणी से तो वह सांसारिक जनों का संसर्ग या संग छोड़ देता है, मगर मन से छोड़ता है या नहीं ? मन के किसी कोने में भी अपने पुत्र, भाई- बहन या परिवार के प्रति उसका स्नेह राग है, आसक्ति है, तो वह संगत्याग वाणी से हुआ है, मन से नहीं और जब तक मन से संगत्याग नहीं होता, तब तक वह औपचारिक त्याग है, अन्तःकरण से त्याग नहीं है और जब तक अन्तःकरण से संगत्याग नहीं होता, निःसंगता नहीं आती और जब तक निःसंगता नहीं आती साधक को अपनी साधना भ्रष्ट होने का भय है, अनेक दोष भी पैदा हो सकते हैं। एक संस्कृत के महान् आचार्य ने निःसंगता पर प्रकाश डालते हुए कहा है
"निःसंगता मुक्तिपदं यतीनां संगादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः । आरूढ योगोऽपि निपात्यतेऽधः, संगेन योगी किमुनाल्पसिद्धिः॥”