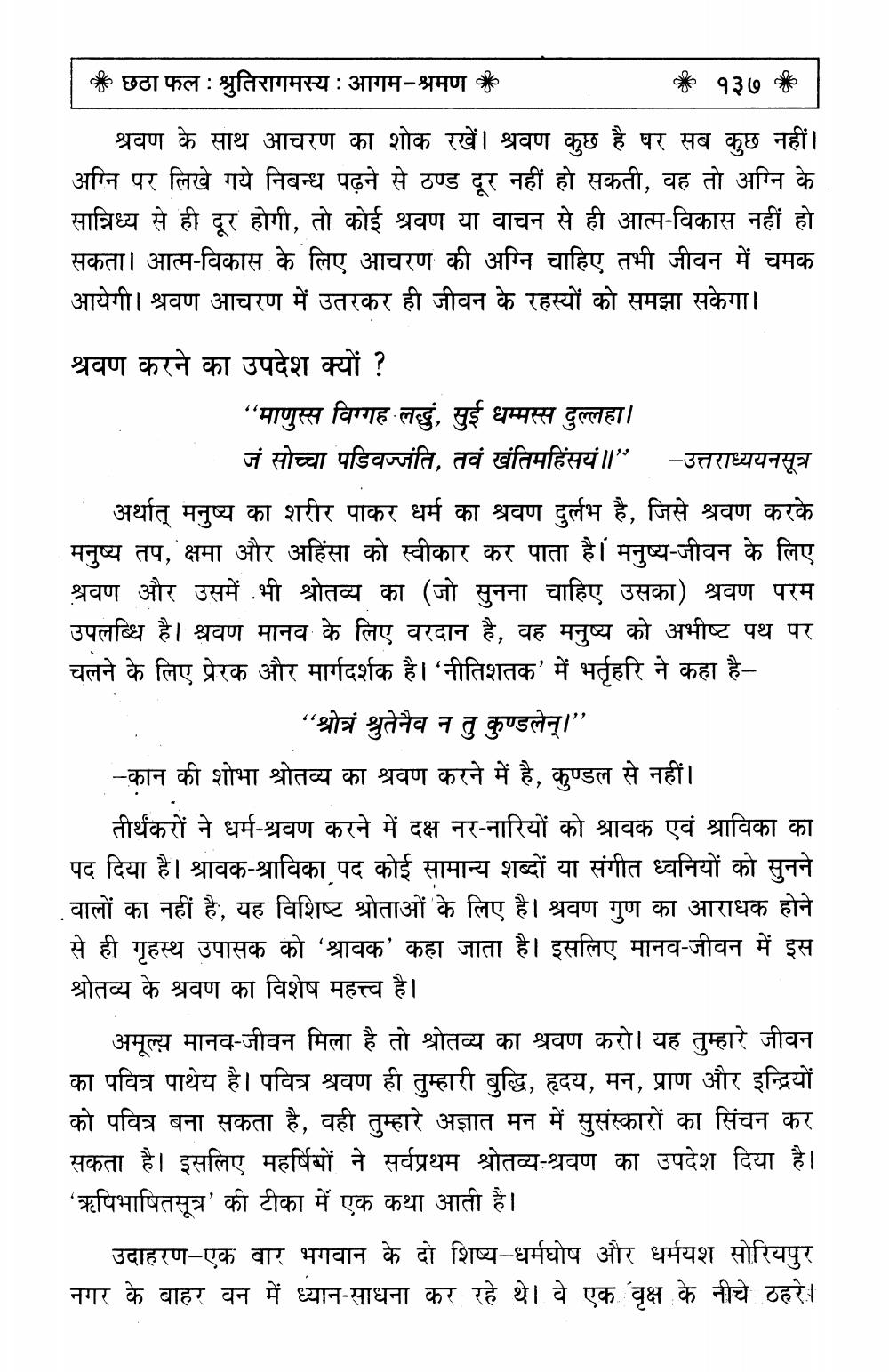________________
* छठा फल : श्रुतिरागमस्य : आगम-श्रमण *
* १३७ * श्रवण के साथ आचरण का शोक रखें। श्रवण कुछ है पर सब कुछ नहीं। अग्नि पर लिखे गये निबन्ध पढ़ने से ठण्ड दूर नहीं हो सकती, वह तो अग्नि के सान्निध्य से ही दूर होगी, तो कोई श्रवण या वाचन से ही आत्म-विकास नहीं हो सकता। आत्म-विकास के लिए आचरण की अग्नि चाहिए तभी जीवन में चमक आयेगी। श्रवण आचरण में उतरकर ही जीवन के रहस्यों को समझा सकेगा।
श्रवण करने का उपदेश क्यों ?
“माणुस्स विग्गह लद्धं, सुई धम्मस्स दुल्लहा।
जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिमहिंसयं॥" -उत्तराध्ययनसूत्र अर्थात् मनुष्य का शरीर पाकर धर्म का श्रवण दुर्लभ है, जिसे श्रवण करके मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार कर पाता है। मनुष्य-जीवन के लिए श्रवण और उसमें भी श्रोतव्य का (जो सुनना चाहिए उसका) श्रवण परम उपलब्धि है। श्रवण मानव के लिए वरदान है, वह मनुष्य को अभीष्ट पथ पर चलने के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक है। 'नीतिशतक' में भर्तृहरि ने कहा है
“श्रोत्रं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन्।" -कान की शोभा श्रोतव्य का श्रवण करने में है, कुण्डल से नहीं।
तीर्थंकरों ने धर्म-श्रवण करने में दक्ष नर-नारियों को श्रावक एवं श्राविका का पद दिया है। श्रावक-श्राविका पद कोई सामान्य शब्दों या संगीत ध्वनियों को सुनने वालों का नहीं है, यह विशिष्ट श्रोताओं के लिए है। श्रवण गुण का आराधक होने से ही गृहस्थ उपासक को 'श्रावक' कहा जाता है। इसलिए मानव-जीवन में इस श्रोतव्य के श्रवण का विशेष महत्त्व है।
अमूल्य मानव-जीवन मिला है तो श्रोतव्य का श्रवण करो। यह तुम्हारे जीवन का पवित्र पाथेय है। पवित्र श्रवण ही तुम्हारी बुद्धि, हृदय, मन, प्राण और इन्द्रियों को पवित्र बना सकता है, वही तुम्हारे अज्ञात मन में सुसंस्कारों का सिंचन कर सकता है। इसलिए महर्षियों ने सर्वप्रथम श्रोतव्य-श्रवण का उपदेश दिया है। 'ऋषिभाषितसूत्र' की टीका में एक कथा आती है।
उदाहरण-एक बार भगवान के दो शिष्य-धर्मघोष और धर्मयश सोरियपुर नगर के बाहर वन में ध्यान-साधना कर रहे थे। वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे।