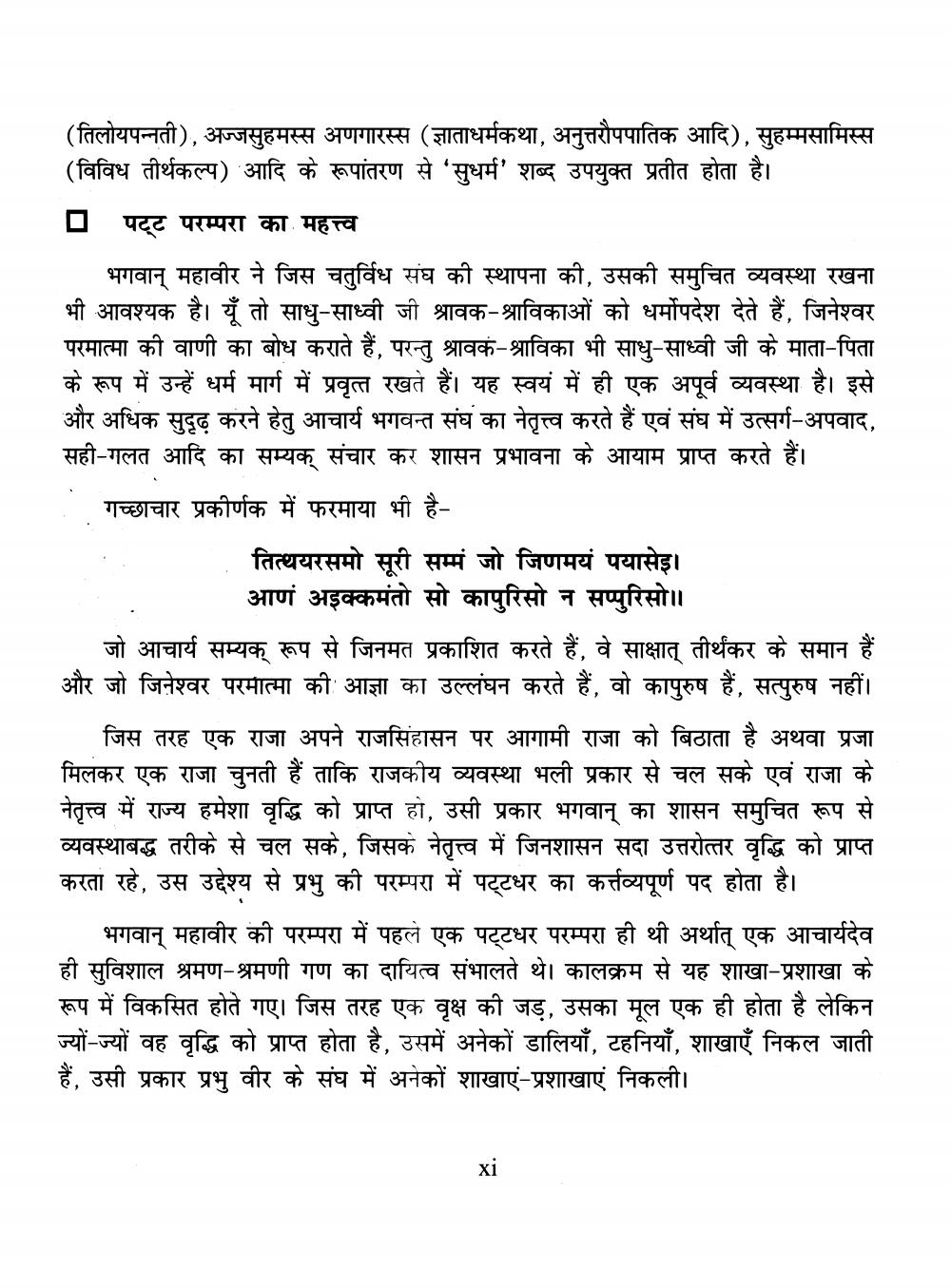________________
(तिलोयपन्नती), अज्जसुहमस्स अणगारस्स (ज्ञाताधर्मकथा, अनुत्तरौपपातिक आदि), सुहम्मसामिस्स (विविध तीर्थकल्प) आदि के रूपांतरण से 'सुधर्म' शब्द उपयुक्त प्रतीत होता है। - पट्ट परम्परा का महत्त्व
भगवान् महावीर ने जिस चतुर्विध संघ की स्थापना की, उसकी समुचित व्यवस्था रखना भी आवश्यक है। यूँ तो साधु-साध्वी जी श्रावक-श्राविकाओं को धर्मोपदेश देते हैं, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी का बोध कराते हैं, परन्तु श्रावक-श्राविका भी साधु-साध्वी जी के माता-पिता के रूप में उन्हें धर्म मार्ग में प्रवृत्त रखते हैं। यह स्वयं में ही एक अपूर्व व्यवस्था है। इसे और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आचार्य भगवन्त संघ का नेतृत्त्व करते हैं एवं संघ में उत्सर्ग-अपवाद, सही-गलत आदि का सम्यक् संचार कर शासन प्रभावना के आयाम प्राप्त करते हैं। गच्छाचार प्रकीर्णक में फरमाया भी है
तित्थयरसमो सूरी सम्म जो जिणमयं पयासेइ।
आणं अइक्कमंतो सो कापुरिसो न सप्पुरिसो॥ जो आचार्य सम्यक् रूप से जिनमत प्रकाशित करते हैं, वे साक्षात् तीर्थंकर के समान हैं और जो जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो कापुरुष हैं, सत्पुरुष नहीं।
जिस तरह एक राजा अपने राजसिंहासन पर आगामी राजा को बिठाता है अथवा प्रजा मिलकर एक राजा चुनती हैं ताकि राजकीय व्यवस्था भली प्रकार से चल सके एवं राजा के नेतृत्त्व में राज्य हमेशा वृद्धि को प्राप्त हो, उसी प्रकार भगवान् का शासन समुचित रूप से व्यवस्थाबद्ध तरीके से चल सके, जिसके नेतृत्त्व में जिनशासन सदा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता रहे, उस उद्देश्य से प्रभु की परम्परा में पट्टधर का कर्तव्यपूर्ण पद होता है।
भगवान् महावीर की परम्परा में पहले एक पट्टधर परम्परा ही थी अर्थात् एक आचार्यदेव ही सुविशाल श्रमण-श्रमणी गण का दायित्व संभालते थे। कालक्रम से यह शाखा-प्रशाखा के रूप में विकसित होते गए। जिस तरह एक वृक्ष की जड़, उसका मूल एक ही होता है लेकिन ज्यों-ज्यों वह वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें अनेकों डालियाँ, टहनियाँ, शाखाएँ निकल जाती हैं, उसी प्रकार प्रभु वीर के संघ में अनेकों शाखाएं-प्रशाखाएं निकली।
xi