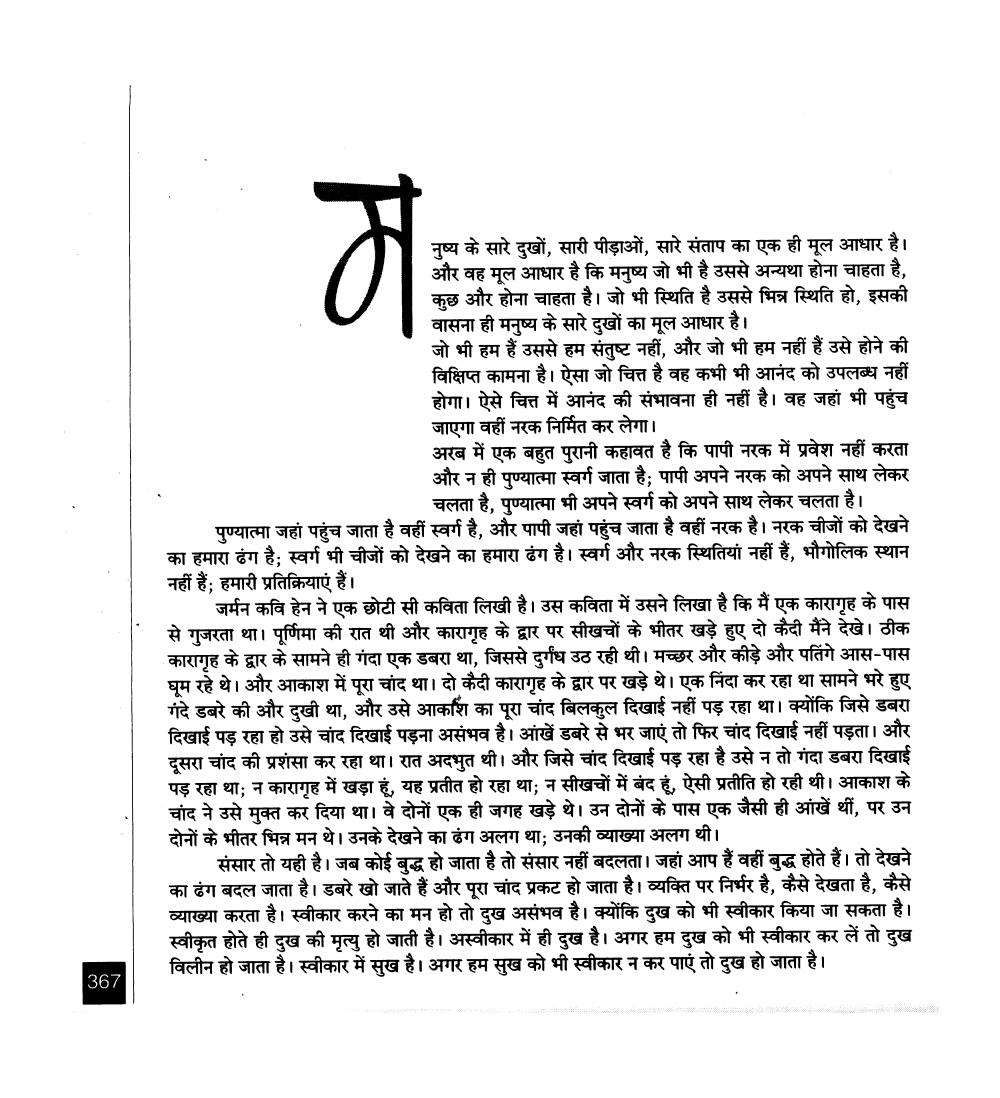________________
नुष्य के सारे दुखों, सारी पीड़ाओं, सारे संताप का एक ही मूल आधार है। और वह मूल आधार है कि मनुष्य जो भी है उससे अन्यथा होना चाहता है, कुछ और होना चाहता है। जो भी स्थिति है उससे भिन्न स्थिति हो, इसकी वासना ही मनुष्य के सारे दुखों का मूल आधार है। जो भी हम हैं उससे हम संतुष्ट नहीं, और जो भी हम नहीं हैं उसे होने की विक्षिप्त कामना है। ऐसा जो चित्त है वह कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे चित्त में आनंद की संभावना ही नहीं है। वह जहां भी पहुंच जाएगा वहीं नरक निर्मित कर लेगा। अरब में एक बहुत पुरानी कहावत है कि पापी नरक में प्रवेश नहीं करता और न ही पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है; पापी अपने नरक को अपने साथ लेकर
चलता है, पुण्यात्मा भी अपने स्वर्ग को अपने साथ लेकर चलता है। पुण्यात्मा जहां पहुंच जाता है वहीं स्वर्ग है, और पापी जहां पहुंच जाता है वहीं नरक है। नरक चीजों को देखने का हमारा ढंग है; स्वर्ग भी चीजों को देखने का हमारा ढंग है। स्वर्ग और नरक स्थितियां नहीं हैं, भौगोलिक स्थान नहीं हैं; हमारी प्रतिक्रियाएं हैं।
जर्मन कवि हेन ने एक छोटी सी कविता लिखी है। उस कविता में उसने लिखा है कि मैं एक कारागृह के पास से गुजरता था। पूर्णिमा की रात थी और कारागृह के द्वार पर सीखचों के भीतर खड़े हुए दो कैदी मैंने देखे। ठीक कारागृह के द्वार के सामने ही गंदा एक डबरा था, जिससे दुर्गंध उठ रही थी। मच्छर और कीड़े और पतिंगे आस-पास घूम रहे थे। और आकाश में पूरा चांद था। दो कैदी कारागृह के द्वार पर खड़े थे। एक निंदा कर रहा था सामने भरे हुए गंदे डबरे की और दुखी था, और उसे आकाश का पूरा चांद बिलकुल दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्योंकि जिसे डबरा दिखाई पड़ रहा हो उसे चांद दिखाई पड़ना असंभव है। आंखें डबरे से भर जाएं तो फिर चांद दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरा चांद की प्रशंसा कर रहा था। रात अदभुत थी। और जिसे चांद दिखाई पड़ रहा है उसे न तो गंदा डबरा दिखाई पड़ रहा था; न कारागृह में खड़ा हूं, यह प्रतीत हो रहा था; न सीखचों में बंद हूं, ऐसी प्रतीति हो रही थी। आकाश के चांद ने उसे मुक्त कर दिया था। वे दोनों एक ही जगह खड़े थे। उन दोनों के पास एक जैसी ही आंखें थीं, पर उन दोनों के भीतर भिन्न मन थे। उनके देखने का ढंग अलग था; उनकी व्याख्या अलग थी।।
संसार तो यही है। जब कोई बुद्ध हो जाता है तो संसार नहीं बदलता। जहां आप हैं वहीं बुद्ध होते हैं। तो देखने का ढंग बदल जाता है। डबरे खो जाते हैं और पूरा चांद प्रकट हो जाता है। व्यक्ति पर निर्भर है, कैसे देखता है, कैसे व्याख्या करता है। स्वीकार करने का मन हो तो दुख असंभव है। क्योंकि दुख को भी स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृत होते ही दुख की मृत्यु हो जाती है। अस्वीकार में ही दुख है। अगर हम दुख को भी स्वीकार कर लें तो दुख विलीन हो जाता है। स्वीकार में सुख है। अगर हम सुख को भी स्वीकार न कर पाएं तो दुख हो जाता है।
367