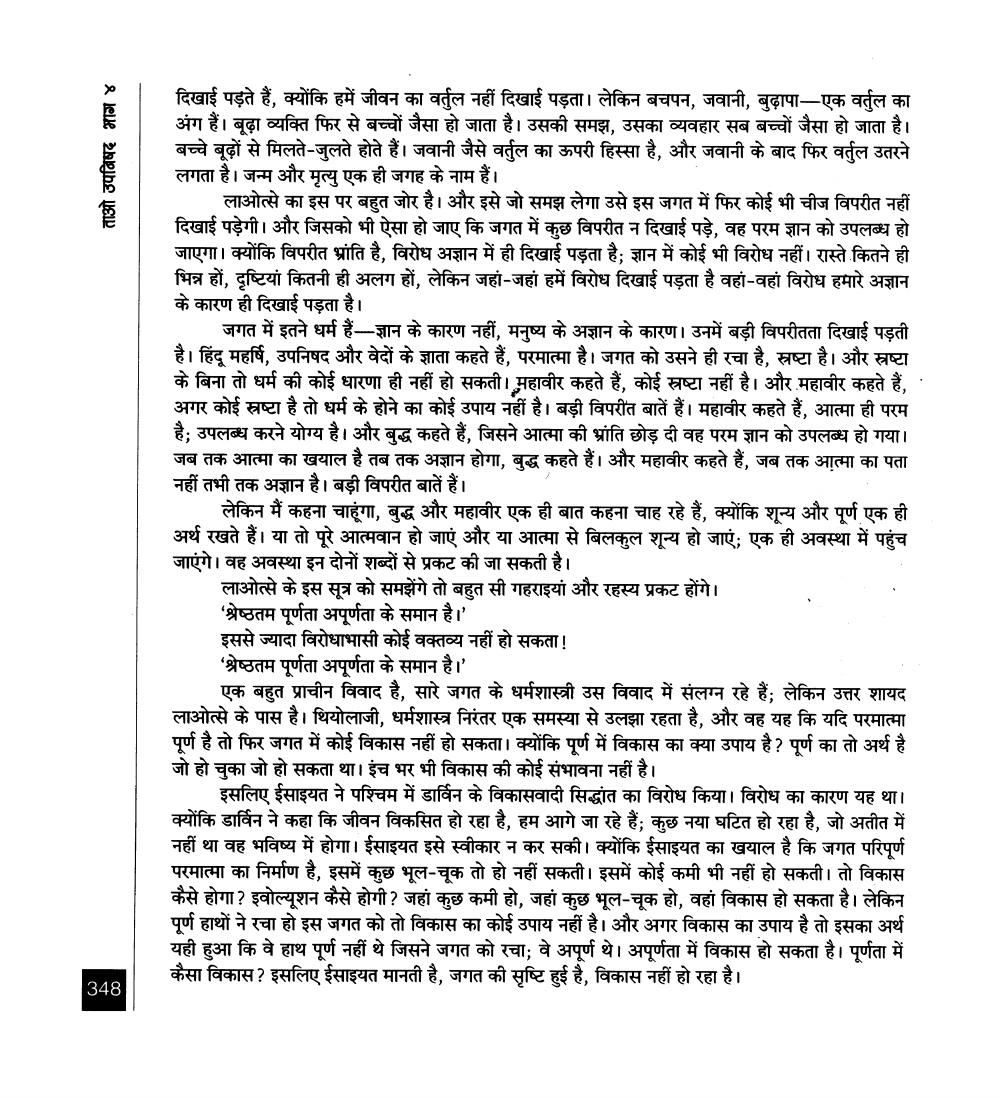________________
ताओ उपनिषद भाग ४
दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमें जीवन का वर्तल नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन बचपन, जवानी, बुढ़ापा-एक वर्तुल का अंग हैं। बूढ़ा व्यक्ति फिर से बच्चों जैसा हो जाता है। उसकी समझ, उसका व्यवहार सब बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चे बूढ़ों से मिलते-जुलते होते हैं। जवानी जैसे वर्तुल का ऊपरी हिस्सा है, और जवानी के बाद फिर वर्तुल उतरने लगता है। जन्म और मृत्यु एक ही जगह के नाम हैं।
लाओत्से का इस पर बहुत जोर है। और इसे जो समझ लेगा उसे इस जगत में फिर कोई भी चीज विपरीत नहीं दिखाई पड़ेगी। और जिसको भी ऐसा हो जाए कि जगत में कुछ विपरीत न दिखाई पड़े, वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि विपरीत भ्रांति है, विरोध अज्ञान में ही दिखाई पड़ता है; ज्ञान में कोई भी विरोध नहीं। रास्ते कितने ही भिन्न हों, दृष्टियां कितनी ही अलग हों, लेकिन जहां-जहां हमें विरोध दिखाई पड़ता है वहां-वहां विरोध हमारे अज्ञान के कारण ही दिखाई पड़ता है।
जगत में इतने धर्म हैं-ज्ञान के कारण नहीं, मनुष्य के अज्ञान के कारण। उनमें बड़ी विपरीतता दिखाई पड़ती है। हिंदू महर्षि, उपनिषद और वेदों के ज्ञाता कहते हैं, परमात्मा है। जगत को उसने ही रचा है, स्रष्टा है। और स्रष्टा के बिना तो धर्म की कोई धारणा ही नहीं हो सकती। महावीर कहते हैं, कोई स्रष्टा नहीं है। और महावीर कहते हैं, . अगर कोई स्रष्टा है तो धर्म के होने का कोई उपाय नहीं है। बड़ी विपरीत बातें हैं। महावीर कहते हैं, आत्मा ही परम है; उपलब्ध करने योग्य है। और बुद्ध कहते हैं, जिसने आत्मा की भ्रांति छोड़ दी वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जब तक आत्मा का खयाल है तब तक अज्ञान होगा, बुद्ध कहते हैं। और महावीर कहते हैं, जब तक आत्मा का पता नहीं तभी तक अज्ञान है। बड़ी विपरीत बातें हैं।
लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बुद्ध और महावीर एक ही बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही अर्थ रखते हैं। या तो पूरे आत्मवान हो जाएं और या आत्मा से बिलकुल शून्य हो जाएं; एक ही अवस्था में पहुंच जाएंगे। वह अवस्था इन दोनों शब्दों से प्रकट की जा सकती है।
लाओत्से के इस सूत्र को समझेंगे तो बहुत सी गहराइयां और रहस्य प्रकट होंगे। 'श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है।' इससे ज्यादा विरोधाभासी कोई वक्तव्य नहीं हो सकता! 'श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है।'
एक बहुत प्राचीन विवाद है, सारे जगत के धर्मशास्त्री उस विवाद में संलग्न रहे हैं; लेकिन उत्तर शायद लाओत्से के पास है। थियोलाजी, धर्मशास्त्र निरंतर एक समस्या से उलझा रहता है, और वह यह कि यदि परमात्मा पूर्ण है तो फिर जगत में कोई विकास नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्ण में विकास का क्या उपाय है? पूर्ण का तो अर्थ है जो हो चुका जो हो सकता था। इंच भर भी विकास की कोई संभावना नहीं है।
इसलिए ईसाइयत ने पश्चिम में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का विरोध किया। विरोध का कारण यह था। क्योंकि डार्विन ने कहा कि जीवन विकसित हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं; कुछ नया घटित हो रहा है, जो अतीत में नहीं था वह भविष्य में होगा। ईसाइयत इसे स्वीकार न कर सकी। क्योंकि ईसाइयत का खयाल है कि जगत परिपूर्ण परमात्मा का निर्माण है, इसमें कुछ भूल-चूक तो हो नहीं सकती। इसमें कोई कमी भी नहीं हो सकती। तो विकास कैसे होगा? इवोल्यूशन कैसे होगी? जहां कुछ कमी हो, जहां कुछ भूल-चूक हो, वहां विकास हो सकता है। लेकिन पूर्ण हाथों ने रचा हो इस जगत को तो विकास का कोई उपाय नहीं है। और अगर विकास का उपाय है तो इसका अर्थ यही हुआ कि वे हाथ पूर्ण नहीं थे जिसने जगत को रचा; वे अपूर्ण थे। अपूर्णता में विकास हो सकता है। पूर्णता में कैसा विकास? इसलिए ईसाइयत मानती है, जगत की सृष्टि हुई है, विकास नहीं हो रहा है।
348