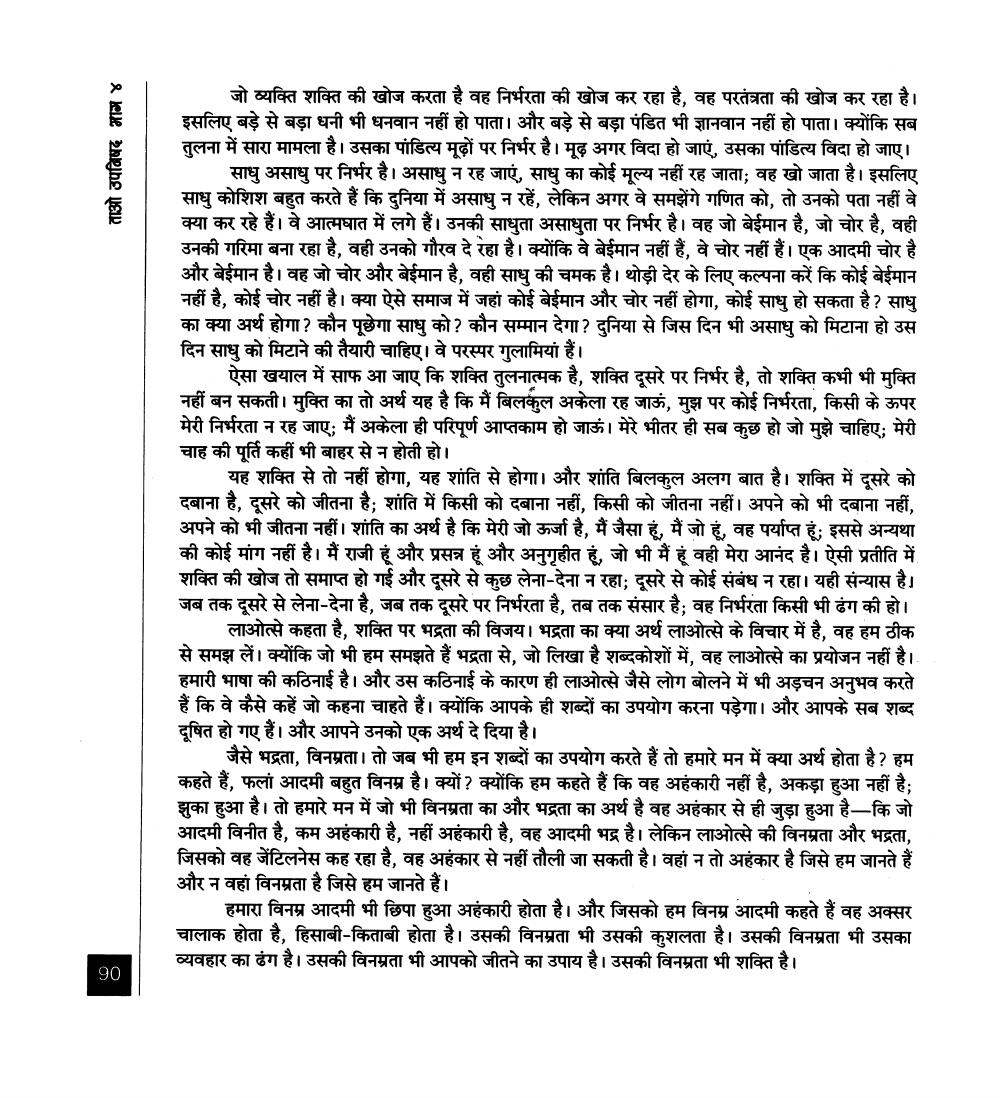________________
ताओ उपनिषद भाग ४
जो व्यक्ति शक्ति की खोज करता है वह निर्भरता की खोज कर रहा है, वह परतंत्रता की खोज कर रहा है। इसलिए बड़े से बड़ा धनी भी धनवान नहीं हो पाता। और बड़े से बड़ा पंडित भी ज्ञानवान नहीं हो पाता। क्योंकि सब तुलना में सारा मामला है। उसका पांडित्य मूढ़ों पर निर्भर है। मूढ़ अगर विदा हो जाएं, उसका पांडित्य विदा हो जाए।
साधु असाधु पर निर्भर है। असाधु न रह जाएं, साधु का कोई मूल्य नहीं रह जाता; वह खो जाता है। इसलिए साधु कोशिश बहुत करते हैं कि दुनिया में असाधु न रहें, लेकिन अगर वे समझेंगे गणित को, तो उनको पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। वे आत्मघात में लगे हैं। उनकी साधुता असाधुता पर निर्भर है। वह जो बेईमान है, जो चोर है, वही उनकी गरिमा बना रहा है, वही उनको गौरव दे रहा है। क्योंकि वे बेईमान नहीं हैं, वे चोर नहीं हैं। एक आदमी चोर है
और बेईमान है। वह जो चोर और बेईमान है, वही साधु की चमक है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि कोई बेईमान नहीं है, कोई चोर नहीं है। क्या ऐसे समाज में जहां कोई बेईमान और चोर नहीं होगा, कोई साधु हो सकता है? साधु का क्या अर्थ होगा? कौन पूछेगा साधु को? कौन सम्मान देगा? दुनिया से जिस दिन भी असाधु को मिटाना हो उस दिन साधु को मिटाने की तैयारी चाहिए। वे परस्पर गुलामियां हैं।
ऐसा खयाल में साफ आ जाए कि शक्ति तुलनात्मक है, शक्ति दूसरे पर निर्भर है, तो शक्ति कभी भी मुक्ति नहीं बन सकती। मुक्ति का तो अर्थ यह है कि मैं बिलकुल अकेला रह जाऊं, मुझ पर कोई निर्भरता, किसी के ऊपर मेरी निर्भरता न रह जाए; मैं अकेला ही परिपूर्ण आप्तकाम हो जाऊं। मेरे भीतर ही सब कुछ हो जो मुझे चाहिए; मेरी चाह की पूर्ति कहीं भी बाहर से न होती हो।
यह शक्ति से तो नहीं होगा, यह शांति से होगा। और शांति बिलकुल अलग बात है। शक्ति में दूसरे को दबाना है, दूसरे को जीतना है; शांति में किसी को दबाना नहीं, किसी को जीतना नहीं। अपने को भी दबाना नहीं, अपने को भी जीतना नहीं। शांति का अर्थ है कि मेरी जो ऊर्जा है, मैं जैसा हूं, मैं जो हूं, वह पर्याप्त हूं; इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं है। मैं राजी हूं और प्रसन्न हूं और अनुगृहीत हूं, जो भी मैं हूं वही मेरा आनंद है। ऐसी प्रतीति में शक्ति की खोज तो समाप्त हो गई और दूसरे से कुछ लेना-देना न रहा; दूसरे से कोई संबंध न रहा। यही संन्यास है। जब तक दूसरे से लेना-देना है, जब तक दूसरे पर निर्भरता है, तब तक संसार है; वह निर्भरता किसी भी ढंग की हो।
लाओत्से कहता है, शक्ति पर भद्रता की विजय। भद्रता का क्या अर्थ लाओत्से के विचार में है, वह हम ठीक से समझ लें। क्योंकि जो भी हम समझते हैं भद्रता से, जो लिखा है शब्दकोशों में, वह लाओत्से का प्रयोजन नहीं है। हमारी भाषा की कठिनाई है। और उस कठिनाई के कारण ही लाओत्से जैसे लोग बोलने में भी अड़चन अनुभव करते हैं कि वे कैसे कहें जो कहना चाहते हैं। क्योंकि आपके ही शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। और आपके सब शब्द दूषित हो गए हैं। और आपने उनको एक अर्थ दे दिया है।
जैसे भद्रता, विनम्रता। तो जब भी हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारे मन में क्या अर्थ होता है? हम कहते हैं, फला आदमी बहुत विनम्र है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि वह अहंकारी नहीं है, अकड़ा हुआ नहीं है; झुका हुआ है। तो हमारे मन में जो भी विनम्रता का और भद्रता का अर्थ है वह अहंकार से ही जुड़ा हुआ है कि जो आदमी विनीत है, कम अहंकारी है, नहीं अहंकारी है, वह आदमी भद्र है। लेकिन लाओत्से की विनम्रता और भद्रता, जिसको वह जेंटिलनेस कह रहा है, वह अहंकार से नहीं तौली जा सकती है। वहां न तो अहंकार है जिसे हम जानते हैं और न वहां विनम्रता है जिसे हम जानते हैं।
हमारा विनम्र आदमी भी छिपा हुआ अहंकारी होता है। और जिसको हम विनम्र आदमी कहते हैं वह अक्सर चालाक होता है, हिसाबी-किताबी होता है। उसकी विनम्रता भी उसकी कुशलता है। उसकी विनम्रता भी उसका व्यवहार का ढंग है। उसकी विनम्रता भी आपको जीतने का उपाय है। उसकी विनम्रता भी शक्ति है।
90