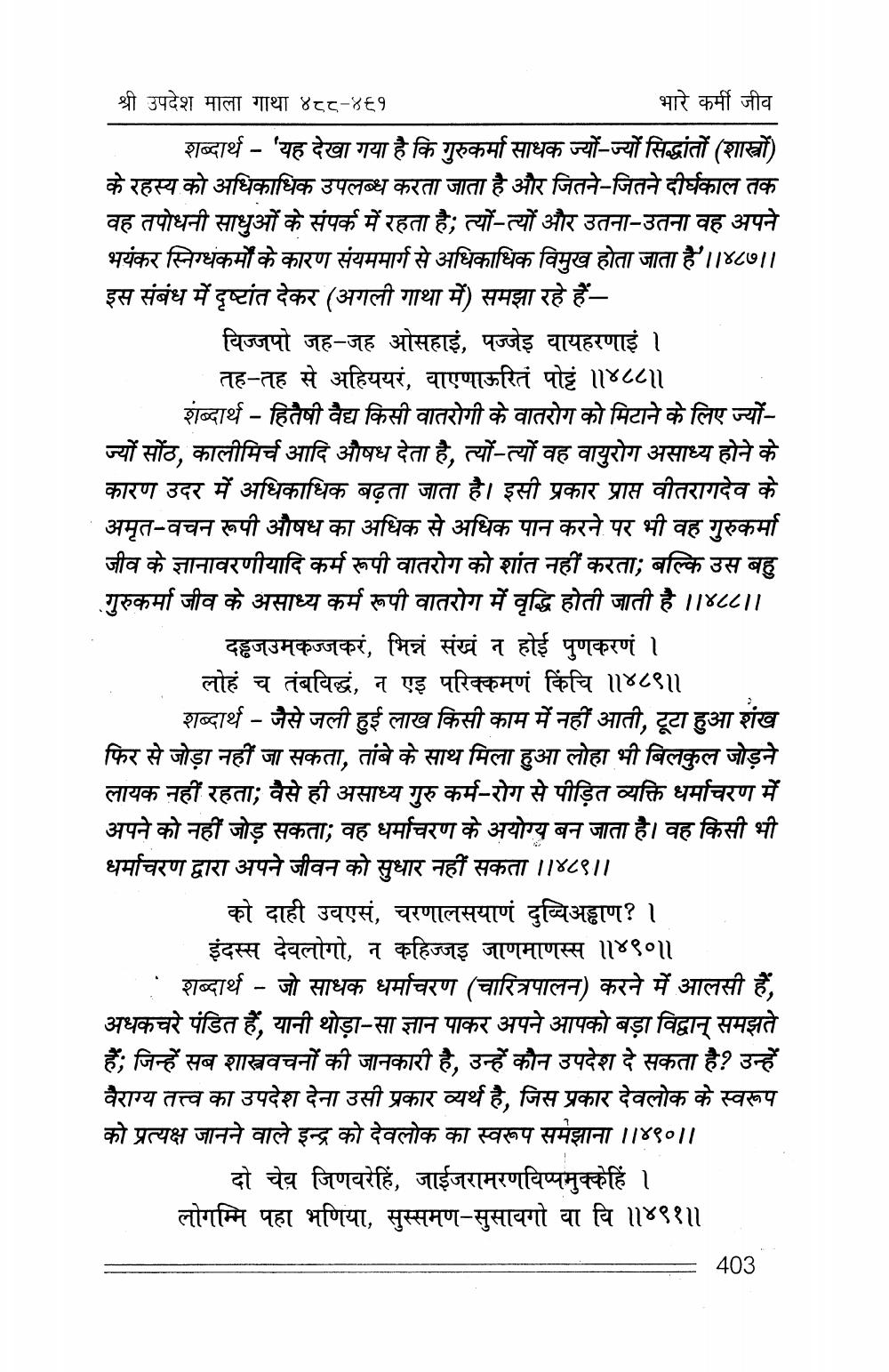________________
श्री उपदेश माला गाथा ४८८-४६१
भारे कर्मी जीव शब्दार्थ - 'यह देखा गया है कि गुरुकर्मा साधक ज्यों-ज्यों सिद्धांतों (शास्त्रों) के रहस्य को अधिकाधिक उपलब्ध करता जाता है और जितने-जितने दीर्घकाल तक वह तपोधनी साधुओं के संपर्क में रहता है; त्यों-त्यों और उतना-उतना वह अपने भयंकर स्निग्धकर्मों के कारण संयममार्ग से अधिकाधिक विमुख होता जाता है ।।४८७।। इस संबंध में दृष्टांत देकर (अगली गाथा में) समझा रहे हैं
विज्जपो जह-जह ओसहाइं, पज्जेइ वायहरणाई । तह-तह से अहिययरं, वाएगाऊरितं पोटें ॥४८८॥
शब्दार्थ - हितैषी वैद्य किसी वातरोगी के वातरोग को मिटाने के लिए ज्योंज्यों सोंठ, कालीमिर्च आदि औषध देता है, त्यों-त्यों वह वायुरोग असाध्य होने के कारण उदर में अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इसी प्रकार प्राप्त वीतरागदेव के अमृत-वचन रूपी औषध का अधिक से अधिक पान करने पर भी वह गुरुकर्मा जीव के ज्ञानावरणीयादि कर्म रूपी वातरोग को शांत नहीं करता; बल्कि उस बहु गुरुकर्मा जीव के असाध्य कर्म रूपी वातरोग में वृद्धि होती जाती है ।।४८८।।
दड्डजउमज्जकर, भिन्नं संखं न होई पुणकरणं । लोहं च तंबविद्धं, न एइ परिक्कमणं किंचि ॥४८९॥
शब्दार्थ - जैसे जली हुई लाख किसी काम में नहीं आती, टूटा हुआ शंख फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, तांबे के साथ मिला हुआ लोहा भी बिलकुल जोड़ने लायक नहीं रहता; वैसे ही असाध्य गुरु कर्म-रोग से पीड़ित व्यक्ति धर्माचरण में अपने को नहीं जोड़ सकता; वह धर्माचरण के अयोग्य बन जाता है। वह किसी भी धर्माचरण द्वारा अपने जीवन को सुधार नहीं सकता ।।४८९।।
___ को दाही उवएसं, चरणालसयाणं दुब्बिअड्डाण? ।
इंदस्स देवलोगो, न कहिज्जड़ जाणमाणस्स ॥४९०॥ ' शब्दार्थ - जो साधक धर्माचरण (चारित्रपालन) करने में आलसी हैं, अधकचरे पंडित हैं, यानी थोड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने आपको बड़ा विद्वान् समझते हैं, जिन्हें सब शास्त्रवचनों की जानकारी है, उन्हें कौन उपदेश दे सकता है? उन्हें वैराग्य तत्त्व का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार देवलोक के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानने वाले इन्द्र को देवलोक का स्वरूप समझाना ।।४९०।।
दो चेव जिणवरेहिं, जाईजरामरणविप्पमुक्केहिं । लोगम्मि पहा भणिया, सुस्समण-सुसावगो वा वि ॥४९१॥
: 403