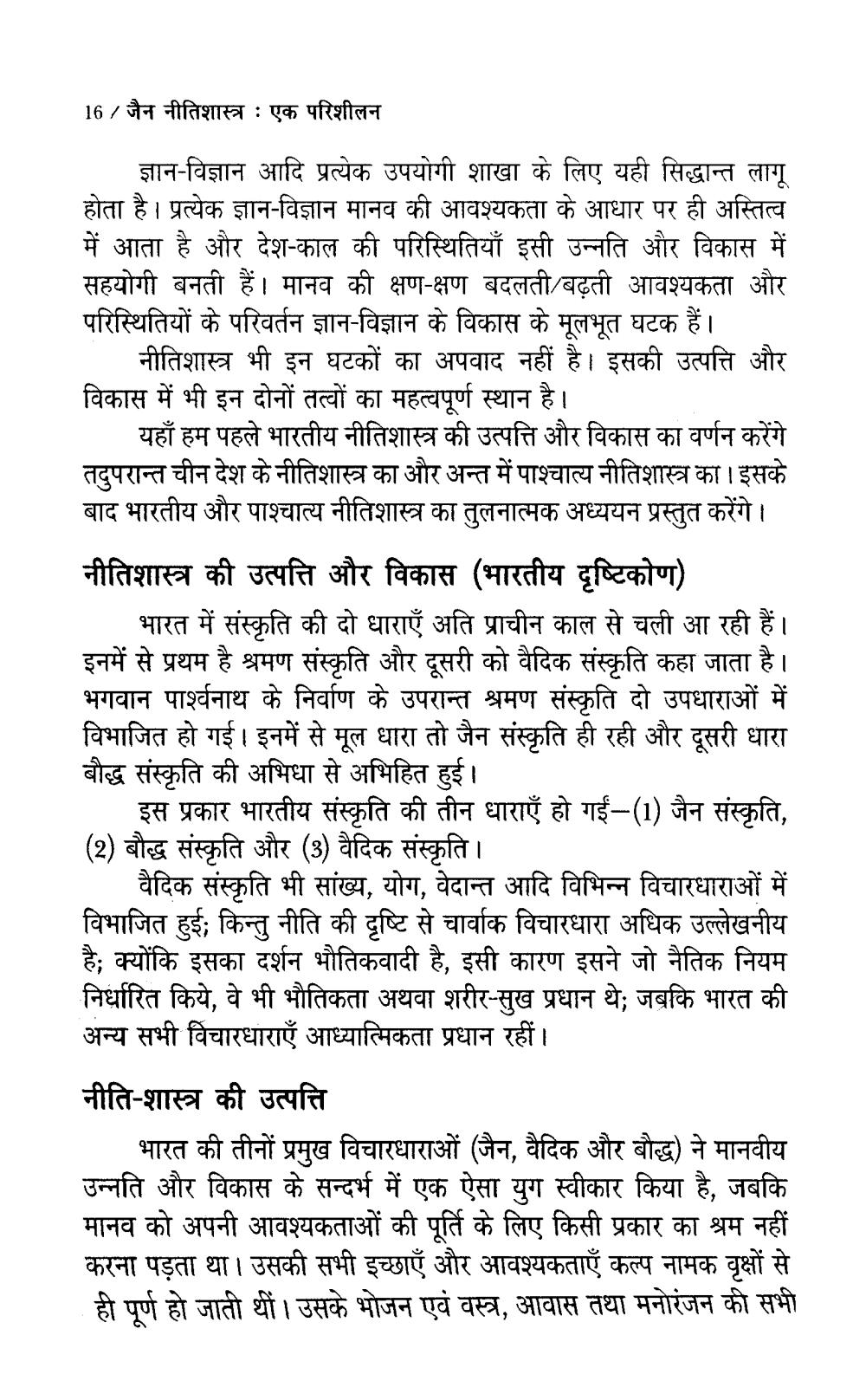________________
16 / जैन नीतिशास्त्र : एक परिशीलन
__ ज्ञान-विज्ञान आदि प्रत्येक उपयोगी शाखा के लिए यही सिद्धान्त लागू होता है। प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान मानव की आवश्यकता के आधार पर ही अस्तित्व में आता है और देश-काल की परिस्थितियाँ इसी उन्नति और विकास में सहयोगी बनती हैं। मानव की क्षण-क्षण बदलती/बढ़ती आवश्यकता और परिस्थितियों के परिवर्तन ज्ञान-विज्ञान के विकास के मूलभूत घटक हैं।
नीतिशास्त्र भी इन घटकों का अपवाद नहीं है। इसकी उत्पत्ति और विकास में भी इन दोनों तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है।
यहाँ हम पहले भारतीय नीतिशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करेंगे तदुपरान्त चीन देश के नीतिशास्त्र का और अन्त में पाश्चात्य नीतिशास्त्र का। इसके बाद भारतीय और पाश्चात्य नीतिशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति और विकास (भारतीय दृष्टिकोण)
भारत में संस्कृति की दो धाराएँ अति प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इनमें से प्रथम है श्रमण संस्कृति और दूसरी को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के उपरान्त श्रमण संस्कृति दो उपधाराओं में विभाजित हो गई। इनमें से मूल धारा तो जैन संस्कृति ही रही और दूसरी धारा बौद्ध संस्कृति की अभिधा से अभिहित हई।
इस प्रकार भारतीय संस्कृति की तीन धाराएँ हो गईं-(1) जैन संस्कृति, (2) बौद्ध संस्कृति और (3) वैदिक संस्कृति।
वैदिक संस्कृति भी सांख्य, योग, वेदान्त आदि विभिन्न विचारधाराओं में विभाजित हुई; किन्तु नीति की दृष्टि से चार्वाक विचारधारा अधिक उल्लेखनीय है; क्योंकि इसका दर्शन भौतिकवादी है, इसी कारण इसने जो नैतिक नियम निर्धारित किये, वे भी भौतिकता अथवा शरीर-सुख प्रधान थे; जबकि भारत की अन्य सभी विचारधाराएँ आध्यात्मिकता प्रधान रहीं। नीति-शास्त्र की उत्पत्ति
भारत की तीनों प्रमुख विचारधाराओं (जैन, वैदिक और बौद्ध) ने मानवीय उन्नति और विकास के सन्दर्भ में एक ऐसा युग स्वीकार किया है, जबकि मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता था। उसकी सभी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ कल्प नामक वृक्षों से ही पूर्ण हो जाती थी। उसके भोजन एवं वस्त्र, आवास तथा मनोरंजन की सभी