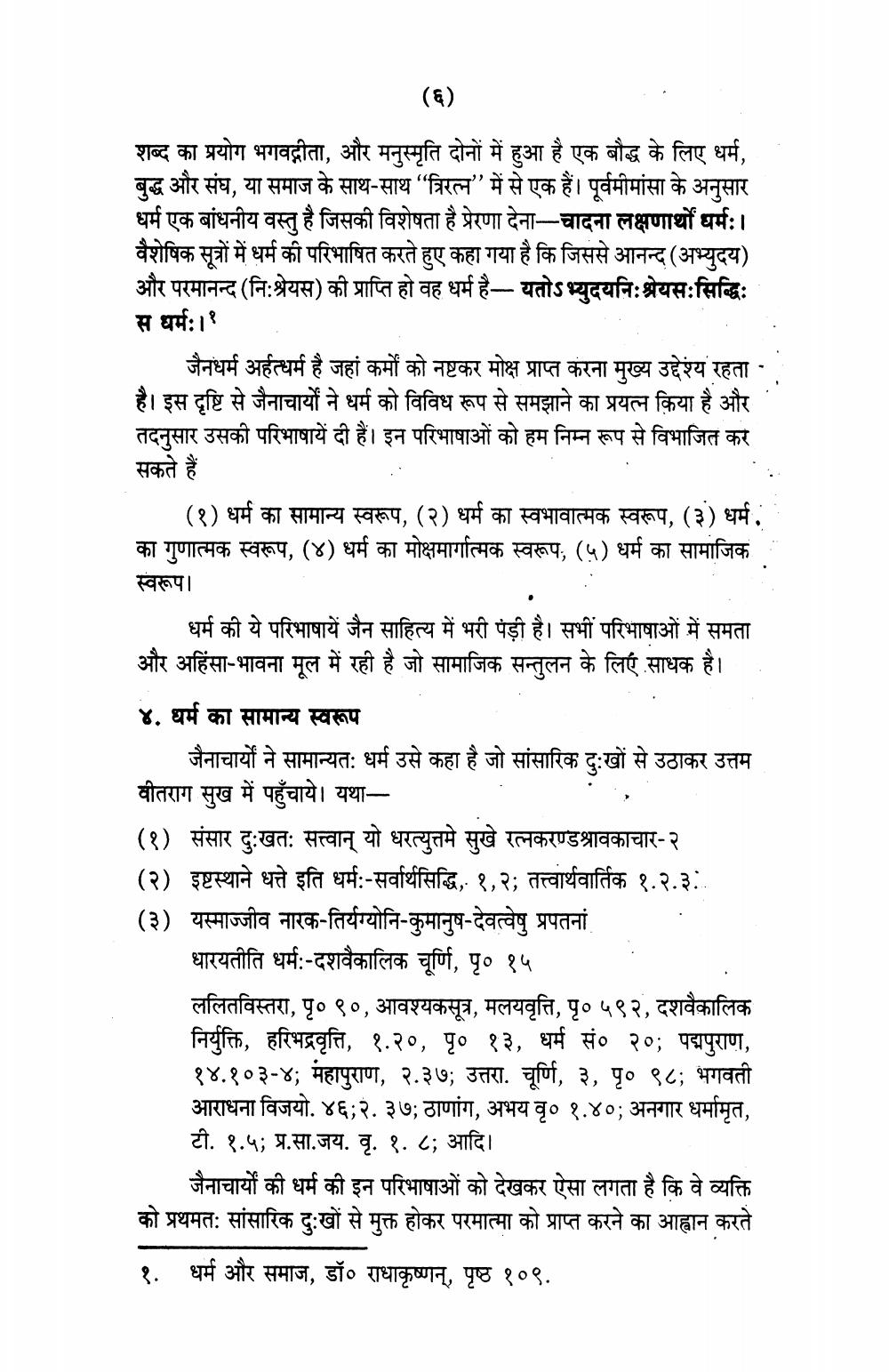________________
(६)
शब्द का प्रयोग भगवद्गीता, और मनुस्मृति दोनों में हुआ है एक बौद्ध के लिए धर्म, बुद्ध और संघ, या समाज के साथ-साथ “त्रिरत्न' में से एक हैं। पूर्वमीमांसा के अनुसार धर्म एक बांधनीय वस्तु है जिसकी विशेषता है प्रेरणा देना-चादना लक्षणार्थों धर्मः। वैशेषिक सूत्रों में धर्म की परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिससे आनन्द (अभ्युदय) और परमानन्द (निःश्रेयस) की प्राप्ति हो वह धर्म है- यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसःसिद्धिः स धर्मः।
जैनधर्म अर्हत्धर्म है जहां कर्मों को नष्टकर मोक्ष प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य रहता । है। इस दृष्टि से जैनाचार्यों ने धर्म को विविध रूप से समझाने का प्रयत्न किया है और तदनुसार उसकी परिभाषायें दी हैं। इन परिभाषाओं को हम निम्न रूप से विभाजित कर सकते हैं
(१) धर्म का सामान्य स्वरूप, (२) धर्म का स्वभावात्मक स्वरूप, (३) धर्म. का गुणात्मक स्वरूप, (४) धर्म का मोक्षमार्गात्मक स्वरूप, (५) धर्म का सामाजिक स्वरूप।
धर्म की ये परिभाषायें जैन साहित्य में भरी पड़ी है। सभी परिभाषाओं में समता और अहिंसा-भावना मूल में रही है जो सामाजिक सन्तुलन के लिए साधक है। ४. धर्म का सामान्य स्वरूप
जैनाचार्यों ने सामान्यत: धर्म उसे कहा है जो सांसारिक दुःखों से उठाकर उत्तम वीतराग सुख में पहुँचाये। यथा(१) संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे रत्नकरण्डश्रावकाचार-२ (२) इष्टस्थाने धत्ते इति धर्म:-सर्वार्थसिद्धि, १,२; तत्त्वार्थवार्तिक १.२.३. (३) यस्माज्जीव नारक-तिर्यग्योनि-कुमानुष-देवत्वेषु प्रपतनां
धारयतीति धर्म:-दशवैकालिक चूर्णि, पृ० १५ ललितविस्तरा, पृ० ९०, आवश्यकसूत्र, मलयवृत्ति, पृ० ५९२, दशवैकालिक नियुक्ति, हरिभद्रवृत्ति, १.२०, पृ० १३, धर्म सं० २०; पद्मपुराण, १४.१०३-४; महापुराण, २.३७; उत्तरा. चूर्णि, ३, पृ० ९८; भगवती आराधना विजयो. ४६,२. ३७; ठाणांग, अभय वृ० १.४०; अनगार धर्मामृत, टी. १.५; प्र.सा.जय. वृ. १. ८; आदि।
जैनाचार्यों की धर्म की इन परिभाषाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे व्यक्ति को प्रथमत: सांसारिक दुःखों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करने का आह्वान करते १. धर्म और समाज, डॉ० राधाकृष्णन्, पृष्ठ १०९.