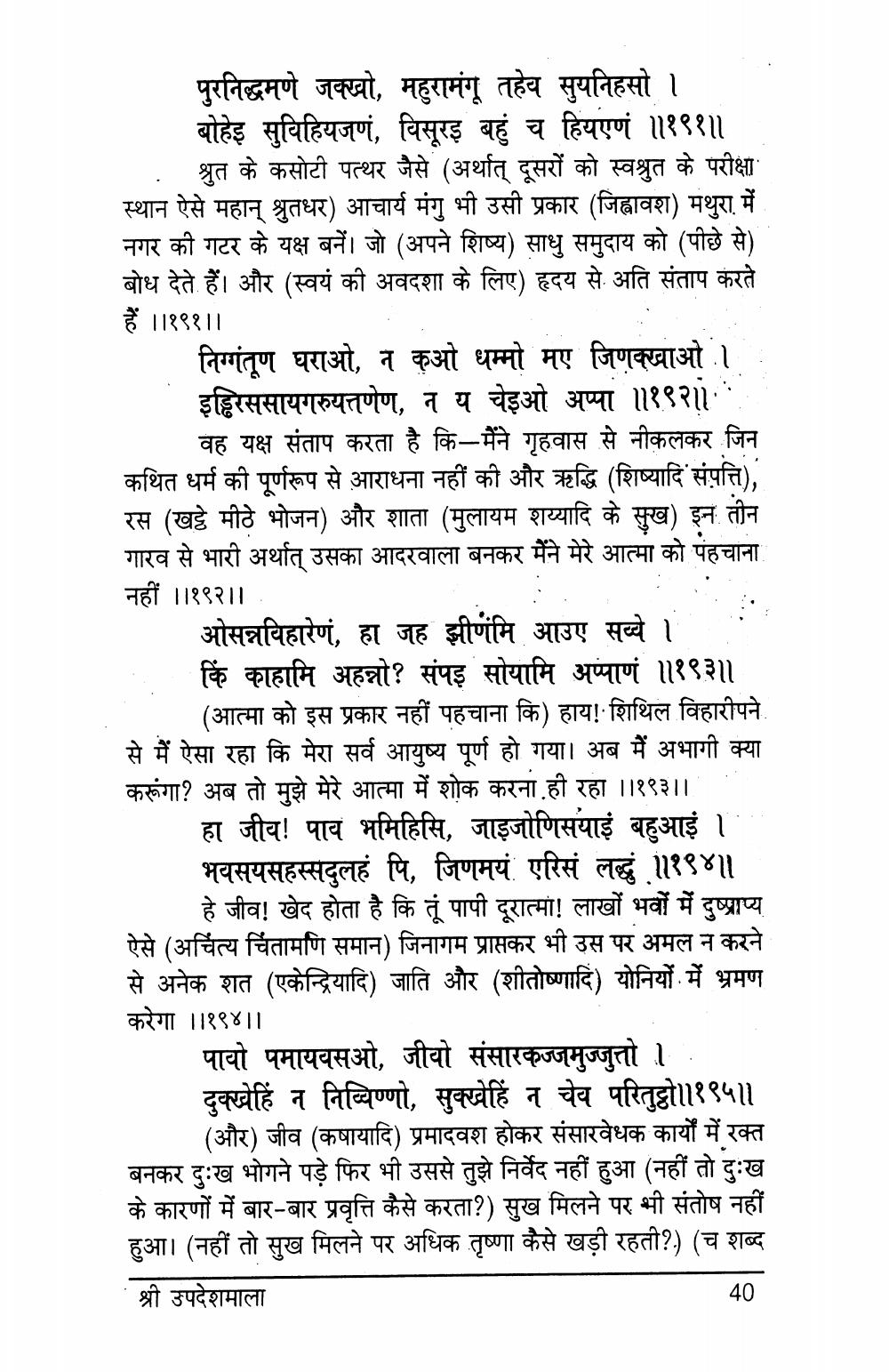________________
पुरनिद्धमणे जक्खो, महुरामंगू तहेव सुयनिहसो ।
बोहेइ सुविहियजणं, विसूरइ बहुं च हियएणं ॥१९१॥ . श्रुत के कसोटी पत्थर जैसे (अर्थात् दूसरों को स्वश्रुत के परीक्षा स्थान ऐसे महान् श्रुतधर) आचार्य मंगु भी उसी प्रकार (जिह्वावश) मथुरा में नगर की गटर के यक्ष बनें। जो (अपने शिष्य) साधु समुदाय को (पीछे से) बोध देते हैं। और (स्वयं की अवदशा के लिए) हृदय से अति संताप करते हैं ।।१९१।।
निग्गंतूण घराओ, न कुओ धम्मो मए जिणक्खाओ । इड्डिरससायगरुयत्तणेण, न य चेइओ अप्पा ॥१९२॥
वह यक्ष संताप करता है कि मैंने गृहवास से नीकलकर जिन कथित धर्म की पूर्णरूप से आराधना नहीं की और ऋद्धि (शिष्यादि संपत्ति), रस (खट्टे मीठे भोजन) और शाता (मुलायम शय्यादि के सुख) इन तीन गारव से भारी अर्थात् उसका आदरवाला बनकर मैंने मेरे आत्मा को पहचाना नहीं ।।१९२।।
ओसन्नविहारेणं, हा जह झीणंमि आउए सब्वे । किं काहामि अहन्नो? संपड़ सोयामि अप्पाणं ॥१९३॥
(आत्मा को इस प्रकार नहीं पहचाना कि) हाय! शिथिल विहारीपने से मैं ऐसा रहा कि मेरा सर्व आयुष्य पूर्ण हो गया। अब मैं अभागी क्या करूंगा? अब तो मुझे मेरे आत्मा में शोक करना ही रहा ।।१९३।।
हा जीव! पाव भमिहिसि, जाइजोणिसयाई बहुआई ।। भवसयसहस्सदुलहं पि, जिणमयं एरिसं लद्धं ॥१९४॥
हे जीव! खेद होता है कि तूं पापी दुरात्मा! लाखों भवों में दुष्प्राप्य ऐसे (अचिंत्य चिंतामणि समान) जिनागम प्राप्तकर भी उस पर अमल न करने से अनेक शत (एकेन्द्रियादि) जाति और (शीतोष्णादि) योनियों में भ्रमण करेगा ।।१९४।।
पायो पमायवसओ, जीवो संसारकज्जमुज्जुत्तो । . दुक्नेहिं न निविण्णो, सुक्नेहिं न चेव परितुट्ठो॥१९५॥
(और) जीव (कषायादि) प्रमादवश होकर संसारवेधक कार्यों में रक्त बनकर दुःख भोगने पड़े फिर भी उससे तुझे निर्वेद नहीं हुआ (नहीं तो दुःख के कारणों में बार-बार प्रवृत्ति कैसे करता?) सुख मिलने पर भी संतोष नहीं हुआ। (नहीं तो सुख मिलने पर अधिक तृष्णा कैसे खड़ी रहती?.) (च शब्द श्री उपदेशमाला
4