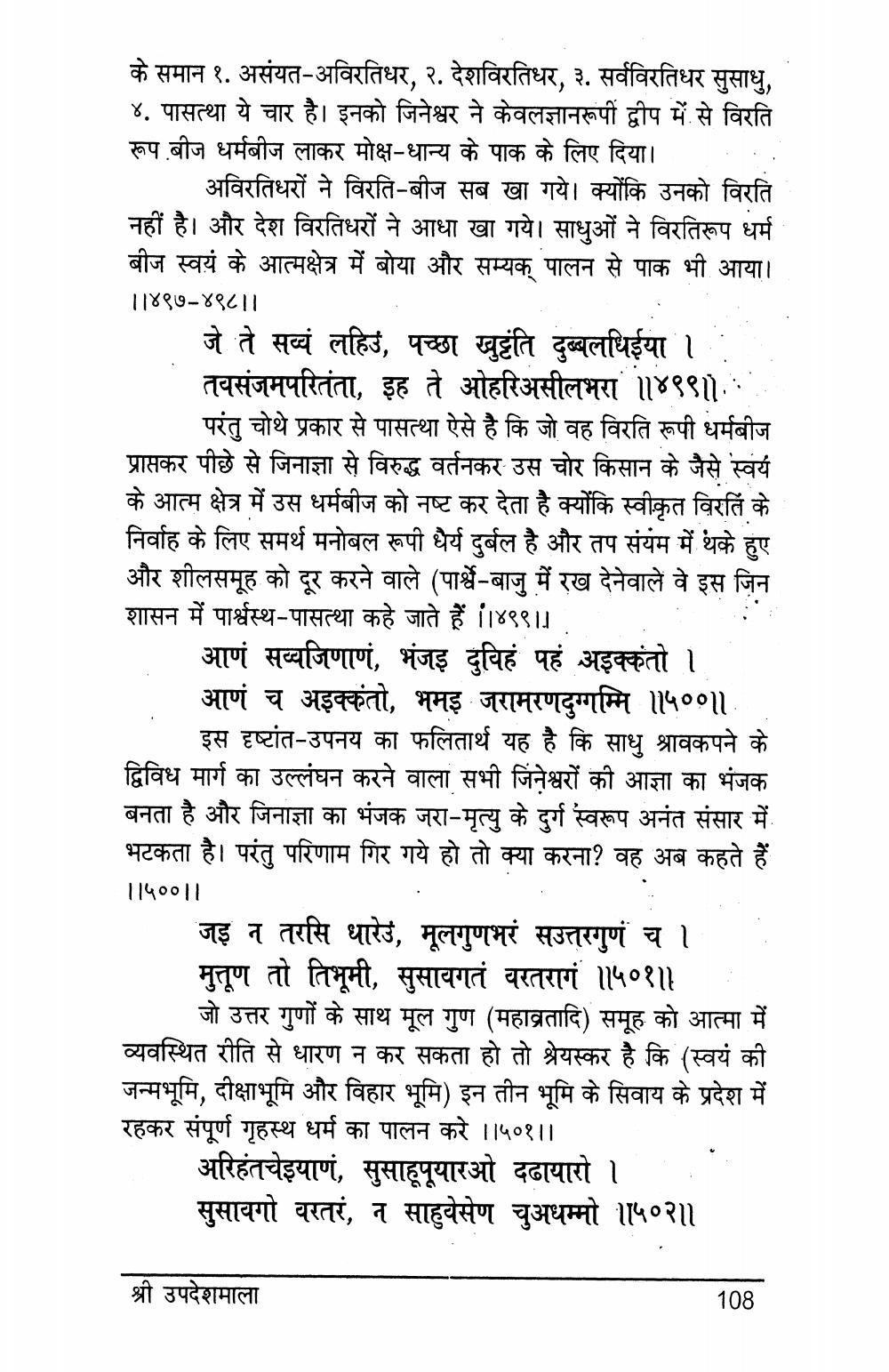________________
के समान १. असंयत-अविरतिधर, २. देशविरतिधर, ३. सर्वविरतिधर सुसाधु, ४. पासत्था ये चार है। इनको जिनेश्वर ने केवलज्ञानरूपी द्वीप में से विरति रूप बीज धर्मबीज लाकर मोक्ष-धान्य के पाक के लिए दिया।
अविरतिधरों ने विरति-बीज सब खा गये। क्योंकि उनको विरति नहीं है। और देश विरतिधरों ने आधा खा गये। साधुओं ने विरतिरूप धर्म बीज स्वयं के आत्मक्षेत्र में बोया और सम्यक् पालन से पाक भी आया। ।।४९७-४९८।।
जे ते सव्वं लहिउँ, पच्छा खुटुंति दुब्बलधिईया । तवसंजमपरितंता, इह ते ओहरिअसीलभरा ॥४९९॥
परंतु चोथे प्रकार से पासत्था ऐसे है कि जो वह विरति रूपी धर्मबीज प्राप्तकर पीछे से जिनाज्ञा से विरुद्ध वर्तनकर उस चोर किसान के जैसे स्वयं के आत्म क्षेत्र में उस धर्मबीज को नष्ट कर देता है क्योंकि स्वीकृत विरतिं के निर्वाह के लिए समर्थ मनोबल रूपी धैर्य दुर्बल है और तप संयम में थके हुए
और शीलसमूह को दूर करने वाले (पार्श्वे-बाजु में रख देनेवाले वे इस जिन शासन में पार्श्वस्थ-पासत्था कहे जाते हैं ।।४९९।।
आणं सव्यजिणाणं, भंजड़ दुविहं पहं अइक्कतो । आणं च अइक्कंतो, भमइ जरामरणदुग्गम्मि ॥५००॥
इस दृष्टांत-उपनय का फलितार्थ यह है कि साधु श्रावकपने के द्विविध मार्ग का उल्लंघन करने वाला सभी जिनेश्वरों की आज्ञा का भंजक बनता है और जिनाज्ञा का भंजक जरा-मृत्यु के दुर्ग स्वरूप अनंत संसार में भटकता है। परंतु परिणाम गिर गये हो तो क्या करना? वह अब कहते हैं ।।५००||
जड़ न तरसि धारेउं, मूलगुणभरं सउत्तरगुणं च । मुत्तूण तो तिभूमी, सुसावगतं वरतरागं ॥५०१॥
जो उत्तर गुणों के साथ मूल गुण (महाव्रतादि) समूह को आत्मा में व्यवस्थित रीति से धारण न कर सकता हो तो श्रेयस्कर है कि (स्वयं की जन्मभूमि, दीक्षाभूमि और विहार भूमि) इन तीन भूमि के सिवाय के प्रदेश में रहकर संपूर्ण गृहस्थ धर्म का पालन करे ।।५०१।।
अरिहंतचेइयाणं, सुसाहूपूयारओ दढायारो । सुसावगो वरतरं, न साहुवेसेण चुअधम्मो ५०२॥
श्री उपदेशमाला
108