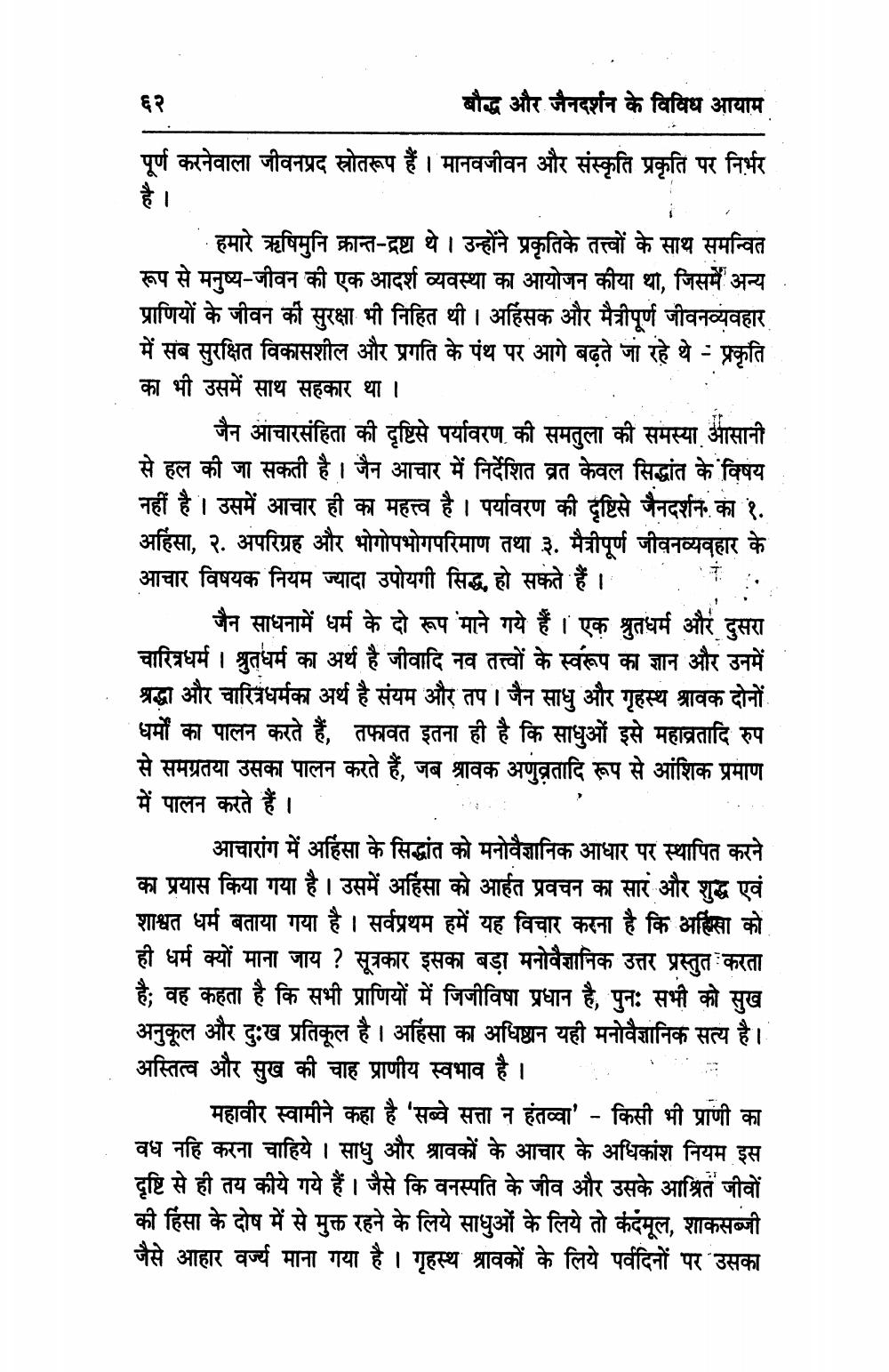________________
बौद्ध और जैनदर्शन के विविध आयाम पूर्ण करनेवाला जीवनप्रद स्रोतरूप हैं । मानवजीवन और संस्कृति प्रकृति पर निर्भर
हमारे ऋषिमुनि क्रान्त-द्रष्टा थे। उन्होंने प्रकृतिके तत्त्वों के साथ समन्वित रूप से मनुष्य-जीवन की एक आदर्श व्यवस्था का आयोजन कीया था, जिसमें अन्य प्राणियों के जीवन की सुरक्षा भी निहित थी । अहिंसक और मैत्रीपूर्ण जीवनव्यवहार में सब सुरक्षित विकासशील और प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ते जा रहे थे - प्रकृति का भी उसमें साथ सहकार था ।
जैन आचारसंहिता की दृष्टि से पर्यावरण की समतुला की समस्या आसानी से हल की जा सकती है। जैन आचार में निर्देशित व्रत केवल सिद्धांत के विषय नहीं है। उसमें आचार ही का महत्त्व है। पर्यावरण की दृष्टिसे जैनदर्शन का १. अहिंसा, २. अपरिग्रह और भोगोपभोगपरिमाण तथा ३. मैत्रीपूर्ण जीवनव्यवहार के आचार विषयक नियम ज्यादा उपोयगी सिद्ध हो सकते हैं।
जैन साधनामें धर्म के दो रूप माने गये हैं । एक श्रुतधर्म और दुसरा चारित्रधर्म । श्रुतधर्म का अर्थ है जीवादि नव तत्त्वों के स्वरूप का ज्ञान और उनमें श्रद्धा और चारित्रधर्मका अर्थ है संयम और तप । जैन साधु और गृहस्थ श्रावक दोनों धर्मों का पालन करते हैं, तफावत इतना ही है कि साधुओं इसे महाव्रतादि रुप से समग्रतया उसका पालन करते हैं, जब श्रावक अणुव्रतादि रूप से आंशिक प्रमाण में पालन करते हैं।
आचारांग में अहिंसा के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसमें अहिंसा को आहत प्रवचन का सारं और शुद्ध एवं शाश्वत धर्म बताया गया है । सर्वप्रथम हमें यह विचार करना है कि अहिंसा को ही धर्म क्यों माना जाय ? सूत्रकार इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रस्तुत करता है; वह कहता है कि सभी प्राणियों में जिजीविषा प्रधान है, पुनः सभी को सुख अनुकूल और दुःख प्रतिकूल है। अहिंसा का अधिष्ठान यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। अस्तित्व और सुख की चाह प्राणीय स्वभाव है।
___ महावीर स्वामीने कहा है 'सब्वे सत्ता न हंतव्वा' - किसी भी प्राणी का वध नहि करना चाहिये । साधु और श्रावकों के आचार के अधिकांश नियम इस दृष्टि से ही तय कीये गये हैं। जैसे कि वनस्पति के जीव और उसके आश्रितं जीवों की हिंसा के दोष में से मुक्त रहने के लिये साधुओं के लिये तो कंदमूल, शाकसब्जी जैसे आहार वर्ण्य माना गया है । गृहस्थ श्रावकों के लिये पर्वदिनों पर उसका