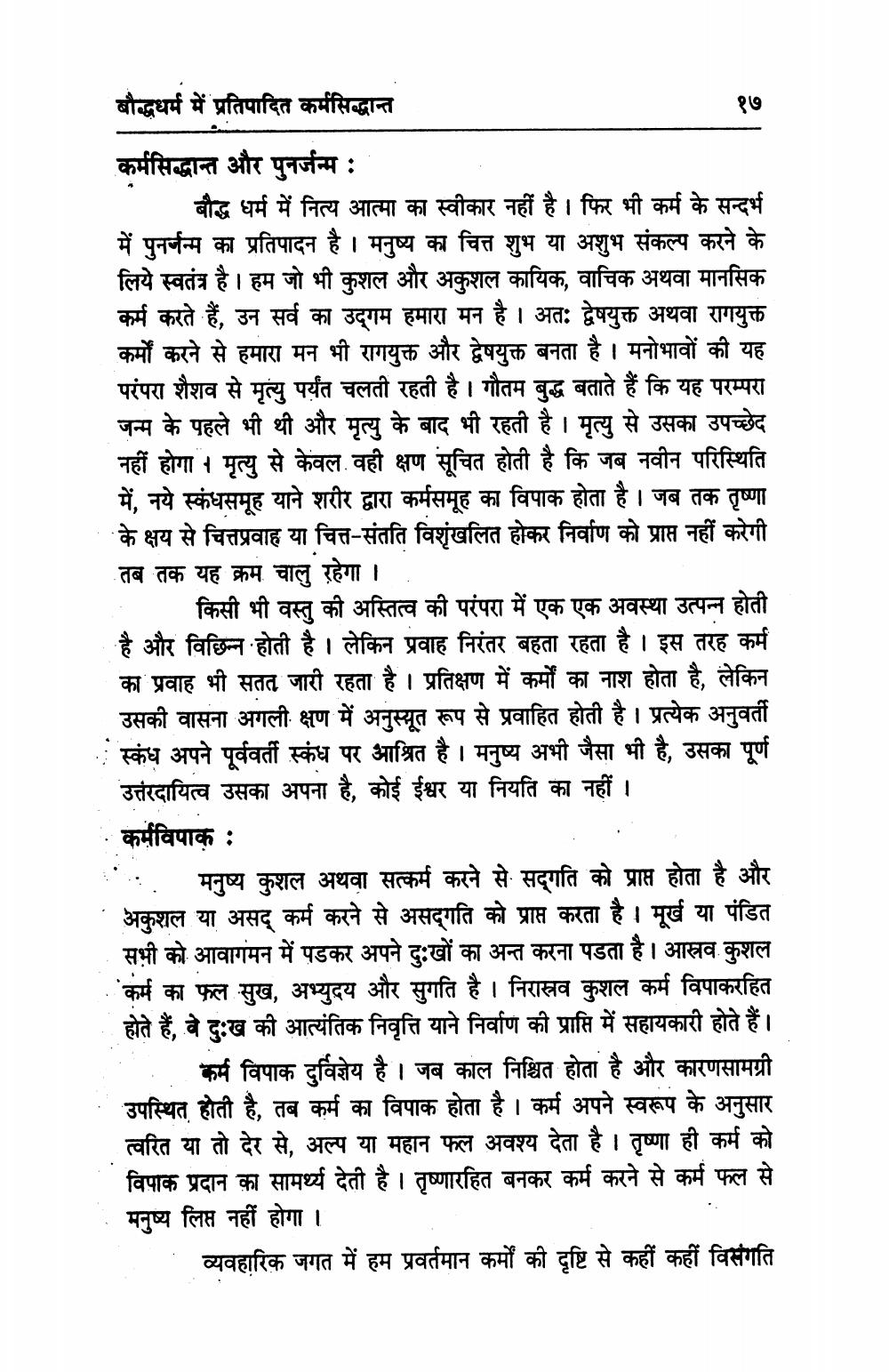________________
बौद्धधर्म में प्रतिपादित कर्मसिद्धान्त कर्मसिद्धान्त और पुनर्जन्म :
बौद्ध धर्म में नित्य आत्मा का स्वीकार नहीं है। फिर भी कर्म के सन्दर्भ में पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। मनुष्य का चित्त शुभ या अशुभ संकल्प करने के लिये स्वतंत्र है। हम जो भी कुशल और अकुशल कायिक, वाचिक अथवा मानसिक कर्म करते हैं, उन सर्व का उद्गम हमारा मन है । अतः द्वेषयुक्त अथवा रागयुक्त कर्मों करने से हमारा मन भी रागयुक्त और द्वेषयुक्त बनता है । मनोभावों की यह परंपरा शैशव से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि यह परम्परा जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है । मृत्यु से उसका उपच्छेद नहीं होगा । मृत्यु से केवल. वही क्षण सूचित होती है कि जब नवीन परिस्थिति में, नये स्कंधसमूह याने शरीर द्वारा कर्मसमूह का विपाक होता है । जब तक तृष्णा के क्षय से चित्तप्रवाह या चित्त-संतति विशृंखलित होकर निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगी तब तक यह क्रम चालु रहेगा।
किसी भी वस्तु की अस्तित्व की परंपरा में एक एक अवस्था उत्पन्न होती है और विछिन्न होती है। लेकिन प्रवाह निरंतर बहता रहता है । इस तरह कर्म का प्रवाह भी सतत जारी रहता है । प्रतिक्षण में कर्मों का नाश होता है, लेकिन
उसकी वासना अगली. क्षण में अनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। प्रत्येक अनुवर्ती . स्कंध अपने पूर्ववर्ती स्कंध पर आश्रित है । मनुष्य अभी जैसा भी है, उसका पूर्ण
उत्तरदायित्व उसका अपना है, कोई ईश्वर या नियति का नहीं । कर्मविपाक: .:. मनुष्य कुशल अथवा सत्कर्म करने से सद्गति को प्राप्त होता है और
अकुशल या असद् कर्म करने से असद्गति को प्राप्त करता है । मूर्ख या पंडित सभी को आवागमन में पडकर अपने दुःखों का अन्त करना पडता है। आस्रव कुशल कर्म का फल सुख, अभ्युदय और सुगति है । निरास्रव कुशल कर्म विपाकरहित होते हैं, वे दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति याने निर्वाण की प्राप्ति में सहायकारी होते हैं।
. कर्म विपाक दुर्विज्ञेय है । जब काल निश्चित होता है और कारणसामग्री उपस्थित होती है, तब कर्म का विपाक होता है। कर्म अपने स्वरूप के अनुसार त्वरित या तो देर से, अल्प या महान फल अवश्य देता है । तृष्णा ही कर्म को विपाक प्रदान का सामर्थ्य देती है । तृष्णारहित बनकर कर्म करने से कर्म फल से मनुष्य लिप्त नहीं होगा।
व्यवहारिक जगत में हम प्रवर्तमान कर्मों की दृष्टि से कहीं कहीं विसंगति