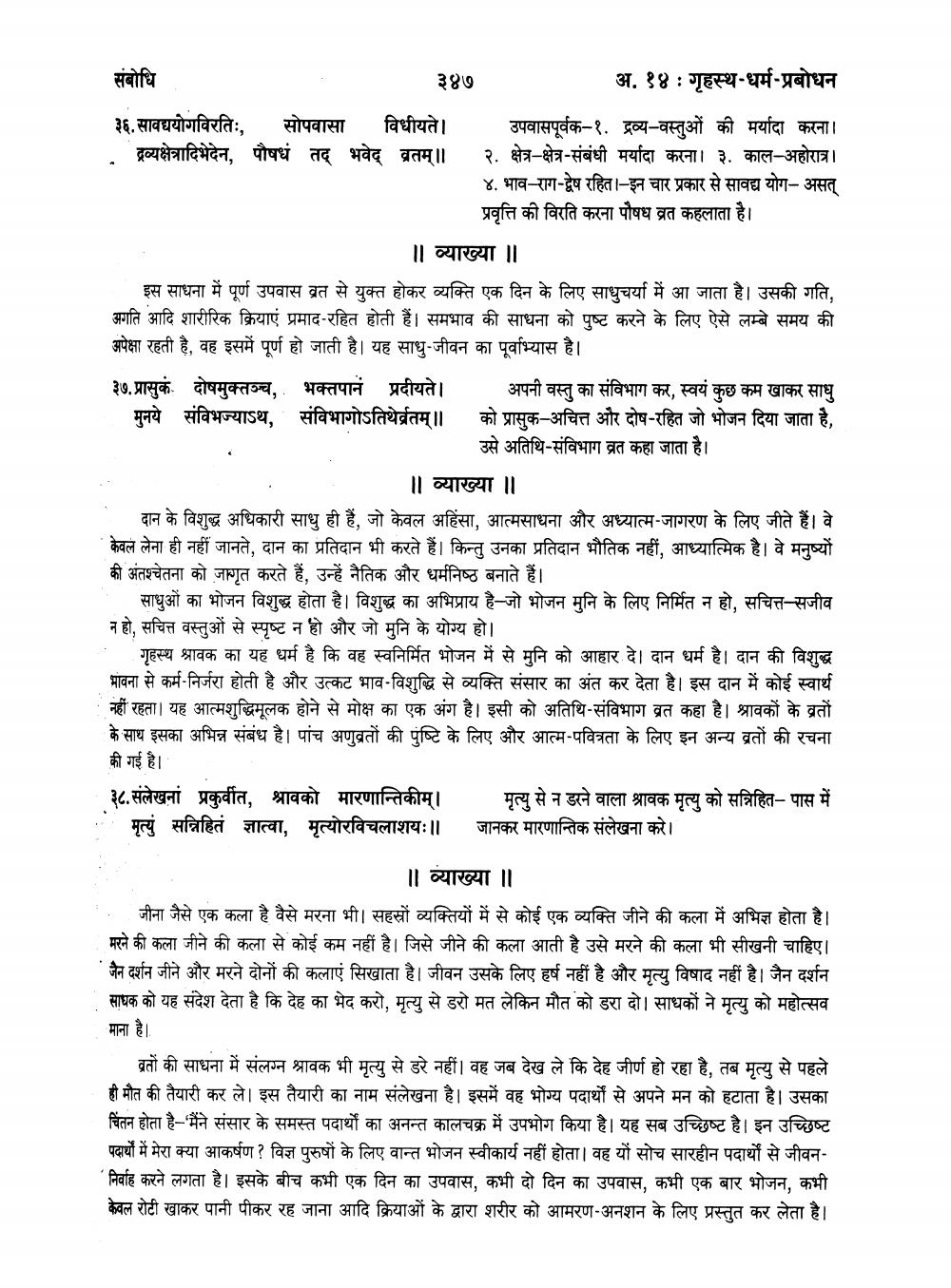________________
संबोधि
३४७
अ. १४ : गृहस्थ-धर्म-प्रबोधन ३६. सावद्ययोगविरतिः, सोपवासा विधीयते। उपवासपूर्वक-१. द्रव्य-वस्तुओं की मर्यादा करना। . द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन, पौषधं तद् भवेद् व्रतम्॥ २. क्षेत्र-क्षेत्र-संबंधी मर्यादा करना। ३. काल-अहोरात्र ।
४. भाव-राग-द्वेष रहित।-इन चार प्रकार से सावध योग-असत्
प्रवृत्ति की विरति करना पौषध व्रत कहलाता है।
॥ व्याख्या ॥ इस साधना में पूर्ण उपवास व्रत से युक्त होकर व्यक्ति एक दिन के लिए साधुचर्या में आ जाता है। उसकी गति, अगति आदि शारीरिक क्रियाएं प्रमाद-रहित होती हैं। समभाव की साधना को पुष्ट करने के लिए ऐसे लम्बे समय की अपेक्षा रहती है, वह इसमें पूर्ण हो जाती है। यह साधु-जीवन का पूर्वाभ्यास है।
३७.प्रासकं. दोषमुक्तञ्च, भक्तपानं प्रदीयते। ___ मुनये संविभज्याऽथ, संविभागोऽतिथेव्रतम्॥
अपनी वस्तु का संविभाग कर, स्वयं कुछ कम खाकर साधु को प्रासुक-अचित्त और दोष-रहित जो भोजन दिया जाता है, उसे अतिथि-संविभाग व्रत कहा जाता है।
॥ व्याख्या ॥ दान के विशुद्ध अधिकारी साधु ही हैं, जो केवल अहिंसा, आत्मसाधना और अध्यात्म-जागरण के लिए जीते हैं। वे केवल लेना ही नहीं जानते, दान का प्रतिदान भी करते हैं। किन्तु उनका प्रतिदान भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वे मनुष्यों की अंतश्चेतना को जागृत करते हैं, उन्हें नैतिक और धर्मनिष्ठ बनाते हैं। ___साधुओं का भोजन विशुद्ध होता है। विशुद्ध का अभिप्राय है-जो भोजन मुनि के लिए निर्मित न हो, सचित्त-सजीव न हो, सचित्त वस्तुओं से स्पृष्ट न हो और जो मुनि के योग्य हो।
गृहस्थ श्रावक का यह धर्म है कि वह स्वनिर्मित भोजन में से मुनि को आहार दे। दान धर्म है। दान की विशुद्ध भावना से कर्म-निर्जरा होती है और उत्कट भाव-विशुद्धि से व्यक्ति संसार का अंत कर देता है। इस दान में कोई स्वार्थ नहीं रहता। यह आत्मशुद्धिमूलक होने से मोक्ष का एक अंग है। इसी को अतिथि-संविभाग व्रत कहा है। श्रावकों के व्रतों के साथ इसका अभिन्न संबंध है। पांच अणुव्रतों की पुष्टि के लिए और आत्म-पवित्रता के लिए इन अन्य व्रतों की रचना की गई है। ३८.संलेखनां प्रकुर्वीत, श्रावको मारणान्तिकीम्। मृत्यु से न डरने वाला श्रावक मृत्यु को सन्निहित- पास में - मृत्युं सन्निहितं ज्ञात्वा, मृत्योरविचलाशयः॥ जानकर मारणान्तिक संलेखना करे।
माना हा
॥ व्याख्या ॥ ... जीना जैसे एक कला है वैसे मरना भी। सहस्रों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जीने की कला में अभिज्ञ होता है। मरने की कला जीने की कला से कोई कम नहीं है। जिसे जीने की कला आती है उसे मरने की कला भी सीखनी चाहिए। जैन दर्शन जीने और मरने दोनों की कलाएं सिखाता है। जीवन उसके लिए हर्ष नहीं है और मृत्यु विषाद नहीं है। जैन दर्शन साधक को यह संदेश देता है कि देह का भेद करो, मृत्यु से डरो मत लेकिन मौत को डरा दो। साधकों ने मृत्यु को महोत्सव माना है। ___ व्रतों की साधना में संलग्न श्रावक भी मृत्यु से डरे नहीं। वह जब देख ले कि देह जीर्ण हो रहा है, तब मृत्यु से पहले ही मौत की तैयारी कर ले। इस तैयारी का नाम संलेखना है। इसमें वह भोग्य पदार्थों से अपने मन को हटाता है। उसका चिंतन होता है-'मैंने संसार के समस्त पदार्थों का अनन्त कालचक्र में उपभोग किया है। यह सब उच्छिष्ट है। इन उच्छिष्ट पदार्थों में मेरा क्या आकर्षण ? विज्ञ पुरुषों के लिए वान्त भोजन स्वीकार्य नहीं होता। वह यों सोच सारहीन पदार्थों से जीवन'निर्वाह करने लगता है। इसके बीच कभी एक दिन का उपवास, कभी दो दिन का उपवास, कभी एक बार भोजन, कभी केवल रोटी खाकर पानी पीकर रह जाना आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर को आमरण अनशन के लिए प्रस्तुत कर लेता है।