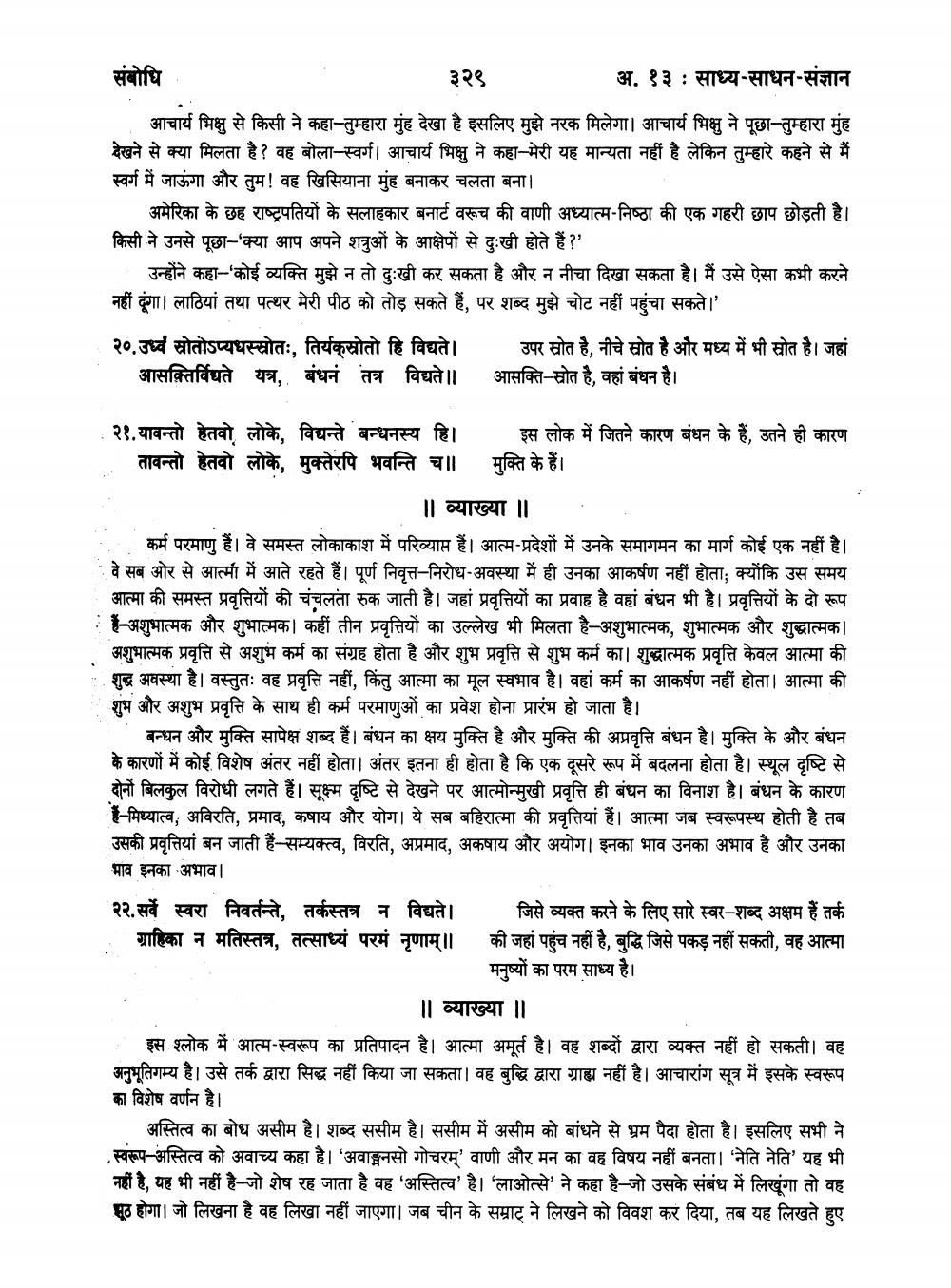________________
संबोधि
३२९
अ. १३ : साध्य-साधन-संज्ञान
. आचार्य भिक्षु से किसी ने कहा-तुम्हारा मुंह देखा है इसलिए मुझे नरक मिलेगा। आचार्य भिक्षु ने पूछा-तुम्हारा मुंह देखने से क्या मिलता है? वह बोला-स्वर्ग। आचार्य भिक्षु ने कहा-मेरी यह मान्यता नहीं है लेकिन तुम्हारे कहने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम! वह खिसियाना मुंह बनाकर चलता बना।
अमेरिका के छह राष्ट्रपतियों के सलाहकार बनार्ट वरूच की वाणी अध्यात्म-निष्ठा की एक गहरी छाप छोड़ती है। किसी ने उनसे पूछा-'क्या आप अपने शत्रुओं के आक्षेपों से दुःखी होते हैं ?'
उन्होंने कहा-'कोई व्यक्ति मुझे न तो दुःखी कर सकता है और न नीचा दिखा सकता है। मैं उसे ऐसा कभी करने नहीं दूंगा। लाठियां तथा पत्थर मेरी पीठ को तोड़ सकते हैं, पर शब्द मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते।'
२०.उध्वं स्रोतोऽप्यधस्स्रोतः, तिर्यकस्रोतो हि विद्यते।
आसक्तिर्विद्यते यत्र, बंधनं तत्र विद्यते॥
उपर स्रोत है, नीचे स्रोत है और मध्य में भी स्रोत है। जहां आसक्ति-स्रोत है, वहां बंधन है।
२१.यावन्तो हेतवो लोके, विद्यन्ते बन्धनस्य हि। इस लोक में जितने कारण बंधन के हैं, उतने ही कारण तावन्तो हेतवो लोके, मुक्तेरपि भवन्ति च॥ मुक्ति के हैं।
॥ व्याख्या ॥ - कर्म परमाणु हैं। वे समस्त लोकाकाश में परिव्याप्त हैं। आत्म-प्रदेशों में उनके समागमन का मार्ग कोई एक नहीं है। - वे सब ओर से आत्मा में आते रहते हैं। पूर्ण निवृत्त-निरोध-अवस्था में ही उनका आकर्षण नहीं होता; क्योंकि उस समय
आत्मा की समस्त प्रवृत्तियों की चंचलता रुक जाती है। जहां प्रवृत्तियों का प्रवाह है वहां बंधन भी है। प्रवृत्तियों के दो रूप : है-अशुभात्मक और शुभात्मक। कहीं तीन प्रवृत्तियों का उल्लेख भी मिलता है-अशुभात्मक, शुभात्मक और शुद्धात्मक।
अशुभात्मक प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का संग्रह होता है और शुभ प्रवृत्ति से शुभ कर्म का। शुद्धात्मक प्रवृत्ति केवल आत्मा की शुद्ध अवस्था है। वस्तुतः वह प्रवृत्ति नहीं, किंतु आत्मा का मूल स्वभाव है। वहां कर्म का आकर्षण नहीं होता। आत्मा की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के साथ ही कर्म परमाणुओं का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है।
बन्धन और मुक्ति सापेक्ष शब्द हैं। बंधन का क्षय मुक्ति है और मुक्ति की अप्रवृत्ति बंधन है। मुक्ति के और बंधन के कारणों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। अंतर इतना ही होता है कि एक दूसरे रूप में बदलना होता है। स्थूल दृष्टि से दोनों बिलकुल विरोधी लगते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति ही बंधन का विनाश है। बंधन के कारण हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये सब बहिरात्मा की प्रवृत्तियां हैं। आत्मा जब स्वरूपस्थ होती है तब उसकी प्रवृत्तियां बन जाती हैं-सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। इनका भाव उनका अभाव है और उनका भाव इनका अभाव। २२.सर्वे स्वरा निवर्तन्ते, तर्कस्तत्र न विद्यते। जिसे व्यक्त करने के लिए सारे स्वर-शब्द अक्षम हैं तर्क ग्राहिका न मतिस्तत्र, तत्साध्यं परमं नृणाम्॥ की जहां पहुंच नहीं है, बुद्धि जिसे पकड़ नहीं सकती, वह आत्मा
मनुष्यों का परम साध्य है।
॥ व्याख्या ॥ इस श्लोक में आत्म-स्वरूप का प्रतिपादन है। आत्मा अमूर्त है। वह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। वह अनुभूतिगम्य है। उसे तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। वह बुद्धि द्वारा ग्राह्य नहीं है। आचारांग सूत्र में इसके स्वरूप का विशेष वर्णन है।
अस्तित्व का बोध असीम है। शब्द ससीम है। ससीम में असीम को बांधने से भ्रम पैदा होता है। इसलिए सभी ने स्वरूप-अस्तित्व को अवाच्य कहा है। 'अवामनसो गोचरम्' वाणी और मन का वह विषय नहीं बनता। 'नेति नेति' यह भी नहीं है, यह भी नहीं है जो शेष रह जाता है वह 'अस्तित्व' है। 'लाओत्से' ने कहा है जो उसके संबंध में लिखूगा तो वह झूठ होगा। जो लिखना है वह लिखा नहीं जाएगा। जब चीन के सम्राट ने लिखने को विवश कर दिया, तब यह लिखते हुए