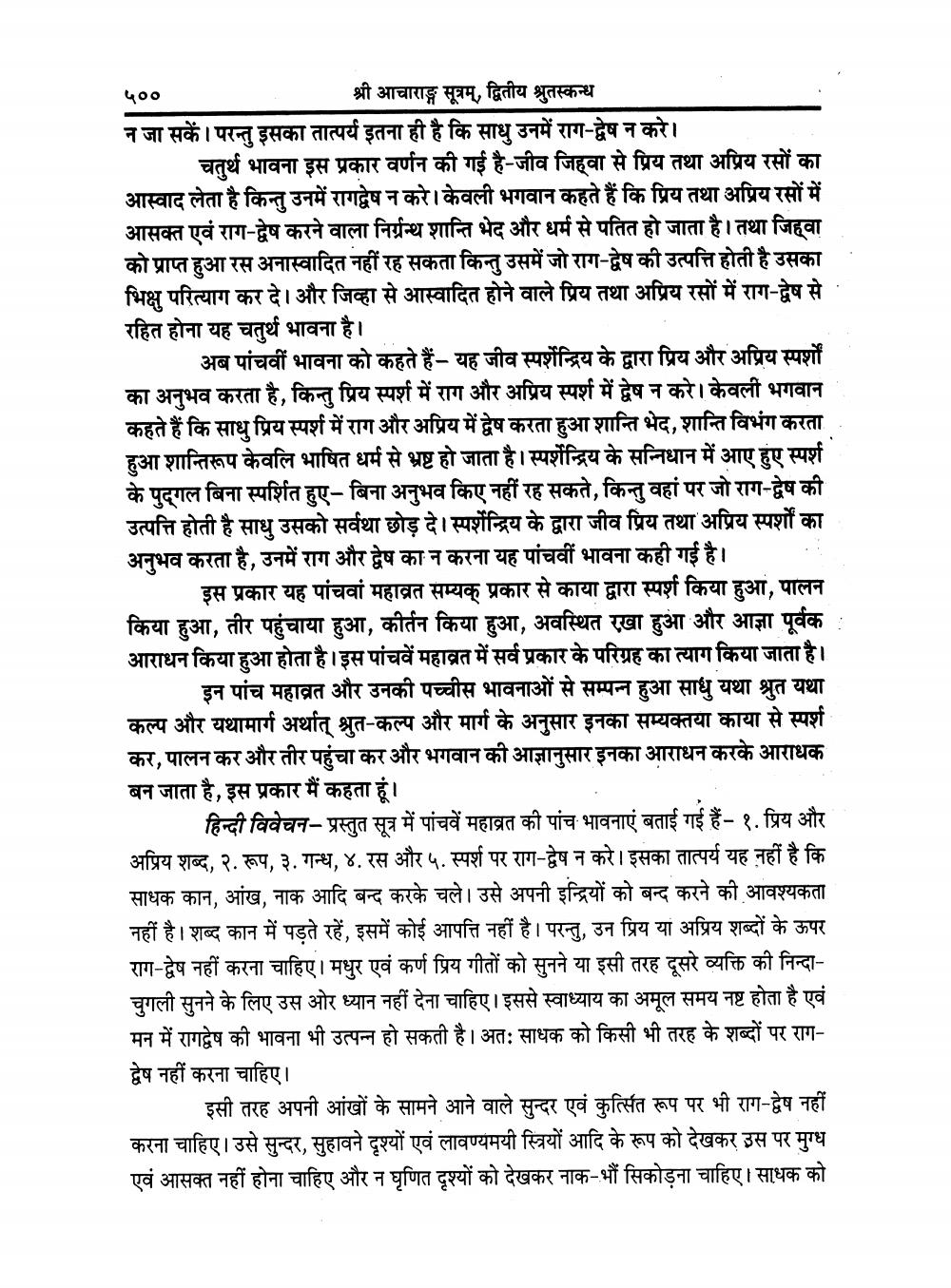________________
५००
श्री आचाराङ्ग सूत्रम्, द्वितीय श्रुतस्कन्ध न जा सकें। परन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि साधु उनमें राग-द्वेष न करे।
चतुर्थ भावना इस प्रकार वर्णन की गई है-जीव जिह्वा से प्रिय तथा अप्रिय रसों का आस्वाद लेता है किन्तु उनमें रागद्वेष न करे।केवली भगवान कहते हैं कि प्रिय तथा अप्रिय रसों में आसक्त एवं राग-द्वेष करने वाला निर्ग्रन्थ शान्ति भेद और धर्म से पतित हो जाता है। तथा जिह्वा को प्राप्त हुआ रस अनास्वादित नहीं रह सकता किन्तु उसमें जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है उसका भिक्षु परित्याग कर दे। और जिव्हा से आस्वादित होने वाले प्रिय तथा अप्रिय रसों में राग-द्वेष से रहित होना यह चतुर्थ भावना है।
अब पांचवीं भावना को कहते हैं- यह जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा प्रिय और अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, किन्तु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय स्पर्श में द्वेष न करे। केवली भगवान कहते हैं कि साधु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय में द्वेष करता हुआ शान्ति भेद,शान्ति विभंग करता हुआ शान्तिरूप केवलि भाषित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। स्पर्शेन्द्रिय के सन्निधान में आए हुए स्पर्श के पुद्गल बिना स्पर्शित हुए- बिना अनुभव किए नहीं रह सकते, किन्तु वहां पर जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है साधु उसको सर्वथा छोड़ दे। स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा जीव प्रिय तथा अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, उनमें राग और द्वेष का न करना यह पांचवीं भावना कही गई है।
इस प्रकार यह पांचवां महाव्रत सम्यक् प्रकार से काया द्वारा स्पर्श किया हुआ, पालन किया हुआ, तीर पहुंचाया हुआ, कीर्तन किया हुआ, अवस्थित रखा हुआ और आज्ञा पूर्वक : आराधन किया हुआ होता है। इस पांचवें महाव्रत में सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग किया जाता है।
इन पांच महाव्रत और उनकी पच्चीस भावनाओं से सम्पन्न हुआ साधु यथा श्रुत यथा कल्प और यथामार्ग अर्थात् श्रुत-कल्प और मार्ग के अनुसार इनका सम्यक्तया काया से स्पर्श कर, पालन कर और तीर पहुंचा कर और भगवान की आज्ञानुसार इनका आराधन करके आराधक बन जाता है, इस प्रकार मैं कहता हूं।
हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में पांचवें महाव्रत की पांच भावनाएं बताई गई हैं- १. प्रिय और अप्रिय शब्द, २. रूप, ३. गन्ध, ४. रस और ५. स्पर्श पर राग-द्वेष न करे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि साधक कान, आंख, नाक आदि बन्द करके चले। उसे अपनी इन्द्रियों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द कान में पड़ते रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, उन प्रिय या अप्रिय शब्दों के ऊपर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। मधुर एवं कर्ण प्रिय गीतों को सुनने या इसी तरह दूसरे व्यक्ति की निन्दाचुगली सुनने के लिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे स्वाध्याय का अमूल समय नष्ट होता है एवं मन में रागद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। अतः साधक को किसी भी तरह के शब्दों पर रागद्वेष नहीं करना चाहिए।
इसी तरह अपनी आंखों के सामने आने वाले सुन्दर एवं कुत्सित रूप पर भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सुन्दर, सुहावने दृश्यों एवं लावण्यमयी स्त्रियों आदि के रूप को देखकर उस पर मुग्ध एवं आसक्त नहीं होना चाहिए और न घृणित दृश्यों को देखकर नाक-भौं सिकोड़ना चाहिए। साधक को