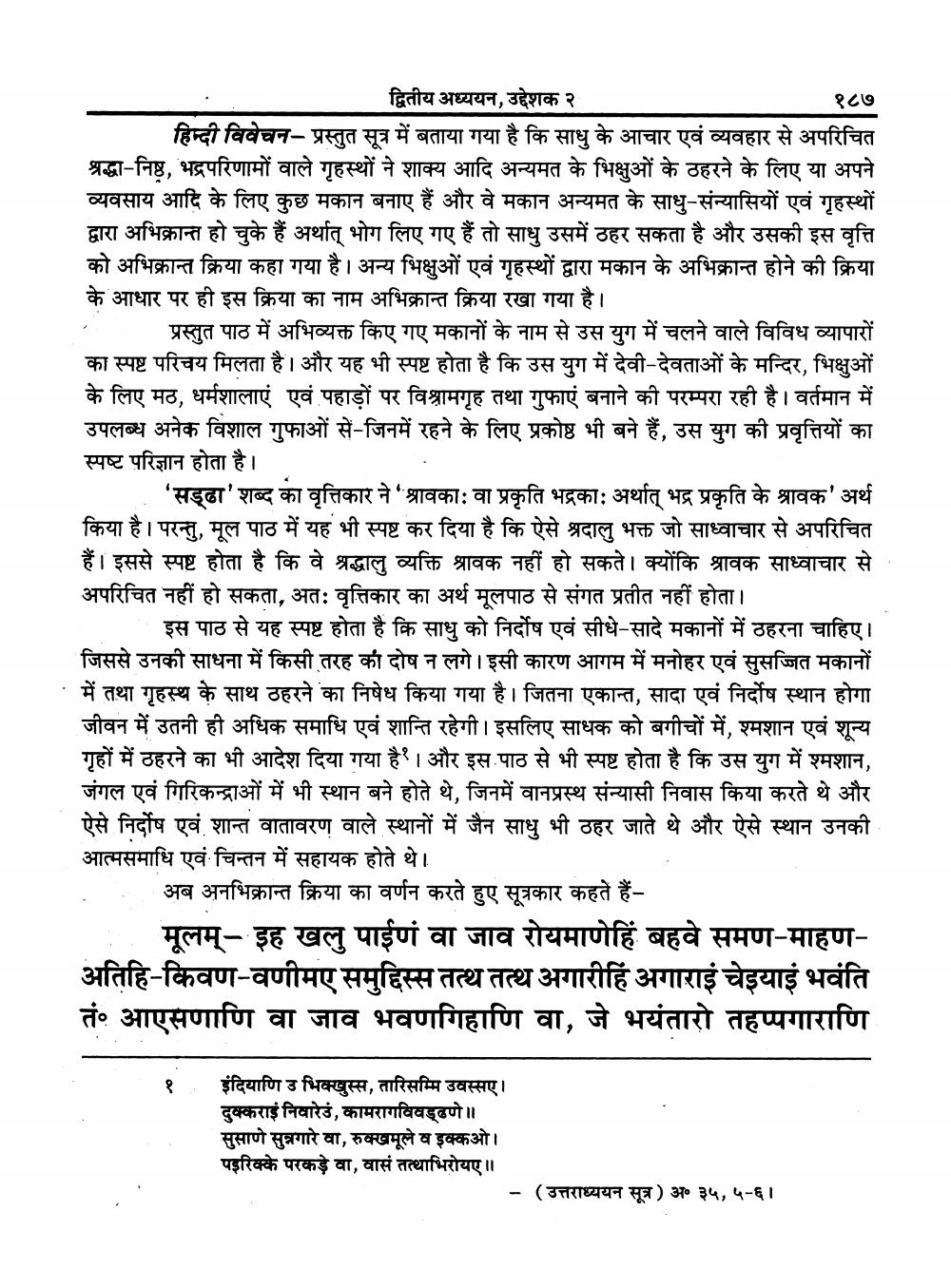________________
द्वितीय अध्ययन, उद्देशक २
१८७
हिन्दी विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु के आचार एवं व्यवहार से अपरिचित श्रद्धा-निष्ठ, भद्रपरिणामों वाले गृहस्थों ने शाक्य आदि अन्यमत के भिक्षुओं के ठहरने के लिए या अपने व्यवसाय आदि के लिए कुछ मकान बनाए हैं और वे मकान अन्यमत के साधु-संन्यासियों एवं गृहस्थों द्वारा अभिक्रान्त हो चुके हैं अर्थात् भोग लिए गए हैं तो साधु उसमें ठहर सकता है और उसकी इस वृत्ति को अभिक्रान्त क्रिया कहा गया है। अन्य भिक्षुओं एवं गृहस्थों द्वारा मकान के अभिक्रान्त होने की क्रिया के आधार पर ही इस क्रिया का नाम अभिक्रान्त क्रिया रखा गया है।
प्रस्तुत पाठ में अभिव्यक्त किए गए मकानों के नाम से उस युग में चलने वाले विविध व्यापारों का स्पष्ट परिचय मिलता है । और यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में देवी-देवताओं के मन्दिर, भिक्षुओं के लिए मठ, धर्मशालाएं एवं पहाड़ों पर विश्रामगृह तथा गुफाएं बनाने की परम्परा रही है। वर्तमान में उपलब्ध अनेक विशाल गुफाओं में जिनमें रहने के लिए प्रकोष्ठ भी बने हैं, उस युग की प्रवृत्तियों का स्पष्ट परिज्ञान होता है।
'सड्ढा' शब्द का वृत्तिकार ने 'श्रावकाः वा प्रकृति भद्रकाः अर्थात् भद्र प्रकृति के श्रावक' अर्थ किया है । परन्तु, मूल पाठ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे श्रदालु भक्त जो साध्वाचार से अपरिचित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे श्रद्धालु व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकते। क्योंकि श्रावक साध्वाचार से अपरिचित नहीं हो सकता, अतः वृत्तिकार का अर्थ मूलपाठ से संगत प्रतीत नहीं होता ।
इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि साधु को निर्दोष एवं सीधे-सादे मकानों में ठहरना चाहिए। जिससे उनकी साधना में किसी तरह की दोष न लगे। इसी कारण आगम में मनोहर एवं सुसज्जित मकानों में तथा गृहस्थ के साथ ठहरने का निषेध किया गया है। जितना एकान्त, सादा एवं निर्दोष स्थान होगा जीवन में उतनी ही अधिक समाधि एवं शान्ति रहेगी। इसलिए साधक को बगीचों में, श्मशान एवं शून्य गृहों में ठहरने का भी आदेश दिया गया है । और इस पाठ से भी स्पष्ट होता है कि उस युग में श्मशान, जंगल एवं गिरिकन्द्राओं में भी स्थान बने होते थे, जिनमें वानप्रस्थ संन्यासी निवास किया करते थे और ऐसे निर्दोष एवं शान्त वातावरण वाले स्थानों में जैन साधु भी ठहर जाते थे और ऐसे स्थान उनकी आत्मसमाधि एवं चिन्तन में सहायक होते थे ।
अब अनभिक्रान्त क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं
मूलम् - इह खलु पाईणं वा जाव रोयमाणेहिं बहवे समण-माहणअतिहि-किवण-वणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराई चेइयाइं भवंति तं. आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराणि
१ इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए । दुक्कराइं निवारेडं, कामरागविवड्ढणे ॥ सुसाणे सुनगारे वा, रुक्खमूले व इक्कओ । परिक्के परकड़े वा, वासं तत्थाभिरोयए ।
(उत्तराध्ययन सूत्र ) अ० ३५, ५-६ ।