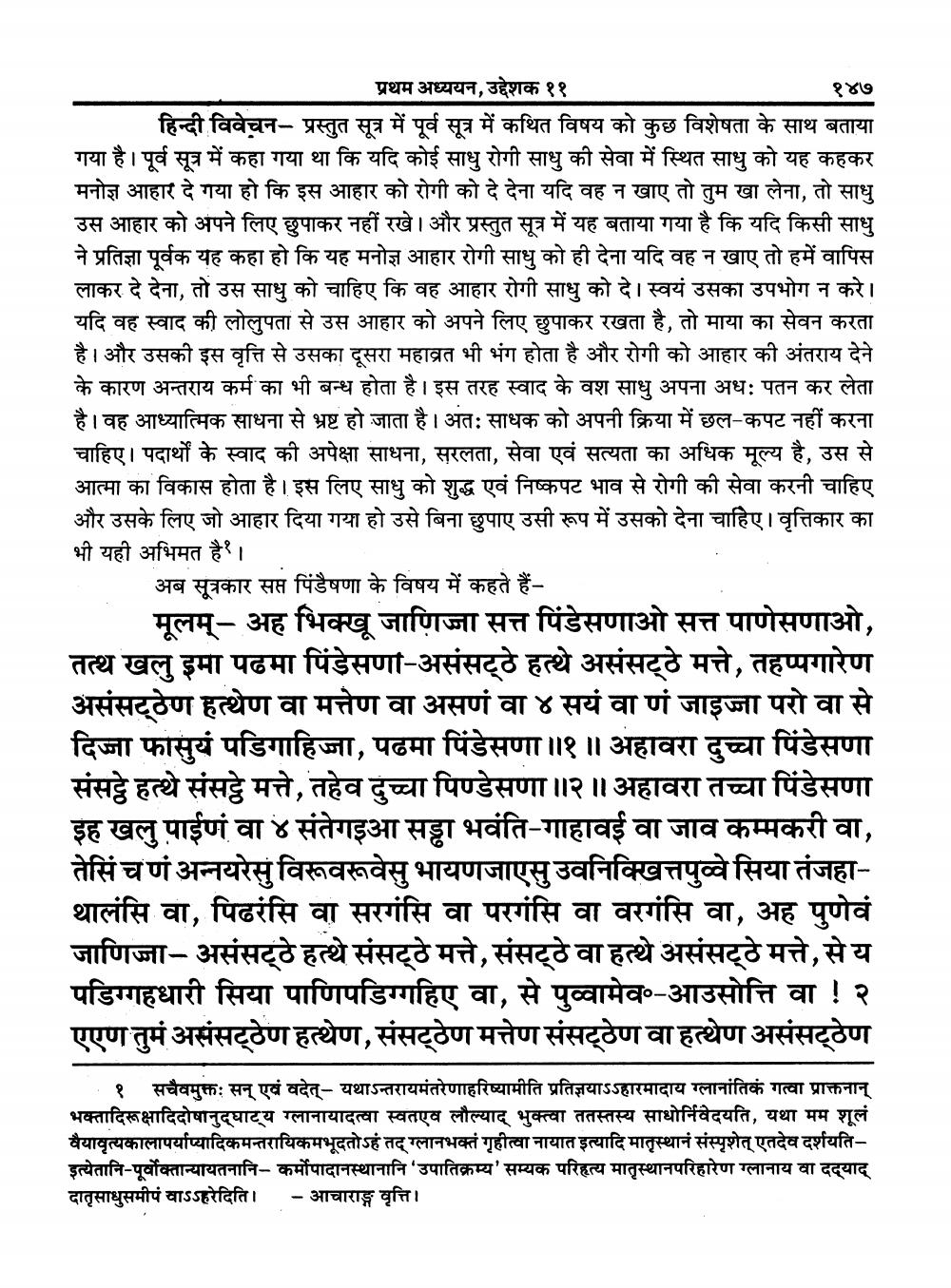________________
१४७
प्रथम अध्ययन, उद्देशक ११ हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में कथित विषय को कुछ विशेषता के साथ बताया गया है। पूर्व सूत्र में कहा गया था कि यदि कोई साधु रोगी साधु की सेवा में स्थित साधु को यह कहकर मनोज्ञ आहार दे गया हो कि इस आहार को रोगी को दे देना यदि वह न खाए तो तुम खा लेना, तो साधु उस आहार को अपने लिए छुपाकर नहीं रखे। और प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि किसी साधु ने प्रतिज्ञा पूर्वक यह कहा हो कि यह मनोज्ञ आहार रोगी साधु को ही देना यदि वह न खाए तो हमें वापिस लाकर दे देना, तो उस साधु को चाहिए कि वह आहार रोगी साधु को दे। स्वयं उसका उपभोग न करे। यदि वह स्वाद की लोलुपता से उस आहार को अपने लिए छुपाकर रखता है, तो माया का सेवन करता है। और उसकी इस वृत्ति से उसका दूसरा महाव्रत भी भंग होता है और रोगी को आहार की अंतराय देने के कारण अन्तराय कर्म का भी बन्ध होता है। इस तरह स्वाद के वश साधु अपना अध: पतन कर लेता है। वह आध्यात्मिक साधना से भ्रष्ट हो जाता है। अतः साधक को अपनी क्रिया में छल-कपट नहीं करना चाहिए। पदार्थों के स्वाद की अपेक्षा साधना, सरलता, सेवा एवं सत्यता का अधिक मूल्य है, उस से आत्मा का विकास होता है। इस लिए साधु को शुद्ध एवं निष्कपट भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए और उसके लिए जो आहार दिया गया हो उसे बिना छुपाए उसी रूप में उसको देना चाहिए। वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।
अब सूत्रकार सप्त पिंडैषणा के विषय में कहते हैं
मूलम्- अह भिक्खू जाणिज्जा सत्त पिंडेसणाओ सत्त पाणेसणाओ, तत्थ खलु इमा पढमा पिंडेसणा-असंसट्ठे हत्थे असंसढे मत्ते, तहप्पगारेण असंसद्रुण हत्थेण वा मत्तेण वा असणं वा ४ सयं वा णं जाइज्जा परो वा से दिज्जा फासुयं पडिगाहिज्जा, पढमा पिंडेसणा॥१॥ अहावरा दुच्चा पिंडेसणा संसटे हत्थे संसटे मत्ते, तहेव दुच्चा पिण्डेसणा॥२॥ अहावरा तच्चा पिंडेसणा इह खलु पाईणं वा ४ संतेगइआ सड्ढा भवंति-गाहावई वा जाव कम्मकरी वा, तेसिंचणं अन्नयरेसुविरूवरूवेसु भायणजाएसु उवनिक्खित्तपुव्वे सिया तंजहाथालंसि वा, पिढरंसि वा सरगंसि वा परगंसि वा वरगंसि वा, अह पुणेवं जाणिज्जा- असंसट्ठे हत्थे संसढे मत्ते, संसट्टे वा हत्थे असंसट्टे मत्ते, सेय पडिग्गहधारी सिया पाणिपडिग्गहिए वा, से पुव्वामेवः-आउसोत्ति वा ! २ एएण तुमं असंसद्रुण हत्थेण,संसट्टेण मत्तेण संसट्टेण वा हत्थेण असंसद्रेण
१ सचैवमुक्तः सन् एवं वदेत्- यथाऽन्तरायमंतरेणाहरिष्यामीति प्रतिज्ञयाऽऽहारमादाय ग्लानांतिकं गत्वा प्राक्तनान् भक्तादिरूक्षादिदोषानुदघाट्य ग्लानायादत्वा स्वतएव लौल्याद् भुक्त्वा ततस्तस्य साधोर्निवेदयति, यथा मम शूलं वैयावृत्यकालापर्याप्यादिकमन्तरायिकमभूदतोऽहं तद् ग्लानभक्तं गृहीत्वा नायात इत्यादि मातृस्थानं संस्पृशेत् एतदेव दर्शयतिइत्येतानि-पूर्वोक्तान्यायतनानि- कर्मोपादानस्थानानि 'उपातिक्रम्य' सम्यक परिहत्य मातृस्थानपरिहारेण ग्लानाय वा दद्याद् दातृसाधुसमीपं वाऽऽहरेदिति। - आचाराङ्ग वृत्ति।