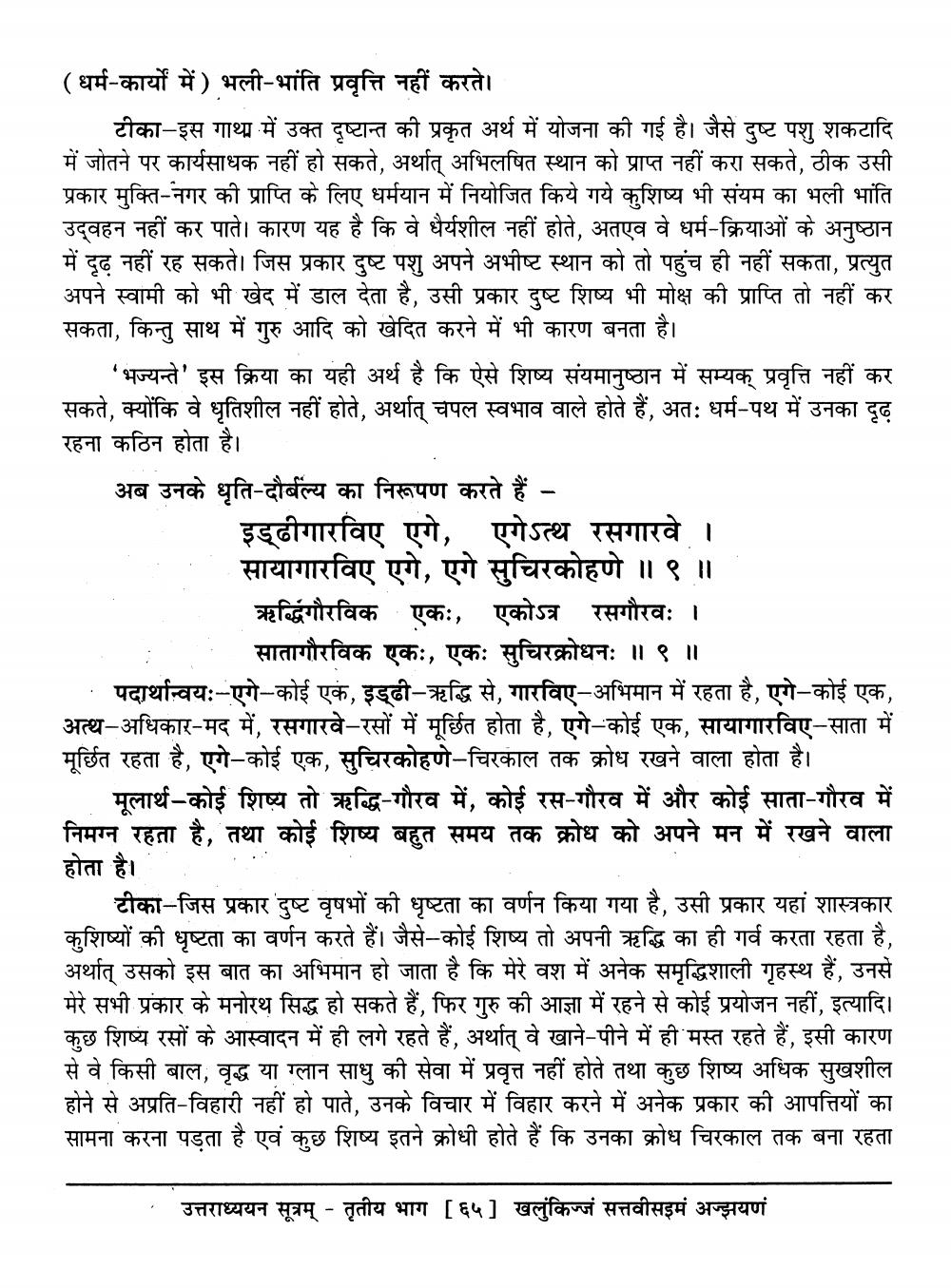________________
(धर्म-कार्यों में) भली-भांति प्रवृत्ति नहीं करते।
टीका-इस गाथा में उक्त दृष्टान्त की प्रकृत अर्थ में योजना की गई है। जैसे दुष्ट पशु शकटादि में जोतने पर कार्यसाधक नहीं हो सकते, अर्थात् अभिलषित स्थान को प्राप्त नहीं करा सकते, ठीक उसी प्रकार मुक्ति-नगर की प्राप्ति के लिए धर्मयान में नियोजित किये गये कुशिष्य भी संयम का भली भांति उद्वहन नहीं कर पाते। कारण यह है कि वे धैर्यशील नहीं होते, अतएव वे धर्म-क्रियाओं के अनुष्ठान में दृढ़ नहीं रह सकते। जिस प्रकार दुष्ट पशु अपने अभीष्ट स्थान को तो पहुंच ही नहीं सकता, प्रत्युत अपने स्वामी को भी खेद में डाल देता है, उसी प्रकार दुष्ट शिष्य भी मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं कर सकता, किन्तु साथ में गुरु आदि को खेदित करने में भी कारण बनता है।
'भज्यन्ते' इस क्रिया का यही अर्थ है कि ऐसे शिष्य संयमानुष्ठान में सम्यक् प्रवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वे धृतिशील नहीं होते, अर्थात् चपल स्वभाव वाले होते हैं, अतः धर्म-पथ में उनका दृढ़ रहना कठिन होता है। अब उनके धृति-दौर्बल्य का निरूपण करते हैं -
इड्ढीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे । सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥९॥ ऋद्धिंगौरविक एकः, एकोऽत्र रसगौरवः ।
सातागौरविक एकः, एकः सुचिरक्रोधनः ॥ ९ ॥ पदार्थान्वयः-एगे-कोई एक, इड्ढी-ऋद्धि से, गारविए-अभिमान में रहता है, एगे-कोई एक, अत्थ-अधिकार-मद में, रसगारवे-रसों में मूर्छित होता है, एगे-कोई एक, सायागारविए-साता में मूर्छित रहता है, एगे-कोई एक, सुचिरकोहणे-चिरकाल तक क्रोध रखने वाला होता है।
मूलार्थ-कोई शिष्य तो ऋद्धि-गौरव में, कोई रस-गौरव में और कोई साता-गौरव में निमग्न रहता है, तथा कोई शिष्य बहुत समय तक क्रोध को अपने मन में रखने वाला होता है।
टीका-जिस प्रकार दुष्ट वृषभों की धृष्टता का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहां शास्त्रकार कुशिष्यों की धृष्टता का वर्णन करते हैं। जैसे-कोई शिष्य तो अपनी ऋद्धि का ही गर्व करता रहता है, अर्थात् उसको इस बात का अभिमान हो जाता है कि मेरे वश में अनेक समृद्धिशाली गृहस्थ हैं, उनसे मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, फिर गुरु की आज्ञा में रहने से कोई प्रयोजन नहीं, इत्यादि। कुछ शिष्य रसों के आस्वादन में ही लगे रहते हैं, अर्थात् वे खाने-पीने में ही मस्त रहते हैं, इसी कारण से वे किसी बाल, वृद्ध या ग्लान साधु की सेवा में प्रवृत्त नहीं होते तथा कुछ शिष्य अधिक सुखशील होने से अप्रति-विहारी नहीं हो पाते, उनके विचार में विहार करने में अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है एवं कुछ शिष्य इतने क्रोधी होते हैं कि उनका क्रोध चिरकाल तक बना रहता
- उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [६५] खलुंकिजं सत्तवीसइमं अज्झयणं