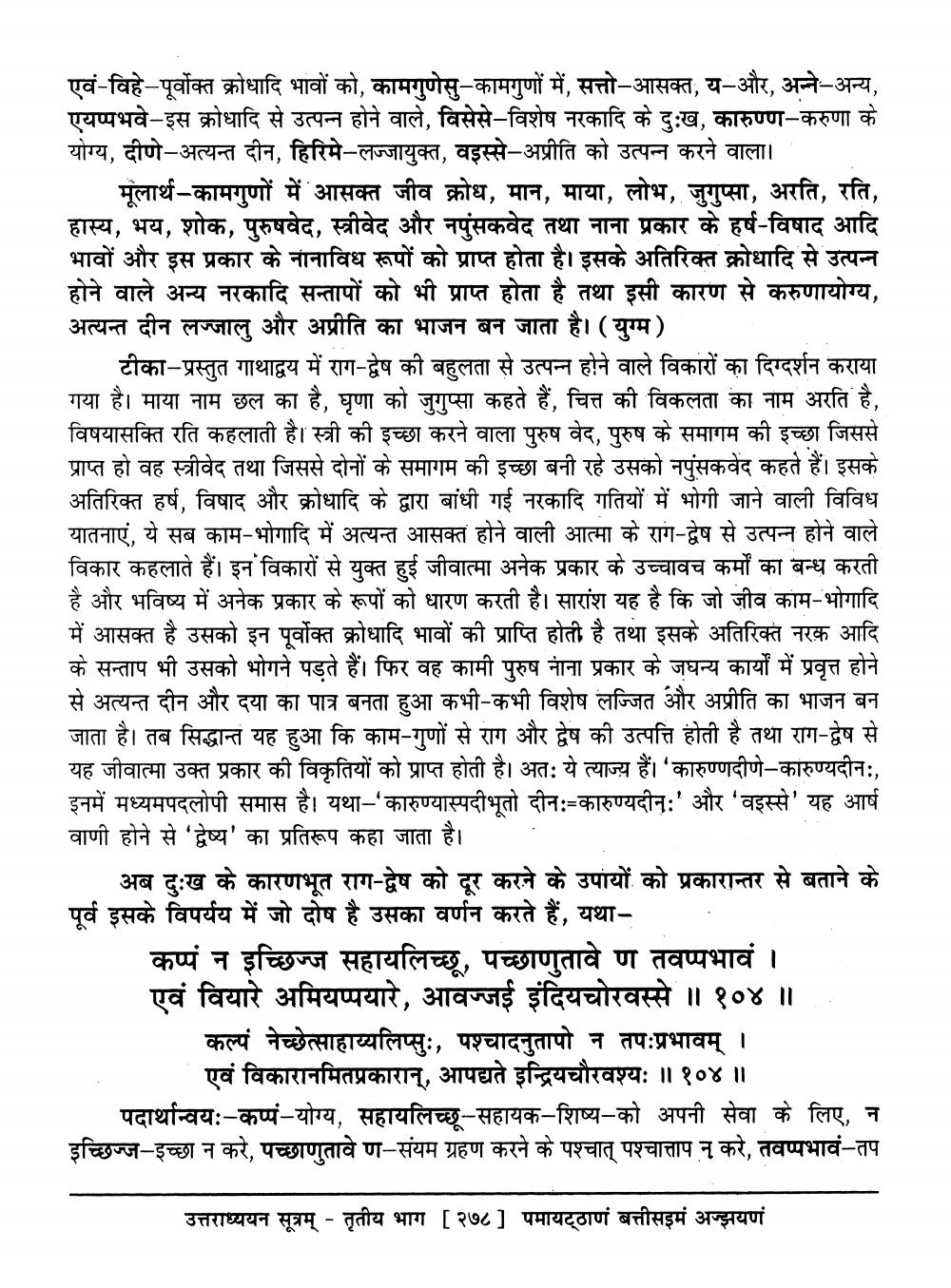________________
एवं-विहे-पूर्वोक्त क्रोधादि भावों को, कामगुणेसु-कामगुणों में, सत्तो-आसक्त, य-और, अन्ने-अन्य, एयप्पभवे-इस क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले, विसेसे-विशेष नरकादि के दु:ख, कारुण्ण-करुणा के योग्य, दीणे-अत्यन्त दीन, हिरिमे-लज्जायुक्त, वइस्से-अप्रीति को उत्पन्न करने वाला।
मूलार्थ-कामगुणों में आसक्त जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद तथा नाना प्रकार के हर्ष-विषाद आदि भावों और इस प्रकार के नानाविध रूपों को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले अन्य नरकादि सन्तापों को भी प्राप्त होता है तथा इसी कारण से करुणायोग्य, अत्यन्त दीन लज्जालु और अप्रीति का भाजन बन जाता है। (युग्म) ____टीका-प्रस्तुत गाथाद्वय में राग-द्वेष की बहुलता से उत्पन्न होने वाले विकारों का दिग्दर्शन कराया गया है। माया नाम छल का है, घृणा को जुगुप्सा कहते हैं, चित्त की विकलता का नाम अरति है, विषयासक्ति रति कहलाती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष वेद, पुरुष के समागम की इच्छा जिससे प्राप्त हो वह स्त्रीवेद तथा जिससे दोनों के समागम की इच्छा बनी रहे उसको नपुंसकवेद कहते हैं। इसके अतिरिक्त हर्ष, विषाद और क्रोधादि के द्वारा बांधी गई नरकादि गतियों में भोगी जाने वाली विविध यातनाएं, ये सब काम-भोगादि में अत्यन्त आसक्त होने वाली आत्मा के राग-द्वेष से उत्पन्न होने वाले विकार कहलाते हैं। इन विकारों से युक्त हुई जीवात्मा अनेक प्रकार के उच्चावच कर्मों का बन्ध करती है और भविष्य में अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है। सारांश यह है कि जो जीव काम-भोगादि में आसक्त है उसको इन पूर्वोक्त क्रोधादि भावों की प्राप्ति होती है तथा इसके अतिरिक्त नरक आदि के सन्ताप भी उसको भोगने पड़ते हैं। फिर वह कामी पुरुष नाना प्रकार के जघन्य कार्यों में प्रवृत्त होने से अत्यन्त दीन और दया का पात्र बनता हुआ कभी-कभी विशेष लज्जित और अप्रीति का भाजन बन जाता है। तब सिद्धान्त यह हुआ कि काम-गुणों से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा राग-द्वेष से यह जीवात्मा उक्त प्रकार की विकृतियों को प्राप्त होती है। अतः ये त्याज्य हैं। कारुण्णदीणे-कारुण्यदीनः, इनमें मध्यमपदलोपी समास है। यथा-'कारुण्यास्पदीभूतो दीन: कारुण्यदीनः' और 'वइस्से' यह आर्ष वाणी होने से 'द्वेष्य' का प्रतिरूप कहा जाता है।
अब दुःख के कारणभूत राग-द्वेष को दूर करने के उपायों को प्रकारान्तर से बताने के पूर्व इसके विपर्यय में जो दोष है उसका वर्णन करते हैं, यथा
कप्पं न इच्छिज्ज सहायलिच्छू, पच्छाणुतावे ण तवप्पभावं । एवं वियारे अमियप्पयारे, आवज्जई इंदियचोरवस्से ॥ १०४ ॥
कल्पं नेच्छेत्साहाय्यलिप्सुः, पश्चादनुतापो न तपःप्रभावम् ।
एवं विकारानमितप्रकारान्, आपद्यते इन्द्रियचौरवश्यः ॥ १०४ ॥ पदार्थान्वयः-कप्प-योग्य, सहायलिच्छू-सहायक-शिष्य-को अपनी सेवा के लिए, न इच्छिज्ज-इच्छा न करे, पच्छाणुतावे ण-संयम ग्रहण करने के पश्चात् पश्चात्ताप न करे, तवप्पभावं-तप
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २७८ ] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं