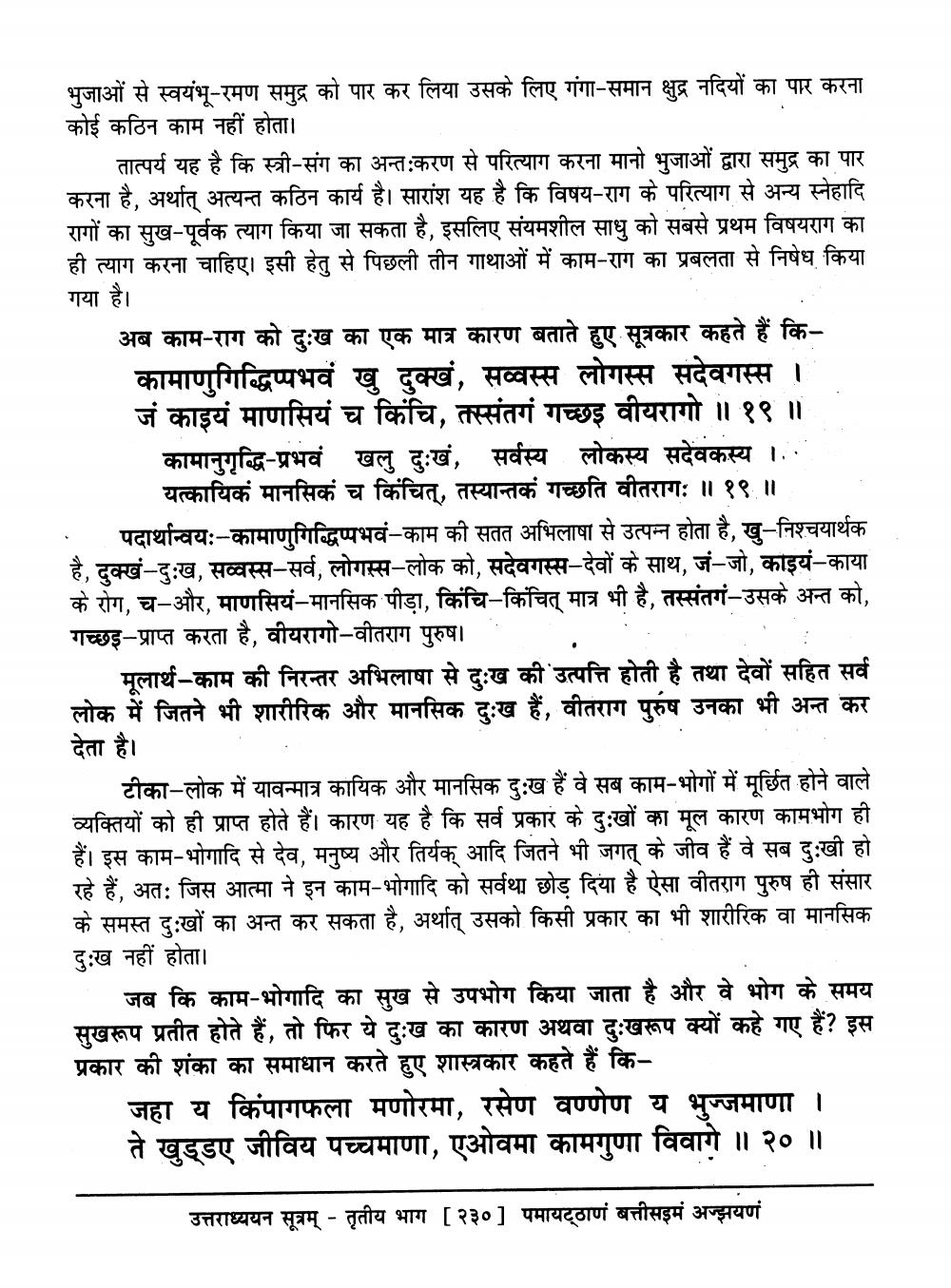________________
भुजाओं से स्वयंभू-रमण समुद्र को पार कर लिया उसके लिए गंगा-समान क्षुद्र नदियों का पार करना कोई कठिन काम नहीं होता।
तात्पर्य यह है कि स्त्री-संग का अन्त:करण से परित्याग करना मानो भुजाओं द्वारा समुद्र का पार करना है, अर्थात् अत्यन्त कठिन कार्य है। सारांश यह है कि विषय-राग के परित्याग से अन्य स्नेहादि रागों का सुख-पूर्वक त्याग किया जा सकता है, इसलिए संयमशील साधु को सबसे प्रथम विषयराग का ही त्याग करना चाहिए। इसी हेतु से पिछली तीन गाथाओं में काम-राग का प्रबलता से निषेध किया गया है।
अब काम-राग को दुःख का एक मात्र कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं किकामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । जं काइयं माणसियं च किंचि, तस्संतगं गच्छइ वीयरागो ॥ १९ ॥
कामानुगृद्धि-प्रभवं खलु दुःखं, सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।..
यत्कायिकं मानसिकं च किंचित्, तस्यान्तकं गच्छति वीतरागः ॥ १९ ॥ • पदार्थान्वयः-कामाणुगिद्धिप्पभवं-काम की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है, खु-निश्चयार्थक है, दुक्खं-दुःख, सव्वस्स-सर्व, लोगस्स-लोक को, सदेवगस्स-देवों के साथ, जं-जो, काइयं-काया के रोग, च-और, माणसियं-मानसिक पीड़ा, किंचि-किंचित् मात्र भी है, तस्संतगं-उसके अन्त को, गच्छइ-प्राप्त करता है, वीयरागो-वीतराग पुरुष। . .
मूलार्थ-काम की निरन्तर अभिलाषा से दुःख की उत्पत्ति होती है तथा देवों सहित सर्व लोक में जितने भी शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, वीतराग पुरुष उनका भी अन्त कर देता है।
टीका-लोक में यावन्मात्र कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब काम-भोगों में मूर्छित होने वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि सर्व प्रकार के दुःखों का मूल कारण कामभोग ही हैं। इस काम-भोगादि से देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि जितने भी जगत् के जीव हैं वे सब दुःखी हो रहे हैं, अत: जिस आत्मा ने इन काम-भोगादि को सर्वथा छोड़ दिया है ऐसा वीतराग पुरुष ही संसार के समस्त दुःखों का अन्त कर सकता है, अर्थात् उसको किसी प्रकार का भी शारीरिक वा मानसिक दु:ख नहीं होता। ___ जब कि काम-भोगादि का सुख से उपभोग किया जाता है और वे भोग के समय सुखरूप प्रतीत होते हैं, तो फिर ये दुःख का कारण अथवा दुःखरूप क्यों कहे गए हैं? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि
जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा । ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥ २० ॥
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २३०] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं