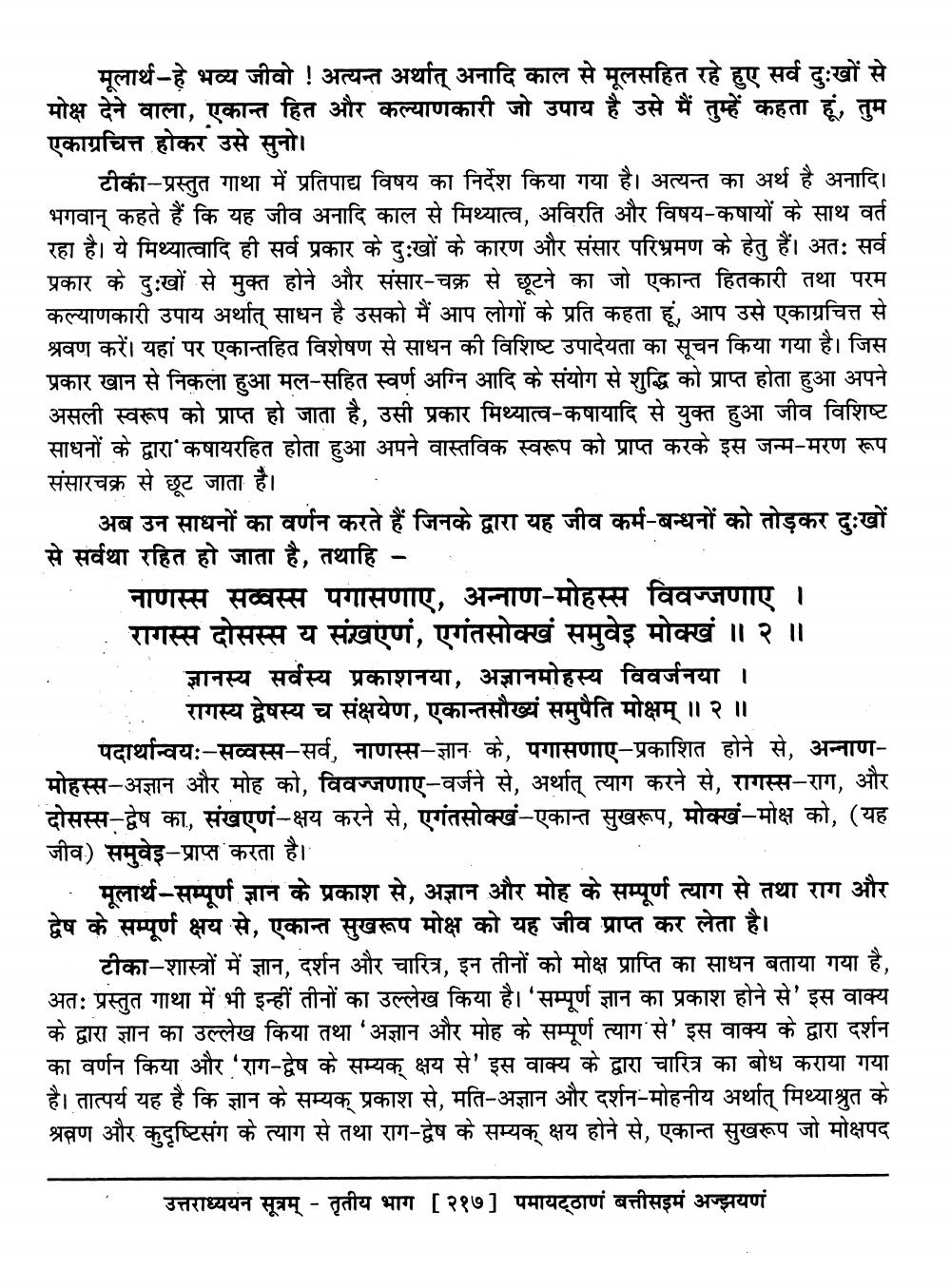________________
मूलार्थ - हे भव्य जीवो ! अत्यन्त अर्थात् अनादि काल से मूलसहित रहे हुए सर्व दुःखों से मोक्ष देने वाला, एकान्त हित और कल्याणकारी जो उपाय है उसे मैं तुम्हें कहता हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो।
टीका - प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया गया है। अत्यन्त का अर्थ है अनादि । भगवान् कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व, अविरति और विषय - कषायों के साथ वर्त रहा है। ये मिथ्यात्वादि ही सर्व प्रकार के दुःखों के कारण और संसार परिभ्रमण के हेतु हैं। अतः सर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त होने और संसार चक्र से छूटने का जो एकान्त हितकारी तथा परम कल्याणकारी उपाय अर्थात् साधन है उसको मैं आप लोगों के प्रति कहता हूं, आप उसे एकाग्रचित्त से श्रवण करें। यहां पर एकान्तहित विशेषण से साधन की विशिष्ट उपादेयता का सूचन किया गया है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ मल सहित स्वर्ण अग्नि आदि के संयोग से शुद्धि को प्राप्त होता हुआ अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व - कषायादि से युक्त हुआ जीव विशिष्ट साधनों के द्वारा कषायरहित होता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके इस जन्म-मरण रूप संसारचक्र से छूट जाता है ।
अब उन साधनों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा यह जीव कर्म - बन्धनों को तोड़कर दुःखों से सर्वथा रहित हो जाता है, तथाहि
-
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण- मोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥ २ ॥
ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया । रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण, एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम् ॥ २ ॥
पदार्थान्वयः - सव्वस्स- सर्व, नाणस्स - ज्ञान के, पगासणाए - प्रकाशित होने से, अन्नाणमोहस्स - अज्ञान और मोह को, विवज्जणाए - वर्जने से, अर्थात् त्याग करने से, रागस्स - राग, और दोसस्स - द्वेष का, संखएणं-क्षय करने से, एगंतसोक्खं - एकान्त सुखरूप, मोक्खं - मोक्ष को, (यह जीव) समुवेइ- - प्राप्त करता है।
मूलार्थ - सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से तथा राग और द्वेष के सम्पूर्ण क्षय से, एकान्त सुखरूप मोक्ष को यह जीव प्राप्त कर लेता है।
टीका- शास्त्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है, अतः प्रस्तुत गाथा में भी इन्हीं तीनों का उल्लेख किया है। 'सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होने से' इस वाक्य के द्वारा ज्ञान का उल्लेख किया तथा 'अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से' इस वाक्य के द्वारा दर्शन का वर्णन किया और 'राग-द्वेष के सम्यक् क्षय से' इस वाक्य के द्वारा चारित्र का बोध कराया गया है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान के सम्यक् प्रकाश से, मति - अज्ञान और दर्शन - मोहनीय अर्थात् मिथ्याश्रुत के श्रवण और कुदृष्टिसंग के त्याग से तथा राग-द्वेष के सम्यक् क्षय होने से, एकान्त सुखरूप जो मोक्षपद
उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [२१७] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं